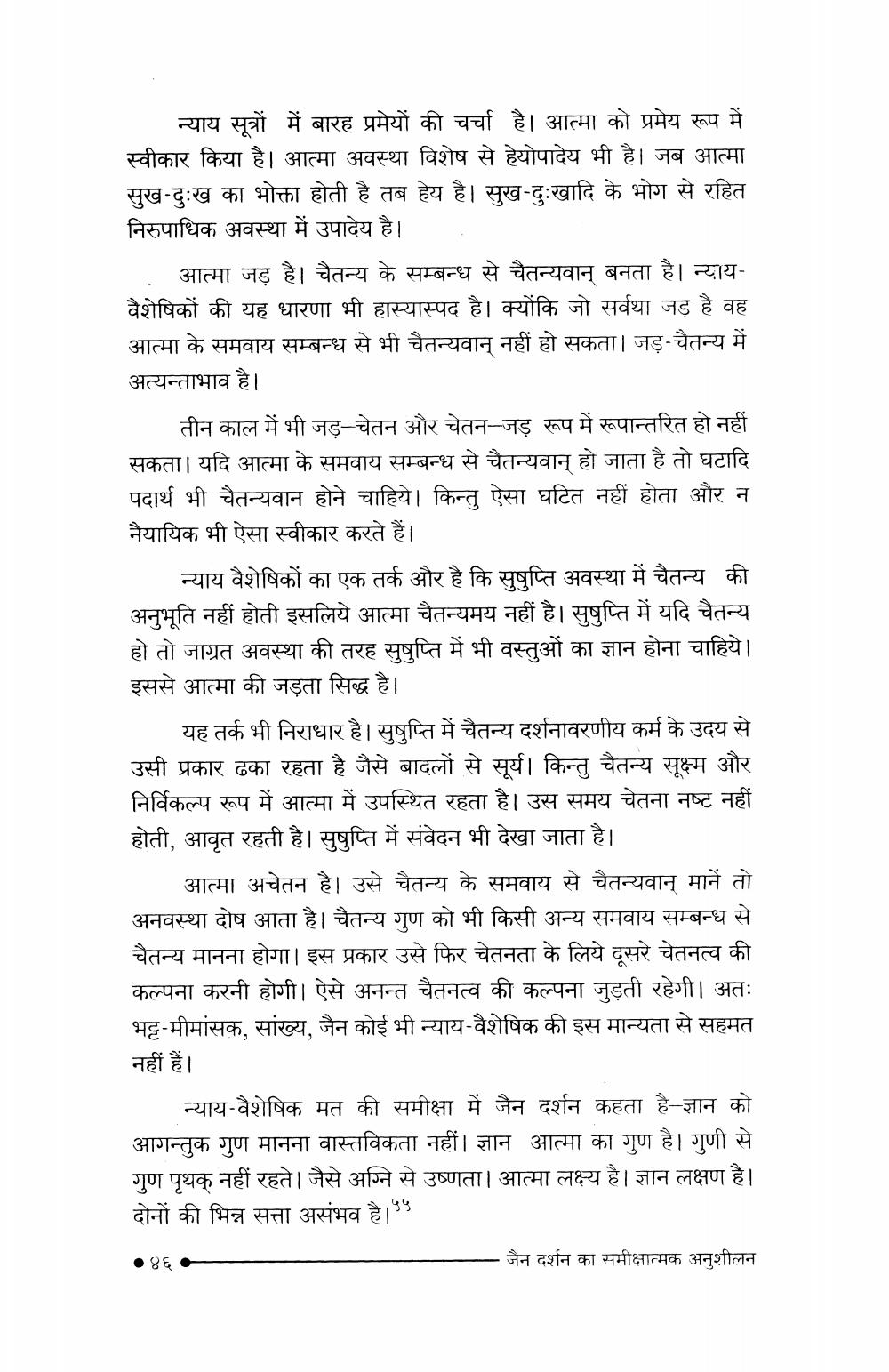________________
न्याय सूत्रों में बारह प्रमेयों की चर्चा है। आत्मा को प्रमेय रूप में स्वीकार किया है। आत्मा अवस्था विशेष से हेयोपादेय भी है। जब आत्मा सुख-दुःख का भोक्ता होती है तब हेय है। सुख-दुःखादि के भोग से रहित निरुपाधिक अवस्था में उपादेय है।
आत्मा जड़ है। चैतन्य के सम्बन्ध से चैतन्यवान् बनता है। न्यायवैशेषिकों की यह धारणा भी हास्यास्पद है। क्योंकि जो सर्वथा जड़ है वह आत्मा के समवाय सम्बन्ध से भी चैतन्यवान् नहीं हो सकता। जड़-चैतन्य में अत्यन्ताभाव है।
तीन काल में भी जड़-चेतन और चेतन-जड़ रूप में रूपान्तरित हो नहीं सकता। यदि आत्मा के समवाय सम्बन्ध से चैतन्यवान् हो जाता है तो घटादि पदार्थ भी चैतन्यवान होने चाहिये। किन्तु ऐसा घटित नहीं होता और न नैयायिक भी ऐसा स्वीकार करते हैं।
न्याय वैशेषिकों का एक तर्क और है कि सुषुप्ति अवस्था में चैतन्य की अनुभूति नहीं होती इसलिये आत्मा चैतन्यमय नहीं है। सुषुप्ति में यदि चैतन्य हो तो जाग्रत अवस्था की तरह सुषुप्ति में भी वस्तुओं का ज्ञान होना चाहिये। इससे आत्मा की जड़ता सिद्ध है।
यह तर्क भी निराधार है। सुषुप्ति में चैतन्य दर्शनावरणीय कर्म के उदय से उसी प्रकार ढका रहता है जैसे बादलों से सूर्य। किन्तु चैतन्य सूक्ष्म और निर्विकल्प रूप में आत्मा में उपस्थित रहता है। उस समय चेतना नष्ट नहीं होती, आवृत रहती है। सुषुप्ति में संवेदन भी देखा जाता है।
आत्मा अचेतन है। उसे चैतन्य के समवाय से चैतन्यवान् मानें तो अनवस्था दोष आता है। चैतन्य गुण को भी किसी अन्य समवाय सम्बन्ध से चैतन्य मानना होगा। इस प्रकार उसे फिर चेतनता के लिये दूसरे चेतनत्व की कल्पना करनी होगी। ऐसे अनन्त चैतनत्व की कल्पना जुड़ती रहेगी। अतः भट्ट-मीमांसक, सांख्य, जैन कोई भी न्याय-वैशेषिक की इस मान्यता से सहमत नहीं हैं।
न्याय-वैशेषिक मत की समीक्षा में जैन दर्शन कहता है-ज्ञान को आगन्तुक गुण मानना वास्तविकता नहीं। ज्ञान आत्मा का गुण है। गुणी से गुण पृथक् नहीं रहते। जैसे अग्नि से उष्णता। आत्मा लक्ष्य है। ज्ञान लक्षण है। दोनों की भिन्न सत्ता असंभव है।५५
- जैन दर्शन का समीक्षात्मक अनशीलन