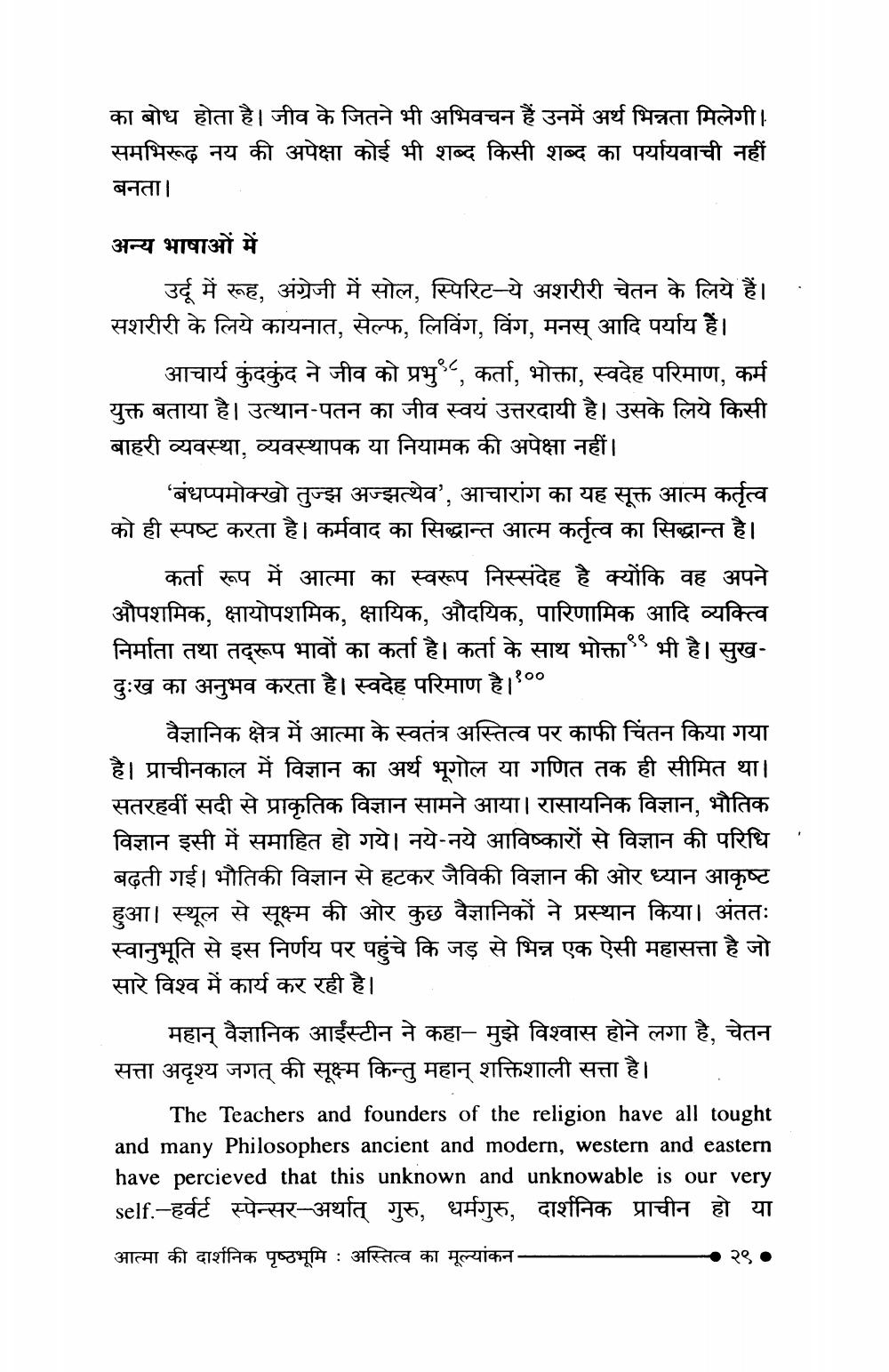________________
का बोध होता है। जीव के जितने भी अभिवचन हैं उनमें अर्थ भिन्नता मिलेगी। समभिरूढ़ नय की अपेक्षा कोई भी शब्द किसी शब्द का पर्यायवाची नहीं बनता।
अन्य भाषाओं में
उर्दू में रूह, अंग्रेजी में सोल, स्पिरिट-ये अशरीरी चेतन के लिये हैं। . सशरीरी के लिये कायनात, सेल्फ, लिविंग, विंग, मनस् आदि पर्याय हैं।
आचार्य कुंदकुंद ने जीव को प्रभु, कर्ता, भोक्ता, स्वदेह परिमाण, कर्म युक्त बताया है। उत्थान-पतन का जीव स्वयं उत्तरदायी है। उसके लिये किसी बाहरी व्यवस्था, व्यवस्थापक या नियामक की अपेक्षा नहीं।
'बंधप्पमोक्खो तुज्झ अज्झत्थेव', आचारांग का यह सूक्त आत्म कर्तृत्व को ही स्पष्ट करता है। कर्मवाद का सिद्धान्त आत्म कर्तृत्व का सिद्धान्त है।
कर्ता रूप में आत्मा का स्वरूप निस्संदेह है क्योंकि वह अपने औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, औदयिक, पारिणामिक आदि व्यक्त्वि निर्माता तथा तद्रूप भावों का कर्ता है। कर्ता के साथ भोक्ता ९ भी है। सुखदुःख का अनुभव करता है। स्वदेह परिमाण है।१००
वैज्ञानिक क्षेत्र में आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व पर काफी चिंतन किया गया है। प्राचीनकाल में विज्ञान का अर्थ भूगोल या गणित तक ही सीमित था। सतरहवीं सदी से प्राकृतिक विज्ञान सामने आया। रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान इसी में समाहित हो गये। नये-नये आविष्कारों से विज्ञान की परिधि बढ़ती गई। भौतिकी विज्ञान से हटकर जैविकी विज्ञान की ओर ध्यान आकृष्ट हुआ। स्थूल से सूक्ष्म की ओर कुछ वैज्ञानिकों ने प्रस्थान किया। अंततः स्वानुभूति से इस निर्णय पर पहुंचे कि जड़ से भिन्न एक ऐसी महासत्ता है जो सारे विश्व में कार्य कर रही है।
महान् वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा- मुझे विश्वास होने लगा है, चेतन सत्ता अदृश्य जगत् की सूक्ष्म किन्तु महान् शक्तिशाली सत्ता है।
The Teachers and founders of the religion have all tought and many Philosophers ancient and modern, western and eastern have percieved that this unknown and unknowable is our very self. हर्ट स्पेन्सर-अर्थात् गुरु, धर्मगुरु, दार्शनिक प्राचीन हो या
आत्मा की दार्शनिक पृष्ठभूमि : अस्तित्व का मूल्यांकन
.२९.