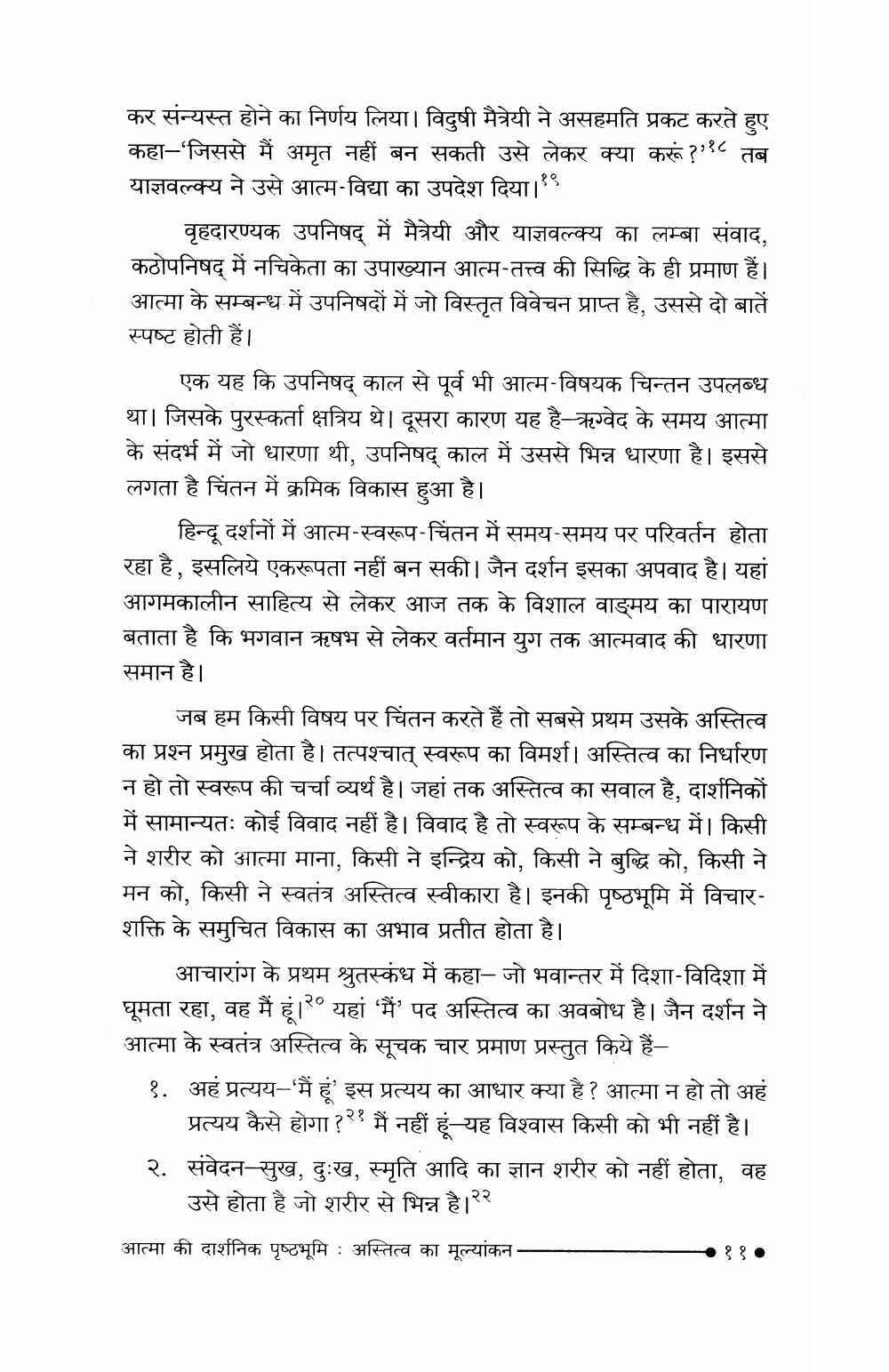________________
कर संन्यस्त होने का निर्णय लिया। विदुषी मैत्रेयी ने असहमति प्रकट करते हुए कहा-'जिससे मैं अमृत नहीं बन सकती उसे लेकर क्या करूं ?१८ तब याज्ञवल्क्य ने उसे आत्म-विद्या का उपदेश दिया।
वृहदारण्यक उपनिषद् में मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का लम्बा संवाद, कठोपनिषद् में नचिकेता का उपाख्यान आत्म-तत्त्व की सिद्धि के ही प्रमाण हैं। आत्मा के सम्बन्ध में उपनिषदों में जो विस्तृत विवेचन प्राप्त है, उससे दो बातें स्पष्ट होती हैं।
एक यह कि उपनिषद् काल से पूर्व भी आत्म-विषयक चिन्तन उपलब्ध था। जिसके पुरस्कर्ता क्षत्रिय थे। दूसरा कारण यह है ऋग्वेद के समय आत्मा के संदर्भ में जो धारणा थी, उपनिषद् काल में उससे भिन्न धारणा है। इससे लगता है चिंतन में क्रमिक विकास हुआ है।
हिन्दू दर्शनों में आत्म-स्वरूप-चिंतन में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है, इसलिये एकरूपता नहीं बन सकी। जैन दर्शन इसका अपवाद है। यहां आगमकालीन साहित्य से लेकर आज तक के विशाल वाङ्मय का पारायण बताता है कि भगवान ऋषभ से लेकर वर्तमान युग तक आत्मवाद की धारणा समान है।
जब हम किसी विषय पर चिंतन करते हैं तो सबसे प्रथम उसके अस्तित्व का प्रश्न प्रमुख होता है। तत्पश्चात् स्वरूप का विमर्श। अस्तित्व का निर्धारण न हो तो स्वरूप की चर्चा व्यर्थ है। जहां तक अस्तित्व का सवाल है, दार्शनिकों में सामान्यतः कोई विवाद नहीं है। विवाद है तो स्वरूप के सम्बन्ध में। किसी ने शरीर को आत्मा माना, किसी ने इन्द्रिय को, किसी ने बुद्धि को, किसी ने मन को, किसी ने स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकारा है। इनकी पृष्ठभूमि में विचारशक्ति के समुचित विकास का अभाव प्रतीत होता है।
आचारांग के प्रथम श्रुतस्कंध में कहा- जो भवान्तर में दिशा-विदिशा में घूमता रहा, वह मैं हूं।२० यहां 'मैं' पद अस्तित्व का अवबोध है। जैन दर्शन ने आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व के सूचक चार प्रमाण प्रस्तुत किये हैं१. अहं प्रत्यय-'मैं हूं' इस प्रत्यय का आधार क्या है ? आत्मा न हो तो अहं
प्रत्यय कैसे होगा?२१ मैं नहीं हूं-यह विश्वास किसी को भी नहीं है। २. संवेदन-सुख, दुःख, स्मृति आदि का ज्ञान शरीर को नहीं होता, वह
उसे होता है जो शरीर से भिन्न है।२२
आत्मा की दार्शनिक पृष्ठभूमि : अस्तित्व का मूल्यांकन -
.११.