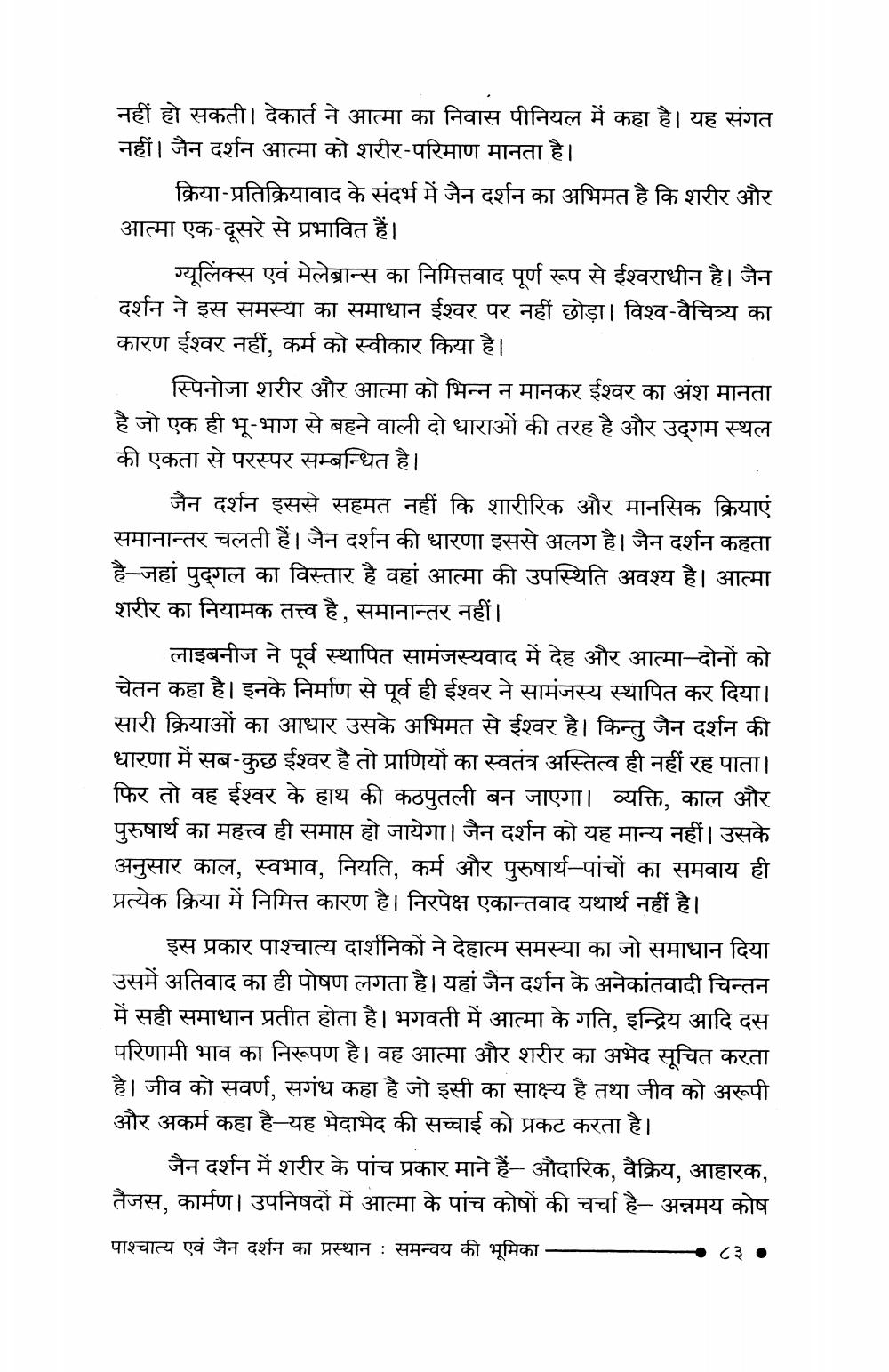________________
नहीं हो सकती। देकार्त ने आत्मा का निवास पीनियल में कहा है। यह संगत नहीं। जैन दर्शन आत्मा को शरीर-परिमाण मानता है।
क्रिया-प्रतिक्रियावाद के संदर्भ में जैन दर्शन का अभिमत है कि शरीर और आत्मा एक-दूसरे से प्रभावित हैं।
म्यूलिंक्स एवं मेलेब्रान्स का निमित्तवाद पूर्ण रूप से ईश्वराधीन है। जैन दर्शन ने इस समस्या का समाधान ईश्वर पर नहीं छोड़ा। विश्व-वैचित्र्य का कारण ईश्वर नहीं, कर्म को स्वीकार किया है।
__ स्पिनोजा शरीर और आत्मा को भिन्न न मानकर ईश्वर का अंश मानता है जो एक ही भू-भाग से बहने वाली दो धाराओं की तरह है और उद्गम स्थल की एकता से परस्पर सम्बन्धित है।
जैन दर्शन इससे सहमत नहीं कि शारीरिक और मानसिक क्रियाएं समानान्तर चलती हैं। जैन दर्शन की धारणा इससे अलग है। जैन दर्शन कहता है-जहां पुद्गल का विस्तार है वहां आत्मा की उपस्थिति अवश्य है। आत्मा शरीर का नियामक तत्त्व है, समानान्तर नहीं।
लाइबनीज ने पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद में देह और आत्मा दोनों को चेतन कहा है। इनके निर्माण से पूर्व ही ईश्वर ने सामंजस्य स्थापित कर दिया। सारी क्रियाओं का आधार उसके अभिमत से ईश्वर है। किन्तु जैन दर्शन की धारणा में सब-कुछ ईश्वर है तो प्राणियों का स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं रह पाता। फिर तो वह ईश्वर के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। व्यक्ति, काल और पुरुषार्थ का महत्त्व ही समाप्त हो जायेगा। जैन दर्शन को यह मान्य नहीं। उसके अनुसार काल, स्वभाव, नियति, कर्म और पुरुषार्थ-पांचों का समवाय ही प्रत्येक क्रिया में निमित्त कारण है। निरपेक्ष एकान्तवाद यथार्थ नहीं है।
इस प्रकार पाश्चात्य दार्शनिकों ने देहात्म समस्या का जो समाधान दिया उसमें अतिवाद का ही पोषण लगता है। यहां जैन दर्शन के अनेकांतवादी चिन्तन में सही समाधान प्रतीत होता है। भगवती में आत्मा के गति, इन्द्रिय आदि दस परिणामी भाव का निरूपण है। वह आत्मा और शरीर का अभेद सूचित करता है। जीव को सवर्ण, सगंध कहा है जो इसी का साक्ष्य है तथा जीव को अरूपी और अकर्म कहा है यह भेदाभेद की सच्चाई को प्रकट करता है।
जैन दर्शन में शरीर के पांच प्रकार माने हैं- औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस, कार्मण। उपनिषदों में आत्मा के पांच कोषों की चर्चा है- अन्नमय कोष पाश्चात्य एवं जैन दर्शन का प्रस्थान : समन्वय की भूमिका -
.८३.