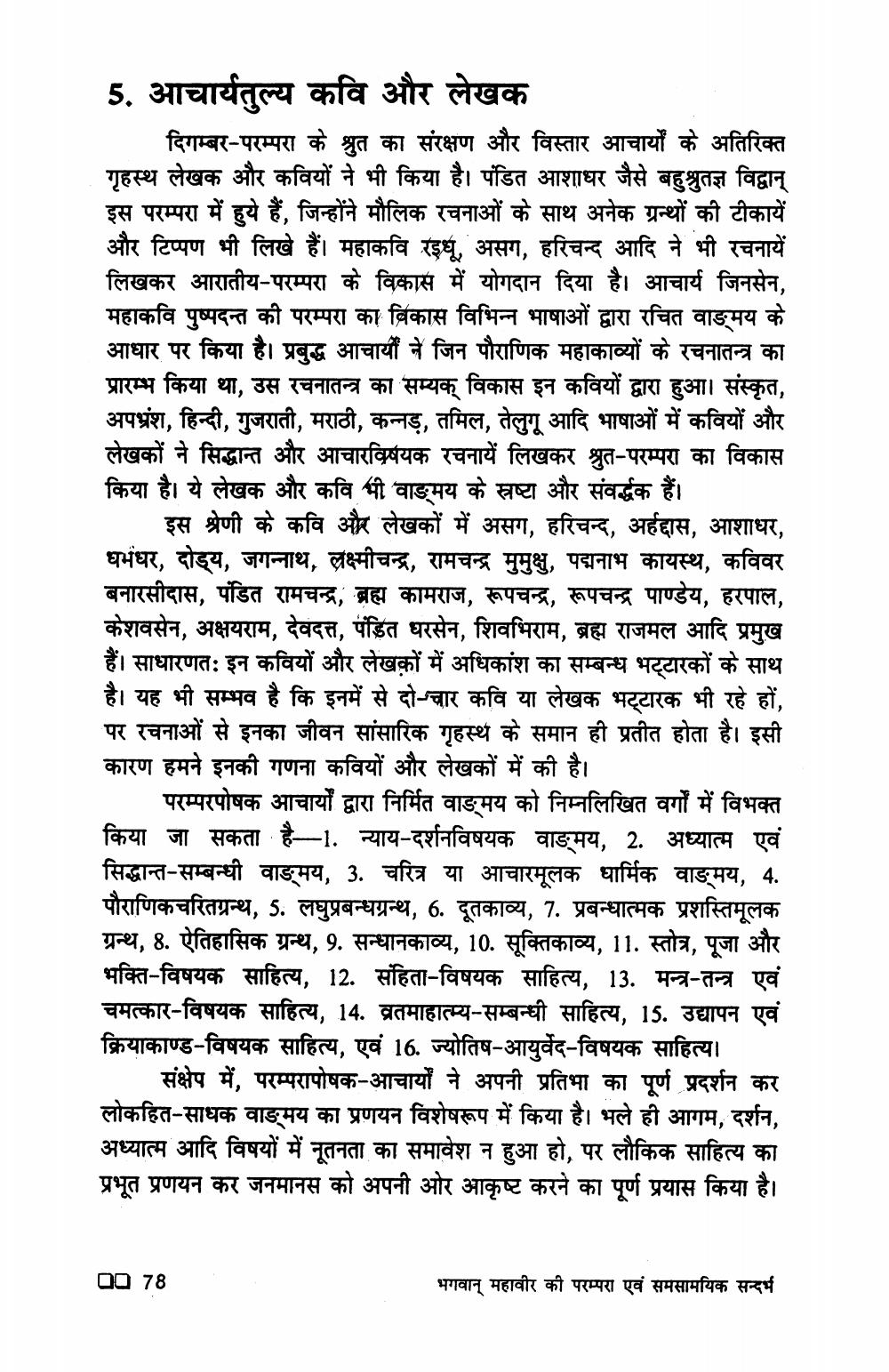________________
5. आचार्यतुल्य कवि और लेखक
दिगम्बर-परम्परा के श्रुत का संरक्षण और विस्तार आचार्यों के अतिरिक्त गृहस्थ लेखक और कवियों ने भी किया है। पंडित आशाधर जैसे बहुश्रुतज्ञ विद्वान् इस परम्परा में हुये हैं, जिन्होंने मौलिक रचनाओं के साथ अनेक ग्रन्थों की टीकायें
और टिप्पण भी लिखे हैं। महाकवि रइधू, असग, हरिचन्द आदि ने भी रचनायें लिखकर आरातीय-परम्परा के विकास में योगदान दिया है। आचार्य जिनसेन, महाकवि पुष्पदन्त की परम्परा का विकास विभिन्न भाषाओं द्वारा रचित वाङ्मय के आधार पर किया है। प्रबुद्ध आचार्यों ने जिन पौराणिक महाकाव्यों के रचनातन्त्र का प्रारम्भ किया था, उस रचनातन्त्र का सम्यक् विकास इन कवियों द्वारा हुआ। संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगू आदि भाषाओं में कवियों और लेखकों ने सिद्धान्त और आचारविषयक रचनायें लिखकर श्रुत-परम्परा का विकास किया है। ये लेखक और कवि भी वाङ्मय के स्रष्टा और संवर्द्धक हैं।
इस श्रेणी के कवि और लेखकों में असग, हरिचन्द, अर्हद्दास, आशाधर, धभंधर, दोड्य, जगन्नाथ, लक्ष्मीचन्द्र, रामचन्द्र मुमुक्षु, पद्मनाभ कायस्थ, कविवर बनारसीदास, पंडित रामचन्द्र, ब्रह्म कामराज, रूपचन्द्र, रूपचन्द्र पाण्डेय, हरपाल, केशवसेन, अक्षयराम, देवदत्त, पंडित धरसेन, शिवभिराम, ब्रह्म राजमल आदि प्रमुख हैं। साधारणतः इन कवियों और लेखकों में अधिकांश का सम्बन्ध भट्टारकों के साथ है। यह भी सम्भव है कि इनमें से दो-चार कवि या लेखक भट्टारक भी रहे हों, पर रचनाओं से इनका जीवन सांसारिक गृहस्थ के समान ही प्रतीत होता है। इसी कारण हमने इनकी गणना कवियों और लेखकों में की है।
परम्परपोषक आचार्यों द्वारा निर्मित वाङ्मय को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है-1. न्याय-दर्शनविषयक वाङ्मय, 2. अध्यात्म एवं सिद्धान्त-सम्बन्धी वाङ्मय, 3. चरित्र या आचारमूलक धार्मिक वाङ्मय, 4. पौराणिकचरितग्रन्थ, 5. लघुप्रबन्धग्रन्थ, 6. दूतकाव्य, 7. प्रबन्धात्मक प्रशस्तिमूलक ग्रन्थ, 8. ऐतिहासिक ग्रन्थ, 9. सन्धानकाव्य, 10. सूक्तिकाव्य, 11. स्तोत्र, पूजा और भक्ति-विषयक साहित्य, 12. संहिता-विषयक साहित्य, 13. मन्त्र-तन्त्र एवं चमत्कार-विषयक साहित्य, 14. व्रतमाहात्म्य-सम्बन्धी साहित्य, 15. उद्यापन एवं क्रियाकाण्ड-विषयक साहित्य, एवं 16. ज्योतिष-आयुर्वेद-विषयक साहित्य।
संक्षेप में, परम्परापोषक-आचार्यों ने अपनी प्रतिभा का पूर्ण प्रदर्शन कर लोकहित-साधक वाङ्मय का प्रणयन विशेषरूप में किया है। भले ही आगम, दर्शन, अध्यात्म आदि विषयों में नूतनता का समावेश न हुआ हो, पर लौकिक साहित्य का प्रभूत प्रणयन कर जनमानस को अपनी ओर आकृष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया है।
40 78
भगवान् महावीर की परम्परा एवं समसामयिक सन्दर्भ