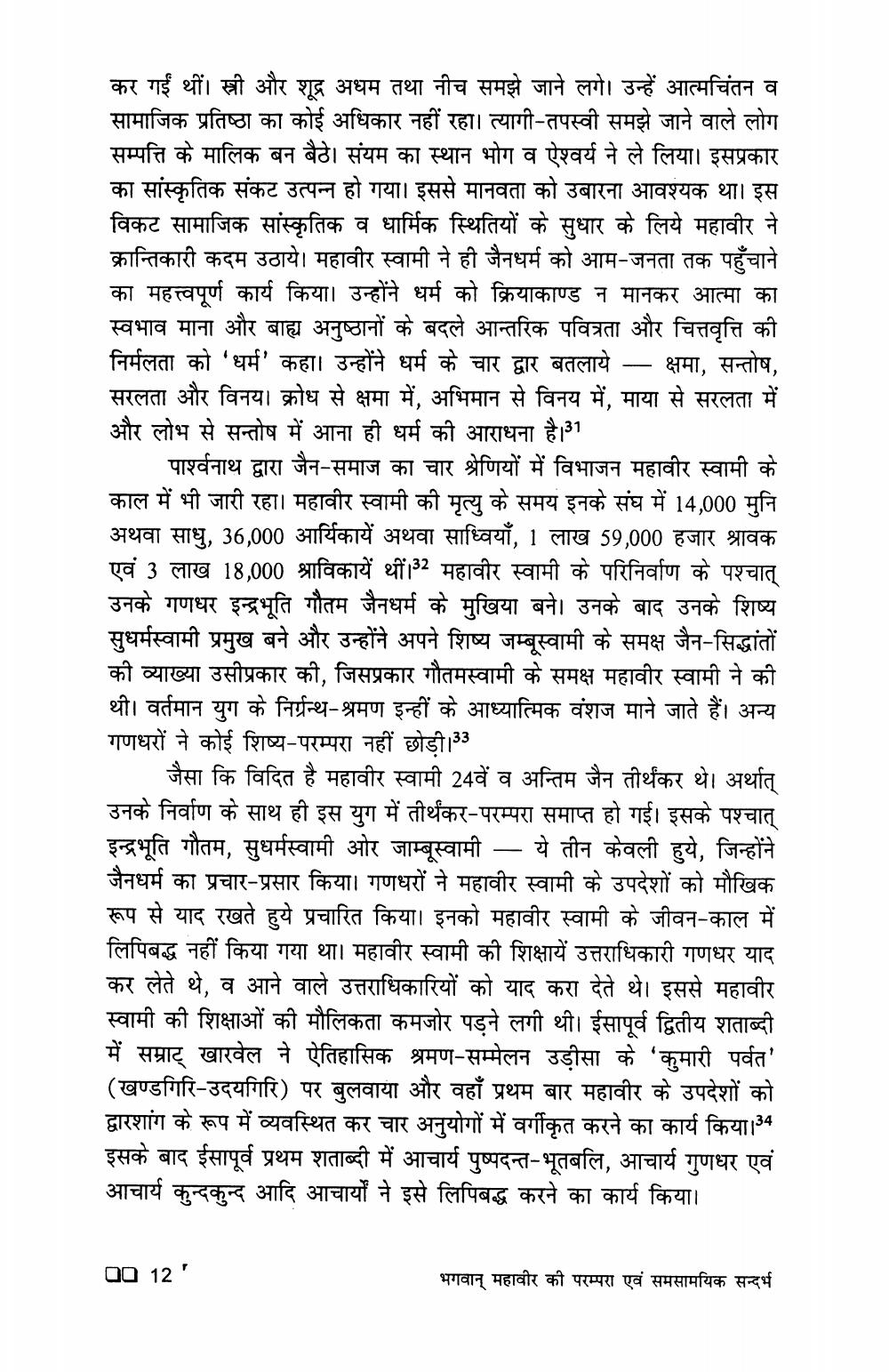________________
कर गईं थीं। स्त्री और शूद्र अधम तथा नीच समझे जाने लगे। उन्हें आत्मचिंतन व सामाजिक प्रतिष्ठा का कोई अधिकार नहीं रहा। त्यागी-तपस्वी समझे जाने वाले लोग सम्पत्ति के मालिक बन बैठे। संयम का स्थान भोग व ऐश्वर्य ने ले लिया। इसप्रकार का सांस्कृतिक संकट उत्पन्न हो गया। इससे मानवता को उबारना आवश्यक था। इस विकट सामाजिक सांस्कृतिक व धार्मिक स्थितियों के सुधार के लिये महावीर ने क्रान्तिकारी कदम उठाये। महावीर स्वामी ने ही जैनधर्म को आम-जनता तक पहुँचाने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने धर्म को क्रियाकाण्ड न मानकर आत्मा का स्वभाव माना और बाह्य अनुष्ठानों के बदले आन्तरिक पवित्रता और चित्तवृत्ति की निर्मलता को 'धर्म' कहा। उन्होंने धर्म के चार द्वार बतलाये – क्षमा, सन्तोष, सरलता और विनय। क्रोध से क्षमा में, अभिमान से विनय में, माया से सरलता में और लोभ से सन्तोष में आना ही धर्म की आराधना है।31
पार्श्वनाथ द्वारा जैन-समाज का चार श्रेणियों में विभाजन महावीर स्वामी के काल में भी जारी रहा। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय इनके संघ में 14,000 मुनि अथवा साधु, 36,000 आर्यिकायें अथवा साध्वियाँ, 1 लाख 59,000 हजार श्रावक एवं 3 लाख 18,000 श्राविकायें थीं।32 महावीर स्वामी के परिनिर्वाण के पश्चात् उनके गणधर इन्द्रभूति गौतम जैनधर्म के मुखिया बने। उनके बाद उनके शिष्य सुधर्मस्वामी प्रमुख बने और उन्होंने अपने शिष्य जम्बूस्वामी के समक्ष जैन-सिद्धांतों की व्याख्या उसीप्रकार की, जिसप्रकार गौतमस्वामी के समक्ष महावीर स्वामी ने की थी। वर्तमान युग के निर्ग्रन्थ-श्रमण इन्हीं के आध्यात्मिक वंशज माने जाते हैं। अन्य गणधरों ने कोई शिष्य-परम्परा नहीं छोड़ी।33
जैसा कि विदित है महावीर स्वामी 24वें व अन्तिम जैन तीर्थंकर थे। अर्थात् उनके निर्वाण के साथ ही इस युग में तीर्थंकर-परम्परा समाप्त हो गई। इसके पश्चात् इन्द्रभूति गौतम, सुधर्मस्वामी ओर जाम्बूस्वामी – ये तीन केवली हुये, जिन्होंने जैनधर्म का प्रचार-प्रसार किया। गणधरों ने महावीर स्वामी के उपदेशों को मौखिक रूप से याद रखते हुये प्रचारित किया। इनको महावीर स्वामी के जीवन-काल में लिपिबद्ध नहीं किया गया था। महावीर स्वामी की शिक्षायें उत्तराधिकारी गणधर याद कर लेते थे, व आने वाले उत्तराधिकारियों को याद करा देते थे। इससे महावीर स्वामी की शिक्षाओं की मौलिकता कमजोर पड़ने लगी थी। ईसापूर्व द्वितीय शताब्दी में सम्राट् खारवेल ने ऐतिहासिक श्रमण-सम्मेलन उड़ीसा के 'कुमारी पर्वत' (खण्डगिरि-उदयगिरि) पर बुलवाया और वहाँ प्रथम बार महावीर के उपदेशों को द्वारशांग के रूप में व्यवस्थित कर चार अनुयोगों में वर्गीकृत करने का कार्य किया।34 इसके बाद ईसापूर्व प्रथम शताब्दी में आचार्य पुष्पदन्त-भूतबलि, आचार्य गुणधर एवं आचार्य कुन्दकुन्द आदि आचार्यों ने इसे लिपिबद्ध करने का कार्य किया।
40 12
भगवान् महावीर की परम्परा एवं समसामयिक सन्दर्भ