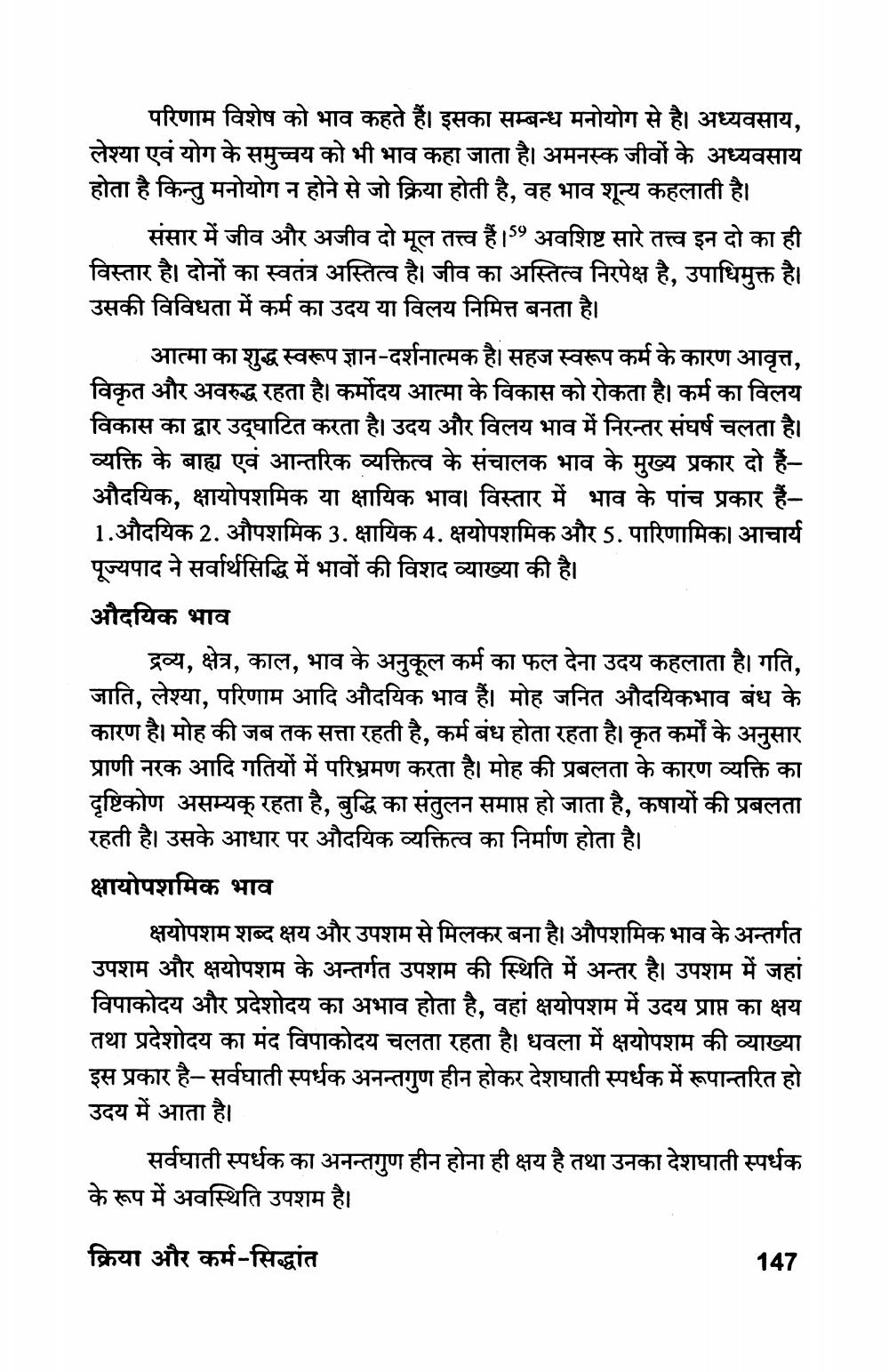________________
परिणाम विशेष को भाव कहते हैं। इसका सम्बन्ध मनोयोग से है। अध्यवसाय, लेश्या एवं योग के समुच्चय को भी भाव कहा जाता है। अमनस्क जीवों के अध्यवसाय होता है किन्तु मनोयोग न होने से जो क्रिया होती है, वह भाव शून्य कहलाती है।
संसार में जीव और अजीव दो मूल तत्त्व हैं।59 अवशिष्ट सारे तत्त्व इन दो का ही विस्तार है। दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है। जीव का अस्तित्व निरपेक्ष है, उपाधिमुक्त है। उसकी विविधता में कर्म का उदय या विलय निमित्त बनता है।
आत्मा का शुद्ध स्वरूप ज्ञान-दर्शनात्मक है। सहज स्वरूप कर्म के कारण आवृत्त, विकृत और अवरुद्ध रहता है। कर्मोदय आत्मा के विकास को रोकता है। कर्म का विलय विकास का द्वार उद्घाटित करता है। उदय और विलय भाव में निरन्तर संघर्ष चलता है। व्यक्ति के बाह्य एवं आन्तरिक व्यक्तित्व के संचालक भाव के मुख्य प्रकार दो हैं
औदयिक, क्षायोपशमिक या क्षायिक भाव। विस्तार में भाव के पांच प्रकार हैं1.औदयिक 2. औपशमिक 3. क्षायिक 4. क्षयोपशमिक और 5. पारिणामिका आचार्य पूज्यपाद ने सर्वार्थसिद्धि में भावों की विशद व्याख्या की है। औदयिक भाव
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुकूल कर्म का फल देना उदय कहलाता है। गति, जाति, लेश्या, परिणाम आदि औदयिक भाव हैं। मोह जनित औदयिकभाव बंध के कारण है। मोह की जब तक सत्ता रहती है, कर्म बंध होता रहता है। कृत कर्मों के अनुसार प्राणी नरक आदि गतियों में परिभ्रमण करता है। मोह की प्रबलता के कारण व्यक्ति का दृष्टिकोण असम्यक् रहता है, बुद्धि का संतुलन समाप्त हो जाता है, कषायों की प्रबलता रहती है। उसके आधार पर औदयिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। क्षायोपशमिक भाव
क्षयोपशम शब्द क्षय और उपशम से मिलकर बना है। औपशमिक भाव के अन्तर्गत उपशम और क्षयोपशम के अन्तर्गत उपशम की स्थिति में अन्तर है। उपशम में जहां विपाकोदय और प्रदेशोदय का अभाव होता है, वहां क्षयोपशम में उदय प्राप्त का क्षय तथा प्रदेशोदय का मंद विपाकोदय चलता रहता है। धवला में क्षयोपशम की व्याख्या इस प्रकार है-सर्वघाती स्पर्धक अनन्तगुण हीन होकर देशघाती स्पर्धक में रूपान्तरित हो उदय में आता है।
सर्वघाती स्पर्धक का अनन्तगण हीन होना ही क्षय है तथा उनका देशघाती स्पर्धक के रूप में अवस्थिति उपशम है।
क्रिया और कर्म-सिद्धांत
147