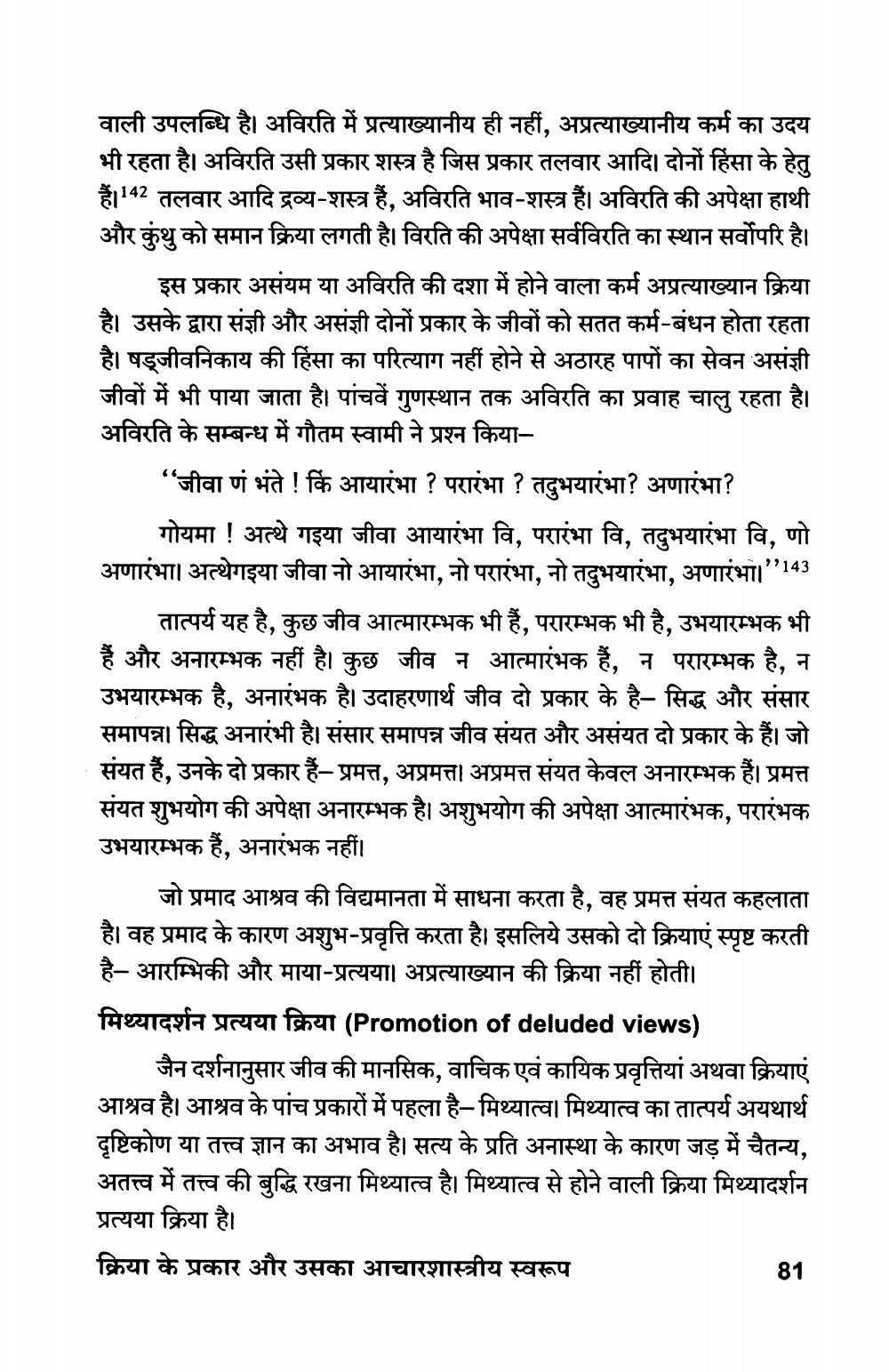________________
वाली उपलब्धि है। अविरति में प्रत्याख्यानीय ही नहीं, अप्रत्याख्यानीय कर्म का उदय भी रहता है। अविरति उसी प्रकार शस्त्र है जिस प्रकार तलवार आदि। दोनों हिंसा के हेतु हैं।142 तलवार आदि द्रव्य-शस्त्र हैं, अविरति भाव-शस्त्र हैं। अविरति की अपेक्षा हाथी और कुंथु को समान क्रिया लगती है। विरति की अपेक्षा सर्वविरति का स्थान सर्वोपरि है। ___ इस प्रकार असंयम या अविरति की दशा में होने वाला कर्म अप्रत्याख्यान क्रिया है। उसके द्वारा संज्ञी और असंज्ञी दोनों प्रकार के जीवों को सतत कर्म-बंधन होता रहता है। षड्जीवनिकाय की हिंसा का परित्याग नहीं होने से अठारह पापों का सेवन असंज्ञी जीवों में भी पाया जाता है। पांचवें गुणस्थान तक अविरति का प्रवाह चालु रहता है। अविरति के सम्बन्ध में गौतम स्वामी ने प्रश्न किया
"जीवा णं भंते ! किं आयारंभा ? परारंभा ? तदुभयारंभा? अणारंभा?
गोयमा ! अत्थे गइया जीवा आयारंभा वि, परारंभा वि, तदुभयारंभा वि, णो अणारंभा। अत्थेगइया जीवा नो आयारंभा, नो परारंभा, नो तदुभयारंभा, अणारंभा।" 143
तात्पर्य यह है, कुछ जीव आत्मारम्भक भी हैं, परारम्भक भी है, उभयारम्भक भी हैं और अनारम्भक नहीं है। कुछ जीव न आत्मारंभक हैं, न परारम्भक है, न उभयारम्भक है, अनारंभक है। उदाहरणार्थ जीव दो प्रकार के है- सिद्ध और संसार समापन्न। सिद्ध अनारंभी है। संसार समापन्न जीव संयत और असंयत दो प्रकार के हैं। जो संयत हैं, उनके दो प्रकार हैं-प्रमत्त, अप्रमत्त। अप्रमत्त संयत केवल अनारम्भक हैं। प्रमत्त संयत शुभयोग की अपेक्षा अनारम्भक है। अशुभयोग की अपेक्षा आत्मारंभक, परारंभक उभयारम्भक हैं, अनारंभक नहीं।
जो प्रमाद आश्रव की विद्यमानता में साधना करता है, वह प्रमत्त संयत कहलाता है। वह प्रमाद के कारण अशुभ-प्रवृत्ति करता है। इसलिये उसको दो क्रियाएं स्पृष्ट करती है- आरम्भिकी और माया-प्रत्यया। अप्रत्याख्यान की क्रिया नहीं होती। मिथ्यादर्शन प्रत्यया क्रिया (Promotion of deluded views)
जैन दर्शनानुसार जीव की मानसिक, वाचिक एवं कायिक प्रवृत्तियां अथवा क्रियाएं आश्रव है। आश्रव के पांच प्रकारों में पहला है-मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का तात्पर्य अयथार्थ दृष्टिकोण या तत्त्व ज्ञान का अभाव है। सत्य के प्रति अनास्था के कारण जड़ में चैतन्य, अतत्त्व में तत्त्व की बुद्धि रखना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व से होने वाली क्रिया मिथ्यादर्शन प्रत्यया क्रिया है। क्रिया के प्रकार और उसका आचारशास्त्रीय स्वरूप
81