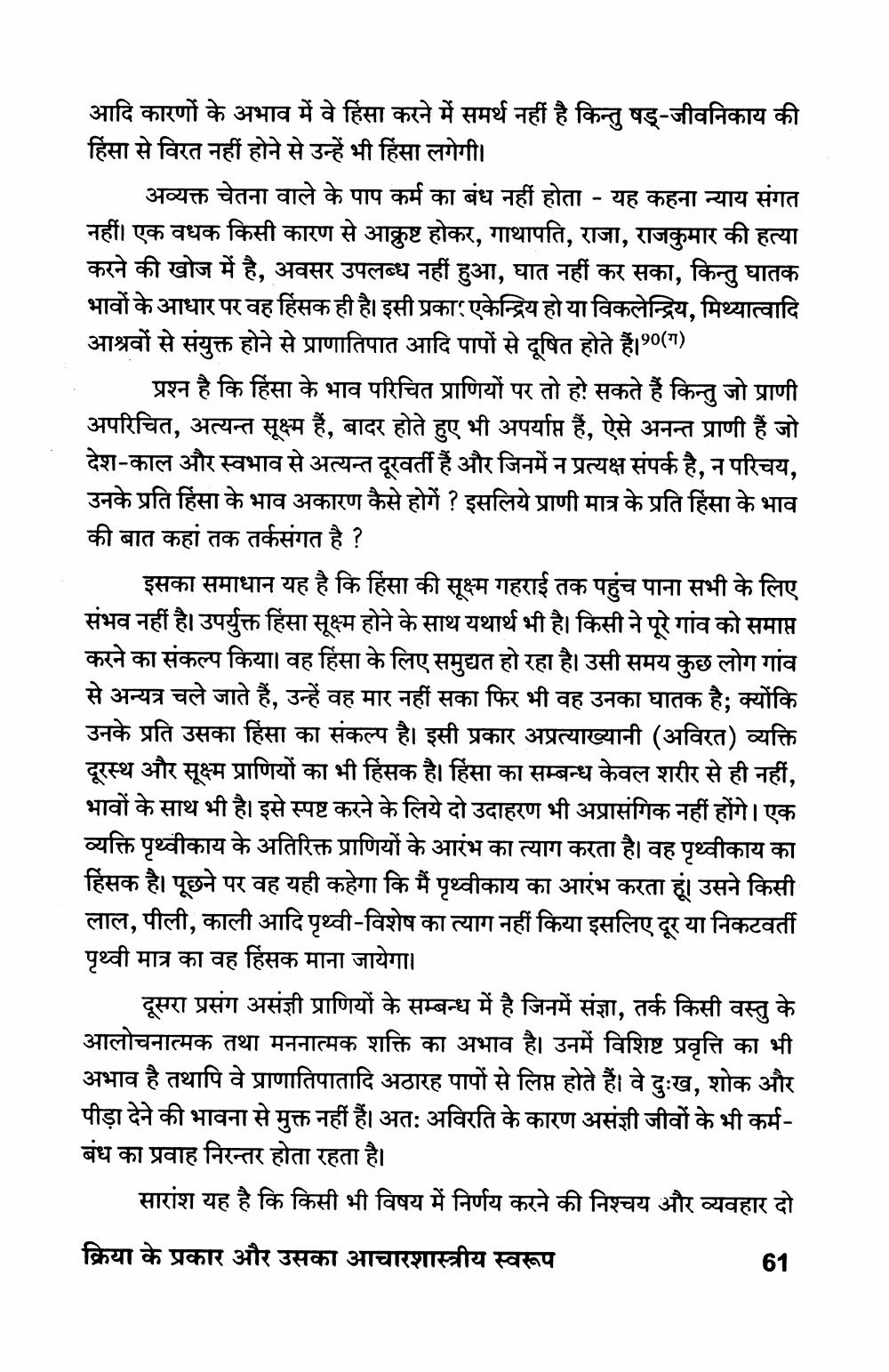________________
आदि कारणों के अभाव में वे हिंसा करने में समर्थ नहीं है किन्तु षड्-जीवनिकाय की हिंसा से विरत नहीं होने से उन्हें भी हिंसा लगेगी।
अव्यक्त चेतना वाले के पाप कर्म का बंध नहीं होता - यह कहना न्याय संगत नहीं। एक वधक किसी कारण से आकृष्ट होकर, गाथापति, राजा, राजकुमार की हत्या करने की खोज में है, अवसर उपलब्ध नहीं हुआ, घात नहीं कर सका, किन्तु घातक भावों के आधार पर वह हिंसक ही है। इसी प्रकार एकेन्द्रिय हो या विकलेन्द्रिय, मिथ्यात्वादि आश्रवों से संयुक्त होने से प्राणातिपात आदि पापों से दूषित होते हैं। 90(ग)
प्रश्न है कि हिंसा के भाव परिचित प्राणियों पर तो हो सकते हैं किन्तु जो प्राणी अपरिचित, अत्यन्त सूक्ष्म हैं, बादर होते हुए भी अपर्याप्त हैं, ऐसे अनन्त प्राणी हैं जो देश-काल और स्वभाव से अत्यन्त दूरवर्ती हैं और जिनमें न प्रत्यक्ष संपर्क है, न परिचय, उनके प्रति हिंसा के भाव अकारण कैसे होगें ? इसलिये प्राणी मात्र के प्रति हिंसा के भाव की बात कहां तक तर्कसंगत है ?
इसका समाधान यह है कि हिंसा की सूक्ष्म गहराई तक पहुंच पाना सभी के लिए संभव नहीं है। उपर्युक्त हिंसा सूक्ष्म होने के साथ यथार्थ भी है। किसी ने पूरे गांव को समाप्त करने का संकल्प किया। वह हिंसा के लिए समुद्यत हो रहा है। उसी समय कुछ लोग गांव से अन्यत्र चले जाते हैं, उन्हें वह मार नहीं सका फिर भी वह उनका घातक है; क्योंकि उनके प्रति उसका हिंसा का संकल्प है। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानी (अविरत) व्यक्ति दूरस्थ और सूक्ष्म प्राणियों का भी हिंसक है। हिंसा का सम्बन्ध केवल शरीर से ही नहीं, भावों के साथ भी है। इसे स्पष्ट करने के लिये दो उदाहरण भी अप्रासंगिक नहीं होंगे। एक व्यक्ति पृथ्वीकाय के अतिरिक्त प्राणियों के आरंभ का त्याग करता है। वह पृथ्वीकाय का हिंसक है। पूछने पर वह यही कहेगा कि मैं पृथ्वीकाय का आरंभ करता हूं। उसने किसी लाल, पीली, काली आदि पृथ्वी-विशेष का त्याग नहीं किया इसलिए दूर या निकटवर्ती पृथ्वी मात्र का वह हिंसक माना जायेगा।
__दूसरा प्रसंग असंज्ञी प्राणियों के सम्बन्ध में है जिनमें संज्ञा, तर्क किसी वस्तु के आलोचनात्मक तथा मननात्मक शक्ति का अभाव है। उनमें विशिष्ट प्रवृत्ति का भी अभाव है तथापि वे प्राणातिपातादि अठारह पापों से लिप्त होते हैं। वे दुःख, शोक और पीड़ा देने की भावना से मुक्त नहीं हैं। अत: अविरति के कारण असंज्ञी जीवों के भी कर्मबंध का प्रवाह निरन्तर होता रहता है।
सारांश यह है कि किसी भी विषय में निर्णय करने की निश्चय और व्यवहार दो क्रिया के प्रकार और उसका आचारशास्त्रीय स्वरूप
61