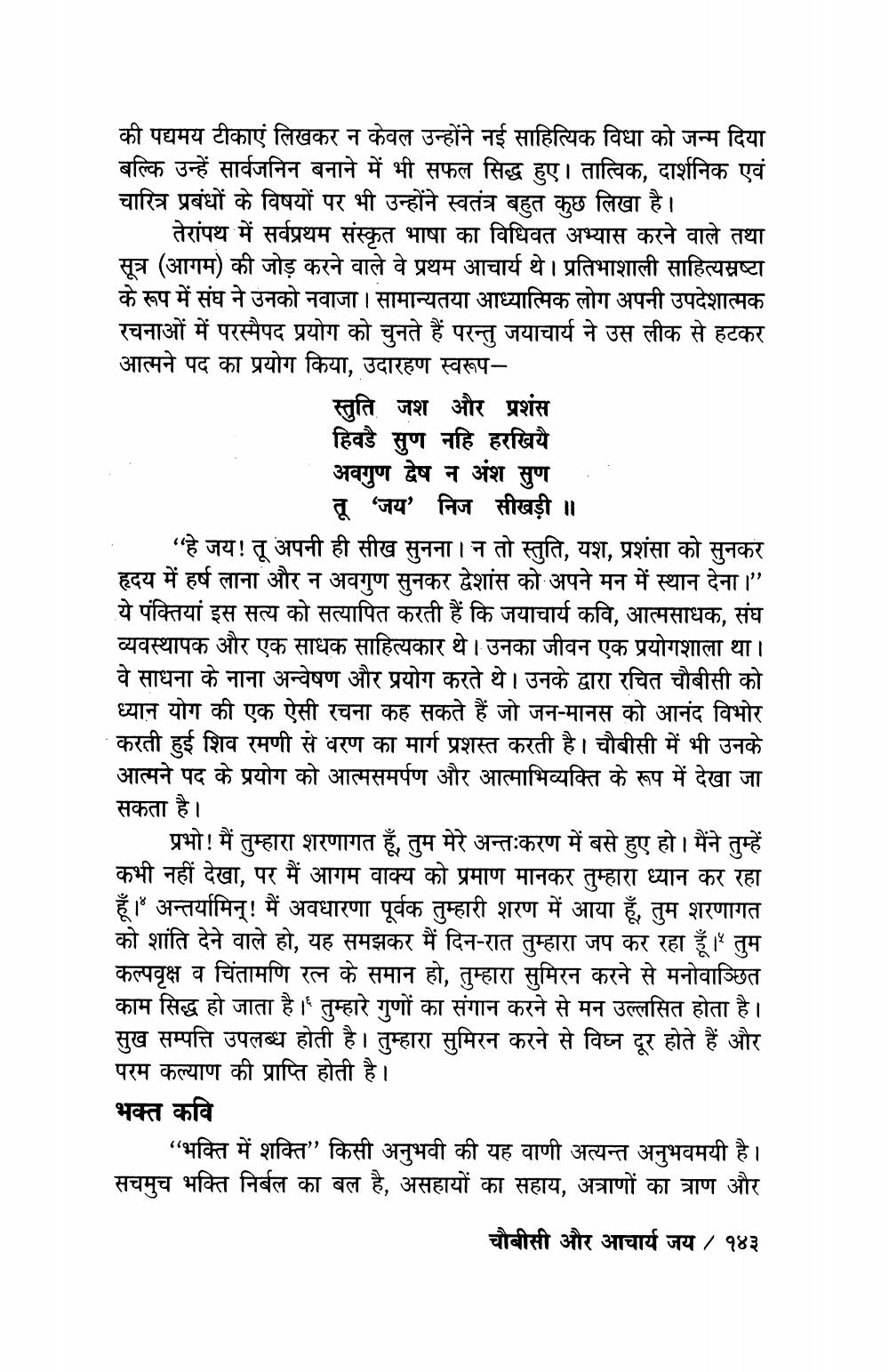________________
की पद्यमय टीकाएं लिखकर न केवल उन्होंने नई साहित्यिक विधा को जन्म दिया बल्कि उन्हें सार्वजनिन बनाने में भी सफल सिद्ध हुए। तात्विक, दार्शनिक एवं चारित्र प्रबंधों के विषयों पर भी उन्होंने स्वतंत्र बहुत कुछ लिखा है।
तेरांपथ में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का विधिवत अभ्यास करने वाले तथा सूत्र (आगम) की जोड़ करने वाले वे प्रथम आचार्य थे। प्रतिभाशाली साहित्यस्रष्टा के रूप में संघ ने उनको नवाजा। सामान्यतया आध्यात्मिक लोग अपनी उपदेशात्मक रचनाओं में परस्मैपद प्रयोग को चुनते हैं परन्तु जयाचार्य ने उस लीक से हटकर आत्मने पद का प्रयोग किया, उदारहण स्वरूप
स्तुति जश और प्रशंस हिवडै सुण नहि हरखियै अवगुण द्वेष न अंश सुण
तू 'जय' निज सीखड़ी ॥ "हे जय! तू अपनी ही सीख सुनना। न तो स्तुति, यश, प्रशंसा को सुनकर हृदय में हर्ष लाना और न अवगुण सुनकर देशांस को अपने मन में स्थान देना।" ये पंक्तियां इस सत्य को सत्यापित करती हैं कि जयाचार्य कवि, आत्मसाधक, संघ व्यवस्थापक और एक साधक साहित्यकार थे। उनका जीवन एक प्रयोगशाला था। वे साधना के नाना अन्वेषण और प्रयोग करते थे। उनके द्वारा रचित चौबीसी को ध्यान योग की एक ऐसी रचना कह सकते हैं जो जन-मानस को आनंद विभोर करती हुई शिव रमणी से वरण का मार्ग प्रशस्त करती है। चौबीसी में भी उनके आत्मने पद के प्रयोग को आत्मसमर्पण और आत्माभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है।
प्रभो! मैं तुम्हारा शरणागत हूँ, तुम मेरे अन्तःकरण में बसे हुए हो। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, पर मैं आगम वाक्य को प्रमाण मानकर तुम्हारा ध्यान कर रहा हूँ। अन्तर्यामिन् ! मैं अवधारणा पूर्वक तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम शरणागत को शांति देने वाले हो, यह समझकर मैं दिन-रात तुम्हारा जप कर रहा हूँ। तुम कल्पवृक्ष व चिंतामणि रत्न के समान हो, तुम्हारा सुमिरन करने से मनोवाञ्छित काम सिद्ध हो जाता है। तुम्हारे गुणों का संगान करने से मन उल्लसित होता है। सुख सम्पत्ति उपलब्ध होती है। तुम्हारा सुमिरन करने से विघ्न दूर होते हैं और परम कल्याण की प्राप्ति होती है। भक्त कवि
"भक्ति में शक्ति' किसी अनुभवी की यह वाणी अत्यन्त अनुभवमयी है। सचमुच भक्ति निर्बल का बल है, असहायों का सहाय, अत्राणों का त्राण और
चौबीसी और आचार्य जय / १४३