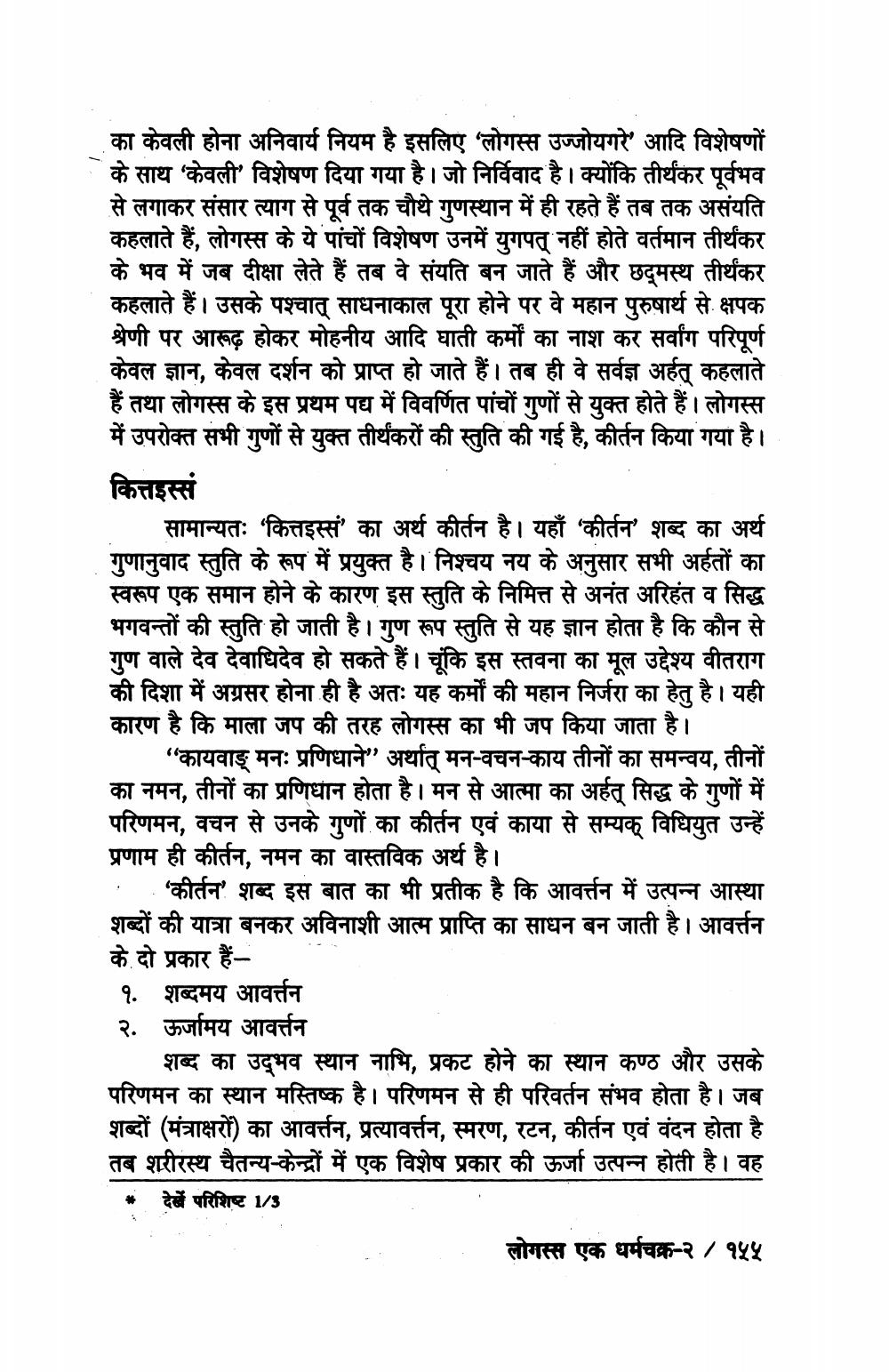________________
. का केवली होना अनिवार्य नियम है इसलिए 'लोगस्स उज्जोयगरे' आदि विशेषणों के साथ 'केवली' विशेषण दिया गया है। जो निर्विवाद है। क्योंकि तीर्थंकर पूर्वभव से लगाकर संसार त्याग से पूर्व तक चौथे गुणस्थान में ही रहते हैं तब तक असंयति कहलाते हैं, लोगस्स के ये पांचों विशेषण उनमें युगपत् नहीं होते वर्तमान तीर्थंकर के भव में जब दीक्षा लेते हैं तब वे संयति बन जाते हैं और छद्मस्थ तीर्थंकर कहलाते हैं । उसके पश्चात् साधनाकाल पूरा होने पर वे महान पुरुषार्थ से क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर मोहनीय आदि घाती कर्मों का नाश कर सर्वांग परिपूर्ण केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त हो जाते हैं । तब ही वे सर्वज्ञ अर्हतु कहलाते हैं तथा लोगस्स के इस प्रथम पद्य में विवर्णित पांचों गुणों से युक्त होते हैं। लोगस्स उपरोक्त सभी गुणों से युक्त तीर्थंकरों की स्तुति की गई है, कीर्तन किया गया है। कित्तइस्सं
सामान्यतः 'कित्तइस्सं' का अर्थ कीर्तन है । यहाँ 'कीर्तन' शब्द का अर्थ गुणानुवाद स्तुति के रूप में प्रयुक्त है। निश्चय नय के अनुसार सभी अर्हतों का स्वरूप एक समान होने के कारण इस स्तुति के निमित्त से अनंत अरिहंत व सिद्ध भगवन्तों की स्तुति हो जाती है। गुण रूप स्तुति से यह ज्ञान होता है कि कौन से गुण वाले देव देवाधिदेव हो सकते हैं। चूंकि इस स्तवना का मूल उद्देश्य वीतराग की दिशा में अग्रसर होना ही है अतः यह कर्मों की महान निर्जरा का हेतु है । यही कारण है कि माला जप की तरह लोगस्स का भी जप किया जाता है ।
“कायवाङ् मनः प्रणिधाने" अर्थात् मन-वचन-काय तीनों का समन्वय, तीनों का नमन, तीनों का प्रणिधान होता है । मन से आत्मा का अर्हत् सिद्ध के गुणों में परिणमन, वचन से उनके गुणों का कीर्तन एवं काया से सम्यक् विधियुत उन्हें प्रणाम ही कीर्तन, नमन का वास्तविक अर्थ है ।
'कीर्तन' शब्द इस बात का भी प्रतीक है कि आवर्त्तन में उत्पन्न आस्था शब्दों की यात्रा बनकर अविनाशी आत्म प्राप्ति का साधन बन जाती है । आवर्त्तन के दो प्रकार हैं
1
१.
शब्दमय आवर्त्तन २. ऊर्जामय आवर्त्तन
शब्द का उद्भव स्थान नाभि, प्रकट होने का स्थान कण्ठ और उसके परिणमन का स्थान मस्तिष्क है। परिणमन से ही परिवर्तन संभव होता है । जब शब्दों (मंत्राक्षरों) का आवर्त्तन, प्रत्यावर्त्तन, स्मरण, रटन, कीर्तन एवं वंदन होता है तब शरीरस्थ चैतन्य - केन्द्रों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह
देखें परिशिष्ट 1/3
*
लोगस्स एक धर्मचक्र - २ / १५५