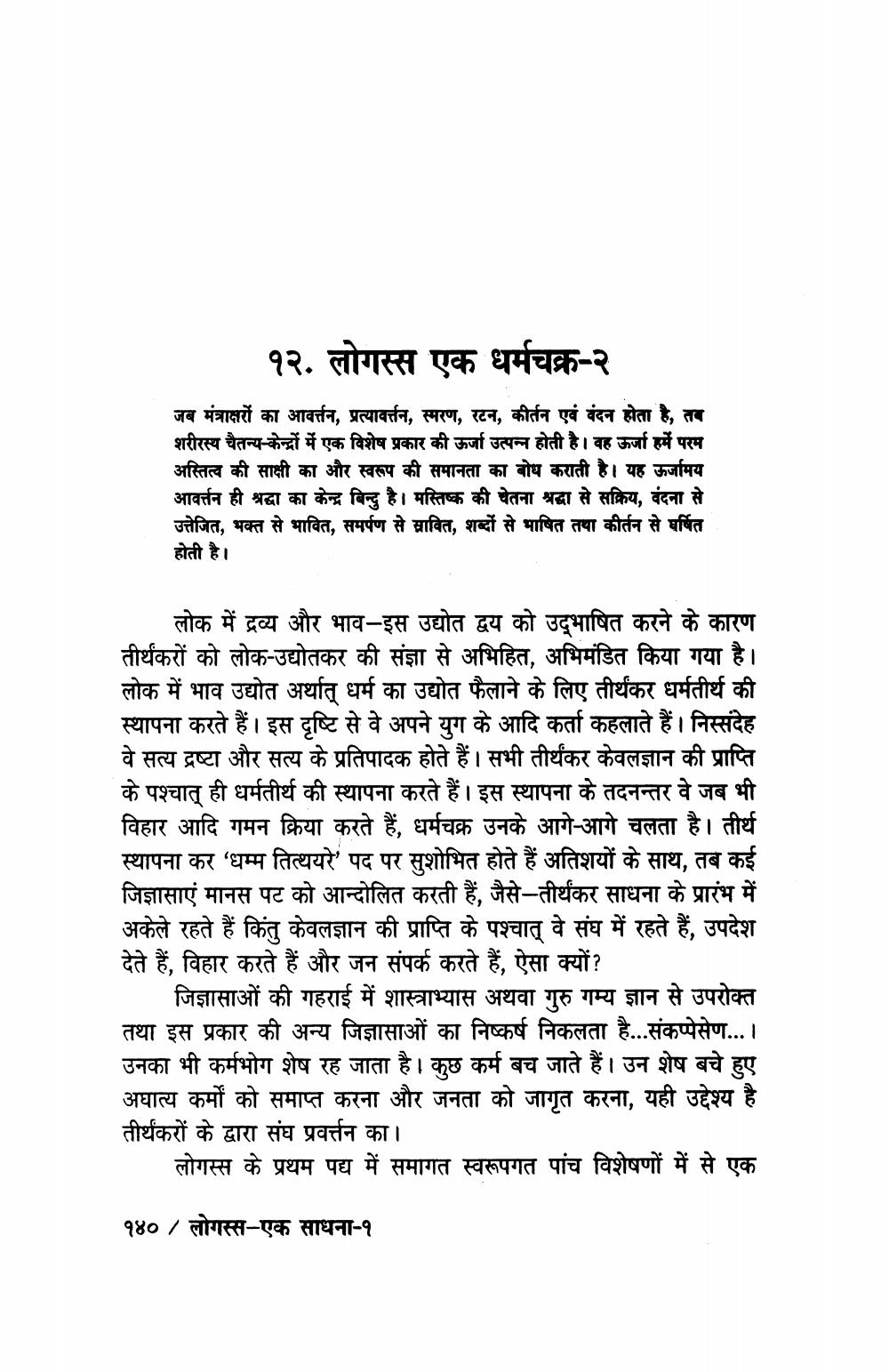________________
१२. लोगस्स एक धर्मचक्र - २
जब मंत्राक्षरों का आवर्त्तन, प्रत्यावर्त्तन, स्मरण, रटन, कीर्तन एवं वंदन होता है, तब शरीरस्य चैतन्य-केन्द्रों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह ऊर्जा हमें परम अस्तित्व की साक्षी का और स्वरूप की समानता का बोध कराती है। यह ऊर्जामय आवर्त्तन ही श्रद्धा का केन्द्र बिन्दु है। मस्तिष्क की चेतना श्रद्धा से सक्रिय, वंदना से उत्तेजित, भक्त से भावित, समर्पण से स्रावित, शब्दों से भाषित तथा कीर्तन से घर्षित होती है।
लोक में द्रव्य और भाव - इस उद्योत द्वय को उद्भाषित करने के कारण तीर्थंकरों को लोक- उद्योतकर की संज्ञा से अभिहित, अभिमंडित किया गया है। लोक में भाव उद्योत अर्थात् धर्म का उद्योत फैलाने के लिए तीर्थंकर धर्मतीर्थ की स्थापना करते हैं । इस दृष्टि से वे अपने युग के आदि कर्ता कहलाते हैं । निस्संदेह वे सत्य द्रष्टा और सत्य के प्रतिपादक होते हैं। सभी तीर्थंकर केवलज्ञान की प्राप्ति के पश्चात् ही धर्मतीर्थ की स्थापना करते हैं । इस स्थापना के तदनन्तर वे जब भी विहार आदि गमन क्रिया करते हैं, धर्मचक्र उनके आगे-आगे चलता है। तीर्थ स्थापना कर 'धम्म तित्थयरे' पद पर सुशोभित होते हैं अतिशयों के साथ, तब कई जिज्ञासाएं मानस पट को आन्दोलित करती हैं, जैसे- तीर्थंकर साधना के प्रारंभ में अकेले रहते हैं किंतु केवलज्ञान की प्राप्ति के पश्चात् वे संघ में रहते हैं, उपदेश देते हैं, विहार करते हैं और जन संपर्क करते हैं, ऐसा क्यों?
जिज्ञासाओं की गहराई में शास्त्राभ्यास अथवा गुरु गम्य ज्ञान से उपरोक्त तथा इस प्रकार की अन्य जिज्ञासाओं का निष्कर्ष निकलता है... संकप्पेसेण... । उनका भी कर्मभोग शेष रह जाता है। कुछ कर्म बच जाते हैं। उन शेष बचे हुए अघात्य कर्मों को समाप्त करना और जनता को जागृत करना, यही उद्देश्य है तीर्थंकरों के द्वारा संघ प्रवर्त्तन का ।
लोगस्स के प्रथम पद्य में समागत स्वरूपगत पांच विशेषणों में से एक
१४० / लोगस्स - एक साधना - १