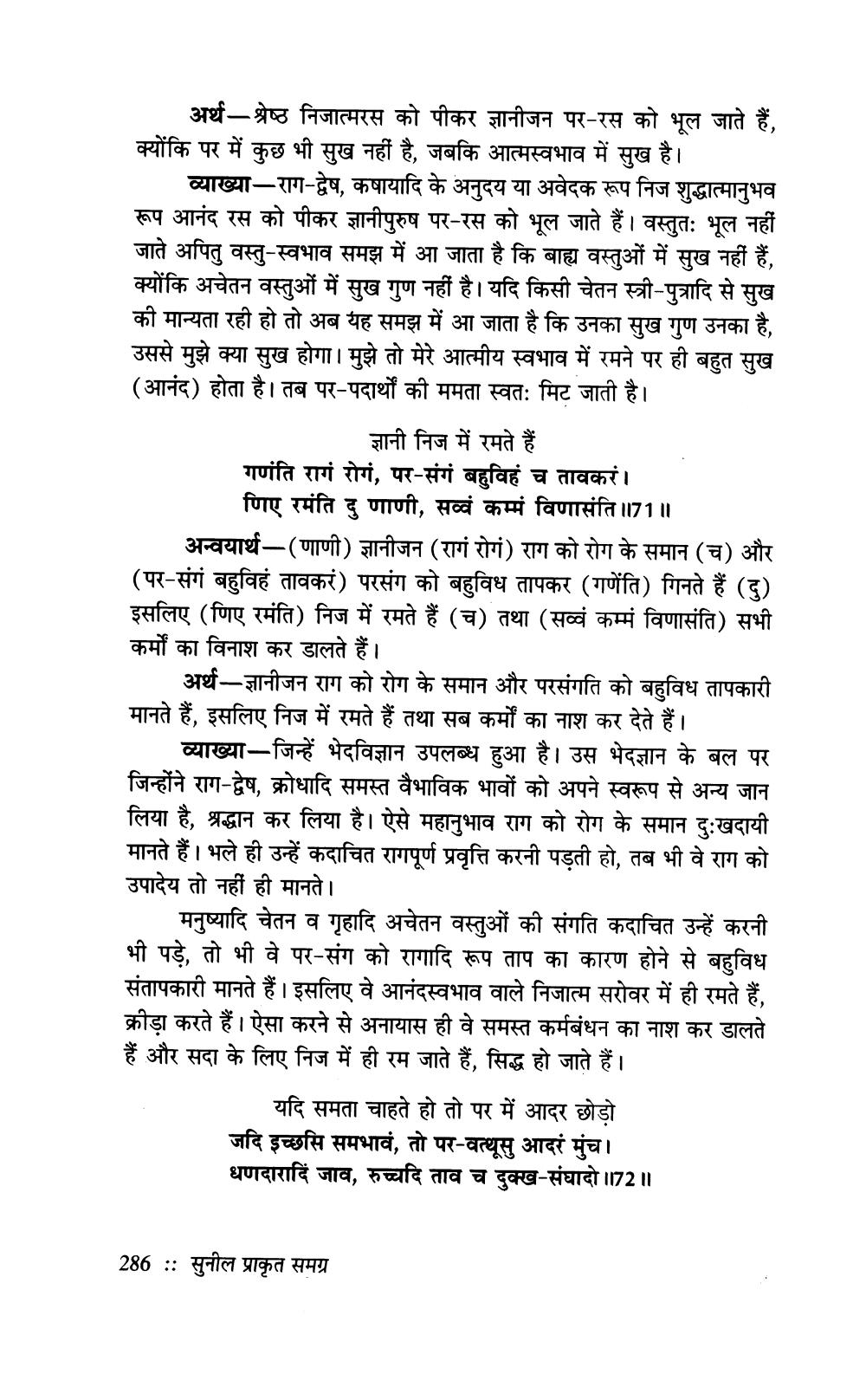________________
अर्थ- श्रेष्ठ निजात्मरस को पीकर ज्ञानीजन पर-रस को भूल जाते हैं, क्योंकि पर में कुछ भी सुख नहीं है, जबकि आत्मस्वभाव में सुख है।
व्याख्या-राग-द्वेष, कषायादि के अनुदय या अवेदक रूप निज शुद्धात्मानुभव रूप आनंद रस को पीकर ज्ञानीपुरुष पर-रस को भूल जाते हैं। वस्तुतः भूल नहीं जाते अपितु वस्तु-स्वभाव समझ में आ जाता है कि बाह्य वस्तुओं में सुख नहीं हैं, क्योंकि अचेतन वस्तुओं में सुख गुण नहीं है। यदि किसी चेतन स्त्री-पुत्रादि से सुख की मान्यता रही हो तो अब यह समझ में आ जाता है कि उनका सुख गुण उनका है, उससे मुझे क्या सुख होगा। मुझे तो मेरे आत्मीय स्वभाव में रमने पर ही बहुत सुख (आनंद) होता है। तब पर-पदार्थों की ममता स्वतः मिट जाती है।
ज्ञानी निज में रमते हैं गणंति रागं रोगं, पर-संगं बहुविहं च तावकरं।
णिए रमंति दु णाणी, सव्वं कम्मं विणासंति ॥71॥ अन्वयार्थ-(णाणी) ज्ञानीजन (रागं रोगं) राग को रोग के समान (च) और (पर-संगं बहुविहं तावकरं) परसंग को बहुविध तापकर (गणेति) गिनते हैं (दु) इसलिए (णिए रमंति) निज में रमते हैं (च) तथा (सव्वं कम्मं विणासंति) सभी कर्मों का विनाश कर डालते हैं।
अर्थ-ज्ञानीजन राग को रोग के समान और परसंगति को बहुविध तापकारी मानते हैं, इसलिए निज में रमते हैं तथा सब कर्मों का नाश कर देते हैं।
व्याख्या-जिन्हें भेदविज्ञान उपलब्ध हुआ है। उस भेदज्ञान के बल पर जिन्होंने राग-द्वेष, क्रोधादि समस्त वैभाविक भावों को अपने स्वरूप से अन्य जान लिया है, श्रद्धान कर लिया है। ऐसे महानुभाव राग को रोग के समान दुःखदायी मानते हैं। भले ही उन्हें कदाचित रागपूर्ण प्रवृत्ति करनी पड़ती हो, तब भी वे राग को उपादेय तो नहीं ही मानते।
मनुष्यादि चेतन व गृहादि अचेतन वस्तुओं की संगति कदाचित उन्हें करनी भी पड़े, तो भी वे पर-संग को रागादि रूप ताप का कारण होने से बहुविध संतापकारी मानते हैं। इसलिए वे आनंदस्वभाव वाले निजात्म सरोवर में ही रमते हैं, क्रीड़ा करते हैं। ऐसा करने से अनायास ही वे समस्त कर्मबंधन का नाश कर डालते हैं और सदा के लिए निज में ही रम जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं।
यदि समता चाहते हो तो पर में आदर छोड़ो जदि इच्छसि समभावं, तो पर-वत्थूसु आदरं मुंच। धणदारादिं जाव, रुच्चदि ताव च दुक्ख-संघादो॥72॥
286 :: सुनील प्राकृत समग्र