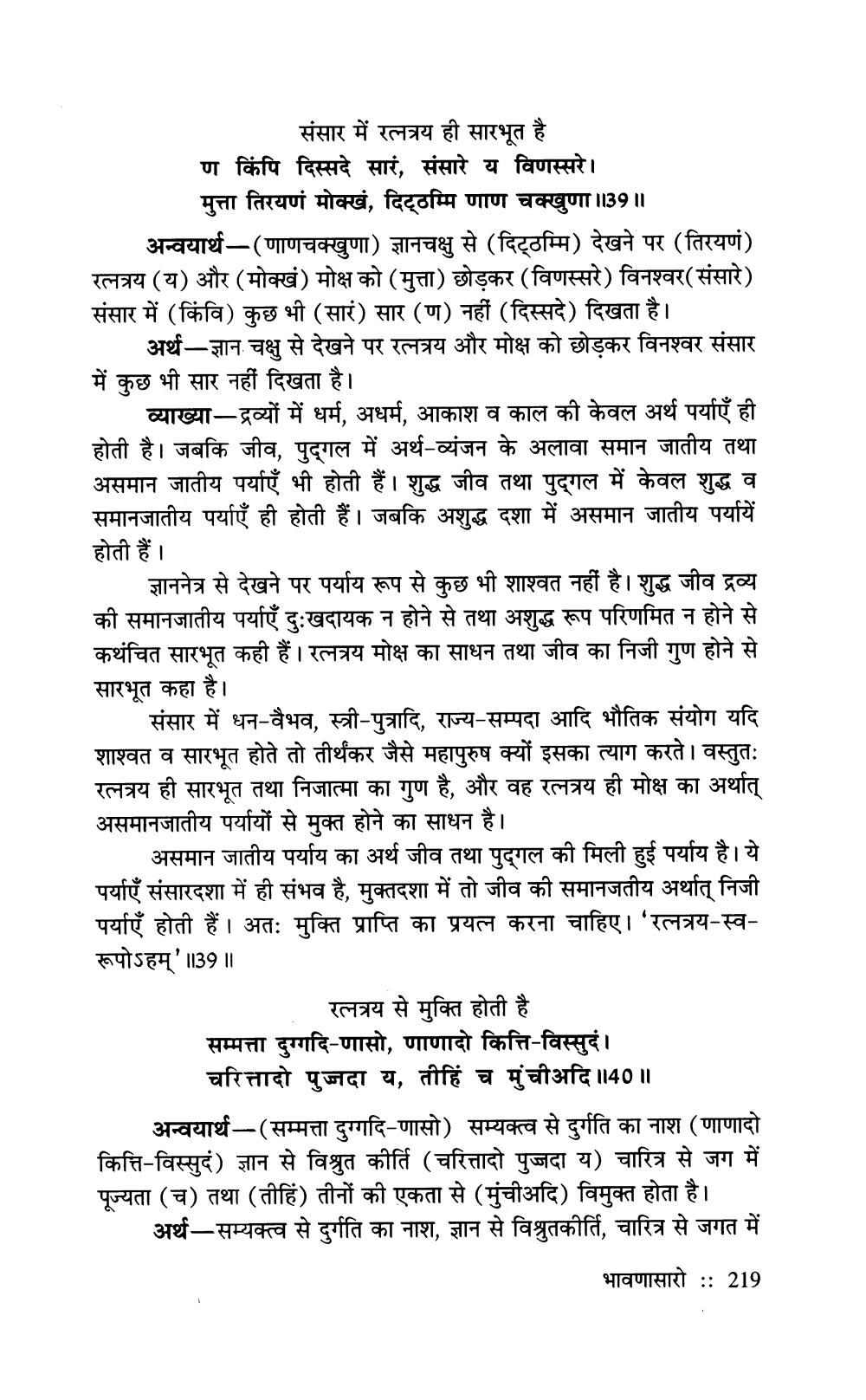________________
संसार में रत्नत्रय ही सारभूत है ण किंपि दिस्सदे सारं, संसारे य विणस्सरे।
मुत्ता तिरयणं मोक्खं, दिट्ठम्मि णाण चक्खुणा ॥39॥ अन्वयार्थ-(णाणचक्खुणा) ज्ञानचक्षु से (दिट्ठम्मि) देखने पर (तिरयणं) रत्नत्रय (य) और (मोक्खं) मोक्ष को (मुत्ता) छोड़कर (विणस्सरे) विनश्वर(संसारे) संसार में (किंवि) कुछ भी (सारं) सार (ण) नहीं (दिस्सदे) दिखता है।
अर्थ-ज्ञान चक्षु से देखने पर रत्नत्रय और मोक्ष को छोड़कर विनश्वर संसार में कुछ भी सार नहीं दिखता है।
व्याख्या-द्रव्यों में धर्म, अधर्म, आकाश व काल की केवल अर्थ पर्याएँ ही होती है। जबकि जीव, पुद्गल में अर्थ-व्यंजन के अलावा समान जातीय तथा असमान जातीय पर्याएँ भी होती हैं। शुद्ध जीव तथा पुद्गल में केवल शुद्ध व समानजातीय पर्याएँ ही होती हैं। जबकि अशुद्ध दशा में असमान जातीय पर्यायें होती हैं।
ज्ञाननेत्र से देखने पर पर्याय रूप से कुछ भी शाश्वत नहीं है। शुद्ध जीव द्रव्य की समानजातीय पर्याएँ दुःखदायक न होने से तथा अशुद्ध रूप परिणमित न होने से कथंचित सारभूत कही हैं। रत्नत्रय मोक्ष का साधन तथा जीव का निजी गुण होने से सारभूत कहा है।
संसार में धन-वैभव, स्त्री-पुत्रादि, राज्य-सम्पदा आदि भौतिक संयोग यदि शाश्वत व सारभूत होते तो तीर्थंकर जैसे महापुरुष क्यों इसका त्याग करते। वस्तुतः रत्नत्रय ही सारभूत तथा निजात्मा का गुण है, और वह रत्नत्रय ही मोक्ष का अर्थात् असमानजातीय पर्यायों से मुक्त होने का साधन है।
असमान जातीय पर्याय का अर्थ जीव तथा पुद्गल की मिली हुई पर्याय है। ये पर्याएँ संसारदशा में ही संभव है, मुक्तदशा में तो जीव की समानजतीय अर्थात् निजी पर्याएँ होती हैं। अतः मुक्ति प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। 'रत्नत्रय-स्वरूपोऽहम्' ॥39॥
रत्नत्रय से मुक्ति होती है सम्मत्ता दुग्गदि-णासो, णाणादो कित्ति-विस्सुदं।
चरित्तादो पुजदा य, तीहिं च मुंचीअदि ॥40॥ अन्वयार्थ-(सम्मत्ता दुग्गदि-णासो) सम्यक्त्व से दुर्गति का नाश (णाणादो कित्ति-विस्सुदं) ज्ञान से विश्रुत कीर्ति (चरित्तादो पुजदा य) चारित्र से जग में पूज्यता (च) तथा (तीहिं) तीनों की एकता से (मुंचीअदि) विमुक्त होता है।
अर्थ-सम्यक्त्व से दुर्गति का नाश, ज्ञान से विश्रुतकीर्ति, चारित्र से जगत में
भावणासारो :: 219