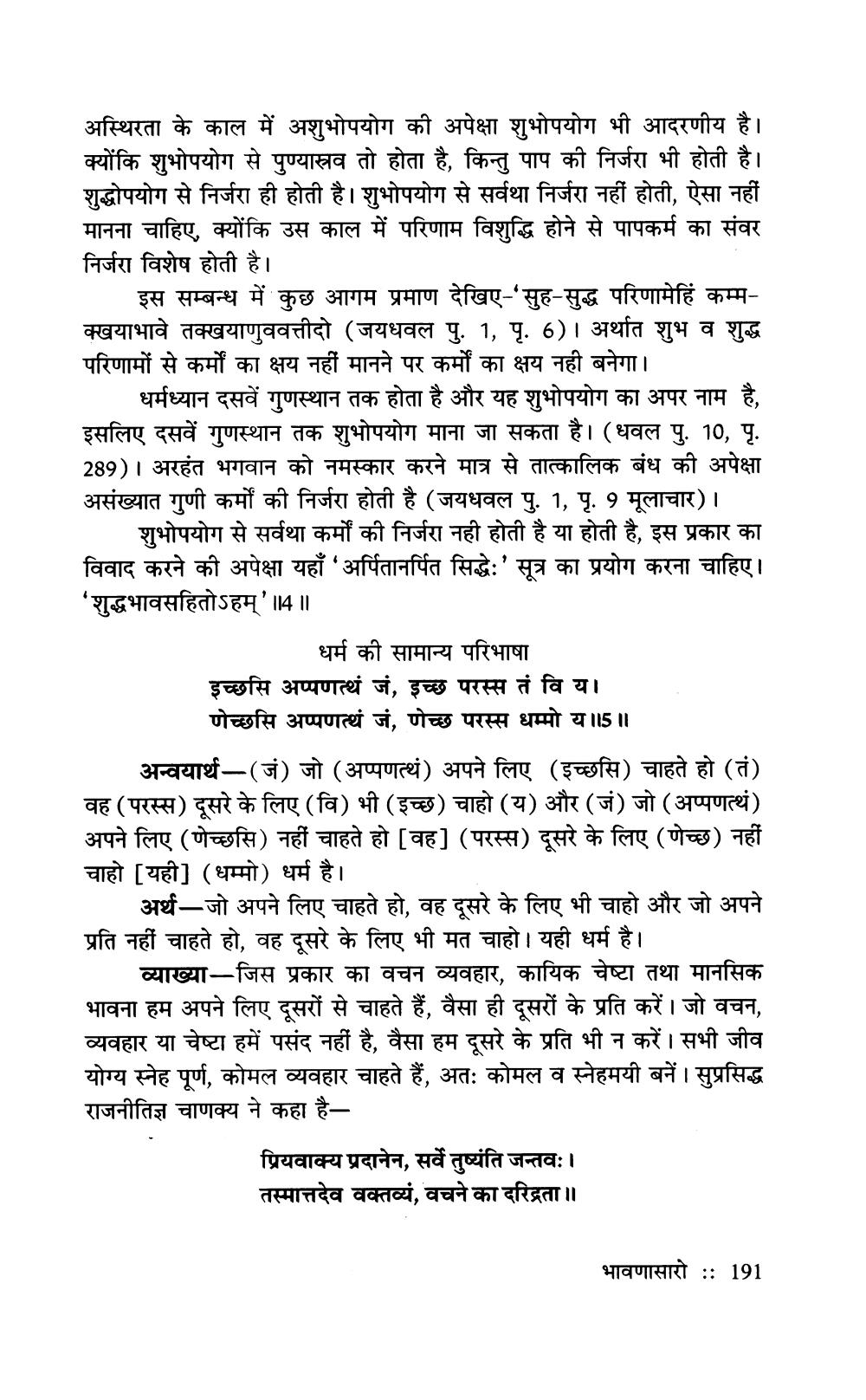________________
अस्थिरता के काल में अशुभोपयोग की अपेक्षा शुभोपयोग भी आदरणीय है। क्योंकि शुभोपयोग से पुण्यास्रव तो होता है, किन्तु पाप की निर्जरा भी होती है। शुद्धोपयोग से निर्जरा ही होती है। शुभोपयोग से सर्वथा निर्जरा नहीं होती, ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उस काल में परिणाम विशुद्धि होने से पापकर्म का संवर निर्जरा विशेष होती है।
इस सम्बन्ध में कुछ आगम प्रमाण देखिए-'सुह-सुद्ध परिणामेहिं कम्मक्खयाभावे तक्खयाणुववत्तीदो (जयधवल पु. 1, पृ. 6)। अर्थात शुभ व शुद्ध परिणामों से कर्मों का क्षय नहीं मानने पर कर्मों का क्षय नही बनेगा।
धर्मध्यान दसवें गुणस्थान तक होता है और यह शुभोपयोग का अपर नाम है, इसलिए दसवें गुणस्थान तक शुभोपयोग माना जा सकता है। (धवल पु. 10, पृ. 289)। अरहंत भगवान को नमस्कार करने मात्र से तात्कालिक बंध की अपेक्षा असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है (जयधवल पु. 1, पृ. 9 मूलाचार)।
शुभोपयोग से सर्वथा कर्मों की निर्जरा नही होती है या होती है, इस प्रकार का विवाद करने की अपेक्षा यहाँ 'अर्पितानर्पित सिद्धेः' सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। 'शुद्धभावसहितोऽहम् ॥4॥
___ धर्म की सामान्य परिभाषा इच्छसि अप्पणत्थं जं, इच्छ परस्स तं वि य।
णेच्छसि अप्पणत्थं जं, णेच्छ परस्स धम्मो य॥5॥ अन्वयार्थ-(जं) जो (अप्पणत्थं) अपने लिए (इच्छसि) चाहते हो (तं) वह (परस्स) दूसरे के लिए (वि) भी (इच्छ) चाहो (य) और (जं) जो (अप्पणत्थं) अपने लिए (णेच्छसि) नहीं चाहते हो [वह] (परस्स) दूसरे के लिए (णेच्छ) नहीं चाहो [यही] (धम्मो) धर्म है।
अर्थ-जो अपने लिए चाहते हो, वह दूसरे के लिए भी चाहो और जो अपने प्रति नहीं चाहते हो, वह दूसरे के लिए भी मत चाहो। यही धर्म है।
व्याख्या-जिस प्रकार का वचन व्यवहार, कायिक चेष्टा तथा मानसिक भावना हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं, वैसा ही दूसरों के प्रति करें। जो वचन, व्यवहार या चेष्टा हमें पसंद नहीं है, वैसा हम दूसरे के प्रति भी न करें। सभी जीव योग्य स्नेह पूर्ण, कोमल व्यवहार चाहते हैं, अतः कोमल व स्नेहमयी बनें। सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चाणक्य ने कहा है
प्रियवाक्य प्रदानेन, सर्वे तुष्यंति जन्तवः । तस्मात्तदेव वक्तव्यं, वचने का दरिद्रता॥
भावणासारो :: 191