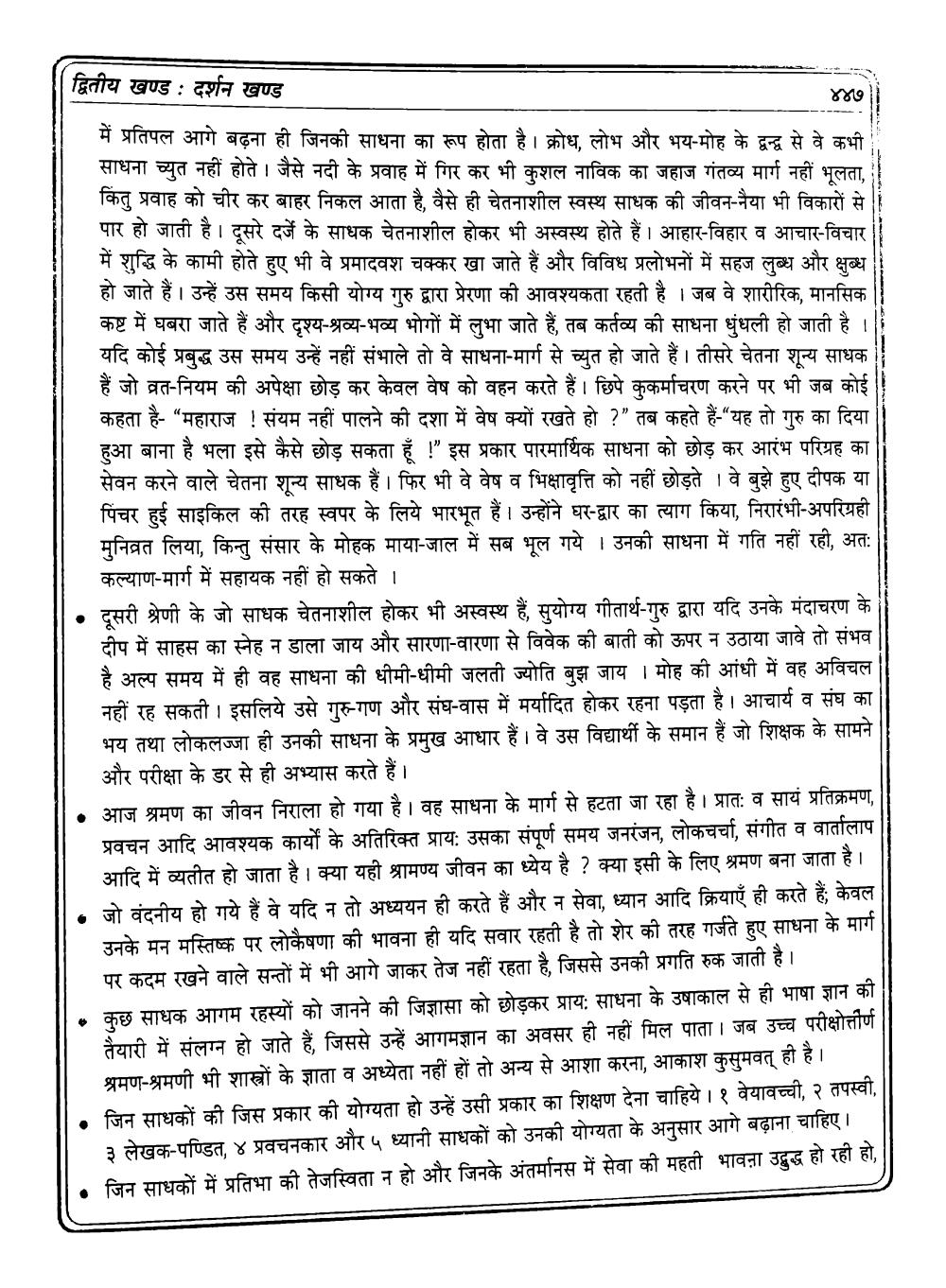________________
द्वितीय खण्ड : दर्शन खण्ड
४४७ में प्रतिपल आगे बढ़ना ही जिनकी साधना का रूप होता है। क्रोध, लोभ और भय-मोह के द्वन्द्व से वे कभी साधना च्युत नहीं होते। जैसे नदी के प्रवाह में गिर कर भी कुशल नाविक का जहाज गंतव्य मार्ग नहीं भूलता, किंतु प्रवाह को चीर कर बाहर निकल आता है, वैसे ही चेतनाशील स्वस्थ साधक की जीवन-नैया भी विकारों से पार हो जाती है। दूसरे दर्जे के साधक चेतनाशील होकर भी अस्वस्थ होते हैं। आहार-विहार व आचार-विचार में शुद्धि के कामी होते हुए भी वे प्रमादवश चक्कर खा जाते हैं और विविध प्रलोभनों में सहज लुब्ध और क्षुब्ध हो जाते हैं। उन्हें उस समय किसी योग्य गुरु द्वारा प्रेरणा की आवश्यकता रहती है । जब वे शारीरिक, मानसिक | कष्ट में घबरा जाते हैं और दृश्य-श्रव्य-भव्य भोगों में लुभा जाते हैं, तब कर्तव्य की साधना धुंधली हो जाती है । यदि कोई प्रबद्ध उस समय उन्हें नहीं संभाले तो वे साधना-मार्ग से च्यत हो जाते हैं। तीसरे चेतना शन्य साधक। हैं जो व्रत-नियम की अपेक्षा छोड़ कर केवल वेष को वहन करते हैं। छिपे कुकर्माचरण करने पर भी जब कोई कहता है- “महाराज ! संयम नहीं पालने की दशा में वेष क्यों रखते हो ?” तब कहते हैं-“यह तो गुरु का दिया हुआ बाना है भला इसे कैसे छोड़ सकता हूँ !” इस प्रकार पारमार्थिक साधना को छोड़ कर आरंभ परिग्रह का सेवन करने वाले चेतना शून्य साधक हैं। फिर भी वे वेष व भिक्षावृत्ति को नहीं छोड़ते । वे बुझे हुए दीपक या पिंचर हुई साइकिल की तरह स्वपर के लिये भारभूत हैं। उन्होंने घर-द्वार का त्याग किया, निरारंभी-अपरिग्रही मुनिव्रत लिया, किन्तु संसार के मोहक माया-जाल में सब भूल गये । उनकी साधना में गति नहीं रही, अत: कल्याण-मार्ग में सहायक नहीं हो सकते ।। दूसरी श्रेणी के जो साधक चेतनाशील होकर भी अस्वस्थ हैं, सुयोग्य गीतार्थ-गुरु द्वारा यदि उनके मंदाचरण के दीप में साहस का स्नेह न डाला जाय और सारणा-वारणा से विवेक की बाती को ऊपर न उठाया जावे तो संभव है अल्प समय में ही वह साधना की धीमी-धीमी जलती ज्योति बुझ जाय । मोह की आंधी में वह अविचल नहीं रह सकती। इसलिये उसे गुरु-गण और संघ-वास में मर्यादित होकर रहना पड़ता है। आचार्य व संघ का भय तथा लोकलज्जा ही उनकी साधना के प्रमुख आधार हैं । वे उस विद्यार्थी के समान हैं जो शिक्षक के सामने और परीक्षा के डर से ही अभ्यास करते हैं। आज श्रमण का जीवन निराला हो गया है। वह साधना के मार्ग से हटता जा रहा है। प्रात: व सायं प्रतिक्रमण, प्रवचन आदि आवश्यक कार्यों के अतिरिक्त प्राय: उसका संपूर्ण समय जनरंजन, लोकचर्चा, संगीत व वार्तालाप
आदि में व्यतीत हो जाता है। क्या यही श्रामण्य जीवन का ध्येय है ? क्या इसी के लिए श्रमण बना जाता है। • जो वंदनीय हो गये हैं वे यदि न तो अध्ययन ही करते हैं और न सेवा, ध्यान आदि क्रियाएँ ही करते हैं; केवल
उनके मन मस्तिष्क पर लोकैषणा की भावना ही यदि सवार रहती है तो शेर की तरह गर्जते हुए साधना के मार्ग
पर कदम रखने वाले सन्तों में भी आगे जाकर तेज नहीं रहता है, जिससे उनकी प्रगति रुक जाती है। • कुछ साधक आगम रहस्यों को जानने की जिज्ञासा को छोड़कर प्राय: साधना के उषाकाल से ही भाषा ज्ञान की ||
तैयारी में संलग्न हो जाते हैं, जिससे उन्हें आगमज्ञान का अवसर ही नहीं मिल पाता। जब उच्च परीक्षोत्तीर्ण |
श्रमण-श्रमणी भी शास्त्रों के ज्ञाता व अध्येता नहीं हों तो अन्य से आशा करना, आकाश कुसुमवत् ही है। • जिन साधकों की जिस प्रकार की योग्यता हो उन्हें उसी प्रकार का शिक्षण देना चाहिये । १ वेयावच्ची, २ तपस्वी, |
३ लेखक-पण्डित, ४ प्रवचनकार और ५ ध्यानी साधकों को उनकी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ाना चाहिए। • जिन साधकों में प्रतिभा की तेजस्विता न हो और जिनके अंतर्मानस में सेवा की महती भावना उद्बुद्ध हो रही हो,
-