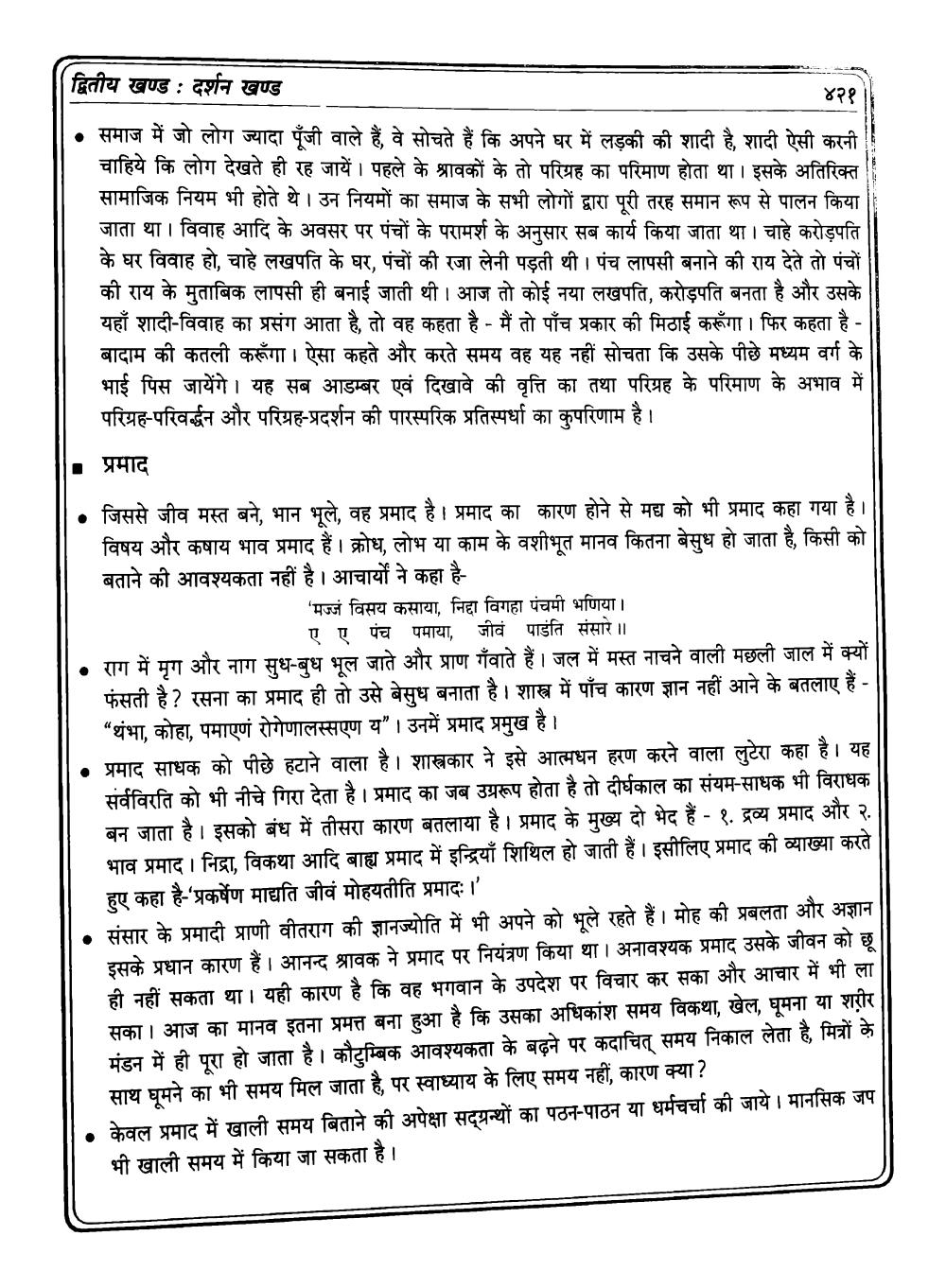________________
द्वितीय खण्ड : दर्शन खण्ड • समाज में जो लोग ज्यादा पूँजी वाले हैं, वे सोचते हैं कि अपने घर में लड़की की शादी है, शादी ऐसी करनी
चाहिये कि लोग देखते ही रह जायें। पहले के श्रावकों के तो परिग्रह का परिमाण होता था। इसके अतिरिक्त सामाजिक नियम भी होते थे। उन नियमों का समाज के सभी लोगों द्वारा पूरी तरह समान रूप से पालन किया जाता था। विवाह आदि के अवसर पर पंचों के परामर्श के अनुसार सब कार्य किया जाता था। चाहे करोड़पति के घर विवाह हो, चाहे लखपति के घर, पंचों की रजा लेनी पड़ती थी। पंच लापसी बनाने की राय देते तो पंचों की राय के मुताबिक लापसी ही बनाई जाती थी। आज तो कोई नया लखपति, करोड़पति बनता है और उसके यहाँ शादी-विवाह का प्रसंग आता है, तो वह कहता है - मैं तो पाँच प्रकार की मिठाई करूँगा। फिर कहता है - बादाम की कतली करूँगा। ऐसा कहते और करते समय वह यह नहीं सोचता कि उसके पीछे मध्यम वर्ग के भाई पिस जायेंगे। यह सब आडम्बर एवं दिखावे की वृत्ति का तथा परिग्रह के परिमाण के अभाव में परिग्रह-परिवर्द्धन और परिग्रह-प्रदर्शन की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का कुपरिणाम है।
प्रमाद
जिससे जीव मस्त बने, भान भूले, वह प्रमाद है। प्रमाद का कारण होने से मद्य को भी प्रमाद कहा गया है। विषय और कषाय भाव प्रमाद हैं। क्रोध, लोभ या काम के वशीभूत मानव कितना बेसुध हो जाता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आचार्यों ने कहा है
'मज्जं विसय कसाया, निद्दा विगहा पंचमी भणिया।
___ ए ए पंच पमाया, जीवं पाडंति संसारे । • राग में मृग और नाग सुध-बुध भूल जाते और प्राण गँवाते हैं। जल में मस्त नाचने वाली मछली जाल में क्यों फंसती है? रसना का प्रमाद ही तो उसे बेसुध बनाता है। शास्त्र में पाँच कारण ज्ञान नहीं आने के बतलाए हैं - "थंभा, कोहा, पमाएणं रोगेणालस्सएण य” । उनमें प्रमाद प्रमुख है। । प्रमाद साधक को पीछे हटाने वाला है। शास्त्रकार ने इसे आत्मधन हरण करने वाला लुटेरा कहा है। यह
सर्वविरति को भी नीचे गिरा देता है। प्रमाद का जब उग्ररूप होता है तो दीर्घकाल का संयम-साधक भी विराधक बन जाता है। इसको बंध में तीसरा कारण बतलाया है। प्रमाद के मुख्य दो भेद हैं - १. द्रव्य प्रमाद और २. भाव प्रमाद । निद्रा, विकथा आदि बाह्य प्रमाद में इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं। इसीलिए प्रमाद की व्याख्या करते हुए कहा है-'प्रकर्षेण माद्यति जीवं मोहयतीति प्रमादः।' संसार के प्रमादी प्राणी वीतराग की ज्ञानज्योति में भी अपने को भूले रहते हैं। मोह की प्रबलता और अज्ञान | इसके प्रधान कारण हैं। आनन्द श्रावक ने प्रमाद पर नियंत्रण किया था। अनावश्यक प्रमाद उसके जीवन को छू ही नहीं सकता था। यही कारण है कि वह भगवान के उपदेश पर विचार कर सका और आचार में भी ला सका। आज का मानव इतना प्रमत्त बना हुआ है कि उसका अधिकांश समय विकथा, खेल, घूमना या शरीर मंडन में ही पूरा हो जाता है। कौटुम्बिक आवश्यकता के बढ़ने पर कदाचित् समय निकाल लेता है, मित्रों के
साथ घूमने का भी समय मिल जाता है, पर स्वाध्याय के लिए समय नहीं, कारण क्या? • केवल प्रमाद में खाली समय बिताने की अपेक्षा सद्ग्रन्थों का पठन-पाठन या धर्मचर्चा की जाये। मानसिक जप
भी खाली समय में किया जा सकता है।