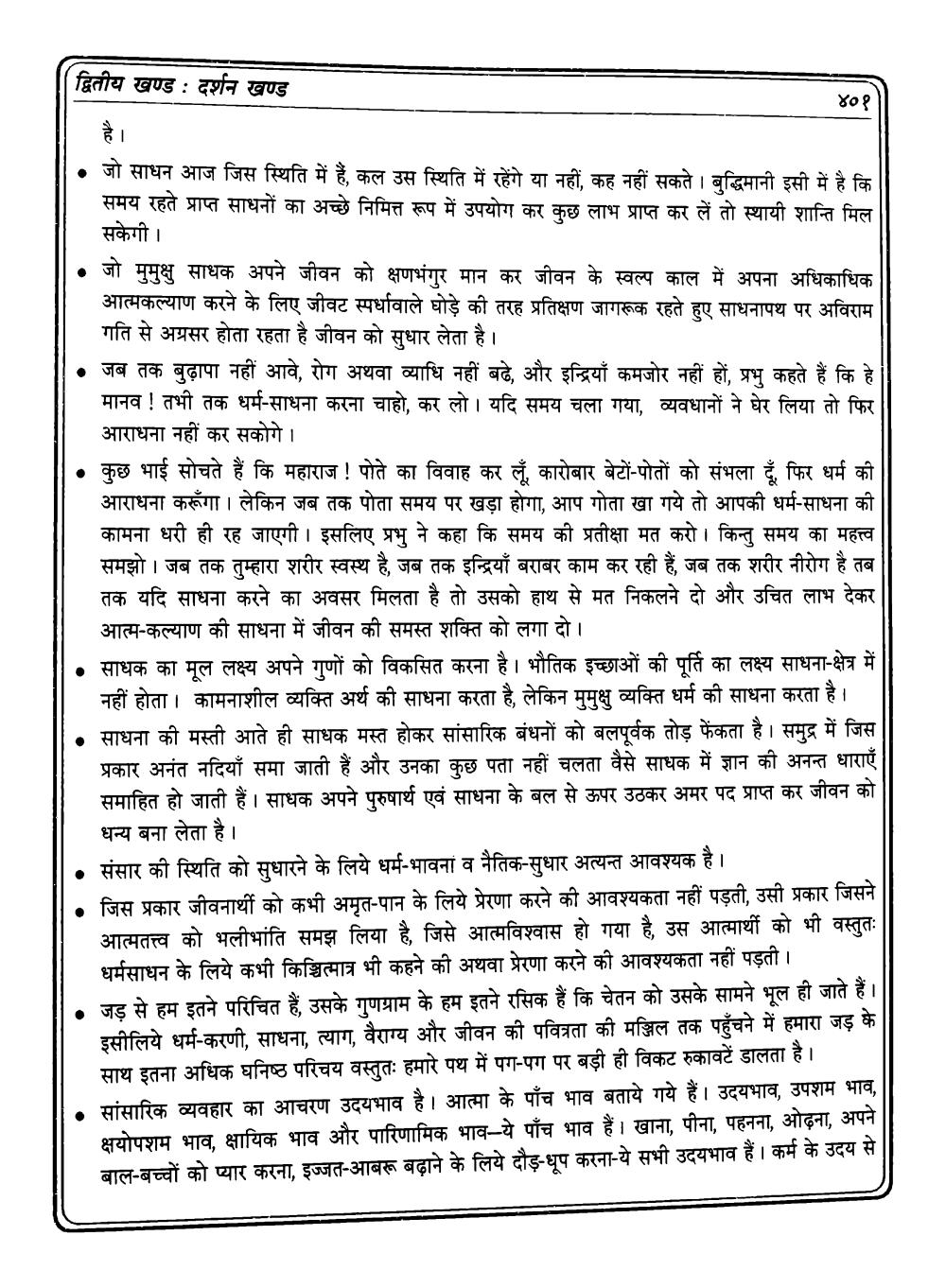________________
द्वितीय खण्ड : दर्शन खण्ड
४०१
• जो साधन आज जिस स्थिति में हैं, कल उस स्थिति में रहेंगे या नहीं, कह नहीं सकते । बुद्धिमानी इसी में है कि
समय रहते प्राप्त साधनों का अच्छे निमित्त रूप में उपयोग कर कुछ लाभ प्राप्त कर लें तो स्थायी शान्ति मिल सकेगी। जो मुमुक्षु साधक अपने जीवन को क्षणभंगुर मान कर जीवन के स्वल्प काल में अपना अधिकाधिक आत्मकल्याण करने के लिए जीवट स्पर्धावाले घोड़े की तरह प्रतिक्षण जागरूक रहते हुए साधनापथ पर अविराम
गति से अग्रसर होता रहता है जीवन को सुधार लेता है। • जब तक बुढ़ापा नहीं आवे, रोग अथवा व्याधि नहीं बढे, और इन्द्रियाँ कमजोर नहीं हों, प्रभु कहते हैं कि हे मानव ! तभी तक धर्म-साधना करना चाहो, कर लो। यदि समय चला गया. व्यवधानों ने घेर लिया तो फिर
आराधना नहीं कर सकोगे। • कुछ भाई सोचते हैं कि महाराज ! पोते का विवाह कर लूँ, कारोबार बेटों-पोतों को संभला दूँ, फिर धर्म की
आराधना करूँगा। लेकिन जब तक पोता समय पर खड़ा होगा, आप गोता खा गये तो आपकी धर्म-साधना की कामना धरी ही रह जाएगी। इसलिए प्रभु ने कहा कि समय की प्रतीक्षा मत करो। किन्तु समय का महत्त्व समझो। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, जब तक इन्द्रियाँ बराबर काम कर रही हैं, जब तक शरीर नीरोग है तब तक यदि साधना करने का अवसर मिलता है तो उसको हाथ से मत निकलने दो और उचित लाभ देकर आत्म-कल्याण की साधना में जीवन की समस्त शक्ति को लगा दो। साधक का मूल लक्ष्य अपने गुणों को विकसित करना है। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का लक्ष्य साधना-क्षेत्र में
नहीं होता। कामनाशील व्यक्ति अर्थ की साधना करता है, लेकिन मुमुक्षु व्यक्ति धर्म की साधना करता है। • साधना की मस्ती आते ही साधक मस्त होकर सांसारिक बंधनों को बलपूर्वक तोड़ फेंकता है। समुद्र में जिस |
प्रकार अनंत नदियाँ समा जाती हैं और उनका कुछ पता नहीं चलता वैसे साधक में ज्ञान की अनन्त धाराएँ | समाहित हो जाती हैं। साधक अपने पुरुषार्थ एवं साधना के बल से ऊपर उठकर अमर पद प्राप्त कर जीवन को | धन्य बना लेता है। संसार की स्थिति को सुधारने के लिये धर्म-भावना व नैतिक-सुधार अत्यन्त आवश्यक है। • जिस प्रकार जीवनार्थी को कभी अमृत-पान के लिये प्रेरणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी प्रकार जिसने |
आत्मतत्त्व को भलीभांति समझ लिया है, जिसे आत्मविश्वास हो गया है, उस आत्मार्थी को भी वस्तुतः धर्मसाधन के लिये कभी किञ्चित्मात्र भी कहने की अथवा प्रेरणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। • जड़ से हम इतने परिचित हैं, उसके गुणग्राम के हम इतने रसिक हैं कि चेतन को उसके सामने भूल ही जाते हैं।
इसीलिये धर्म-करणी, साधना, त्याग, वैराग्य और जीवन की पवित्रता की मञ्जिल तक पहुँचने में हमारा जड़ के साथ इतना अधिक घनिष्ठ परिचय वस्तुतः हमारे पथ में पग-पग पर बड़ी ही विकट रुकावटें डालता है। सांसारिक व्यवहार का आचरण उदयभाव है। आत्मा के पाँच भाव बताये गये हैं। उदयभाव, उपशम भाव, क्षयोपशम भाव, क्षायिक भाव और पारिणामिक भाव-ये पाँच भाव हैं। खाना, पीना, पहनना, ओढ़ना, अपने बाल-बच्चों को प्यार करना, इज्जत-आबरू बढ़ाने के लिये दौड़-धूप करना-ये सभी उदयभाव हैं । कर्म के उदय से