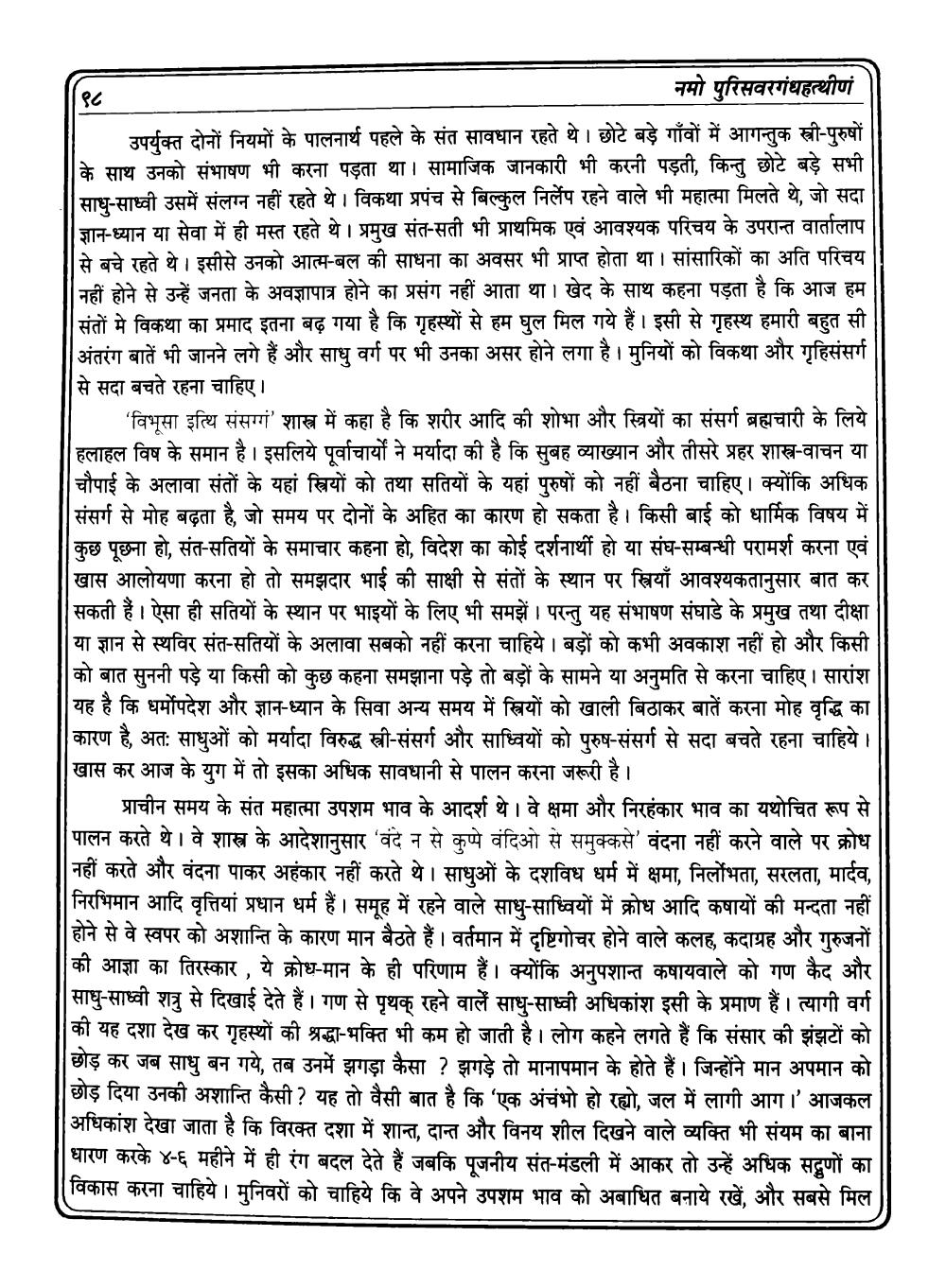________________
गंधहत्थीणं
उपर्युक्त दोनों नियमों के पालनार्थ पहले के संत सावधान रहते थे। छोटे बड़े गाँवों में आगन्तुक स्त्री-पुरुषों के साथ उनको संभाषण भी करना पड़ता था। सामाजिक जानकारी भी करनी पड़ती, किन्तु छोटे बड़े सभी साधु-साध्वी उसमें संलग्न नहीं रहते थे। विकथा प्रपंच से बिल्कुल निर्लेप रहने वाले भी महात्मा मिलते थे, जो सदा ज्ञान-ध्यान या सेवा में ही मस्त रहते थे। प्रमुख संत-सती भी प्राथमिक एवं आवश्यक परिचय के उपरान्त वार्तालाप से बचे रहते थे। इसीसे उनको आत्म-बल की साधना का अवसर भी प्राप्त होता था। सांसारिकों का अति परिचय नहीं होने से उन्हें जनता के अवज्ञापात्र होने का प्रसंग नहीं आता था। खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज हम संतों मे विकथा का प्रमाद इतना बढ़ गया है कि गृहस्थों से हम घुल मिल गये हैं। इसी से गृहस्थ हमारी बहुत सी अंतरंग बातें भी जानने लगे हैं और साधु वर्ग पर भी उनका असर होने लगा है। मुनियों को विकथा और गृहिसंसर्ग से सदा बचते रहना चाहिए। ___विभूसा इत्थि संसग्गं' शास्त्र में कहा है कि शरीर आदि की शोभा और स्त्रियों का संसर्ग ब्रह्मचारी के लिये | हलाहल विष के समान है। इसलिये पूर्वाचार्यों ने मर्यादा की है कि सुबह व्याख्यान और तीसरे प्रहर शास्त्र-वाचन या चौपाई के अलावा संतों के यहां स्त्रियों को तथा सतियों के यहां पुरुषों को नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि अधिक संसर्ग से मोह बढ़ता है, जो समय पर दोनों के अहित का कारण हो सकता है। किसी बाई को धार्मिक विषय में कुछ पूछना हो, संत-सतियों के समाचार कहना हो, विदेश का कोई दर्शनार्थी हो या संघ-सम्बन्धी परामर्श करना एवं खास आलोयणा करना हो तो समझदार भाई की साक्षी से संतों के स्थान पर स्त्रियाँ आवश्यकतानुसार बात कर सकती हैं। ऐसा ही सतियों के स्थान पर भाइयों के लिए भी समझें। परन्तु यह संभाषण संघाडे के प्रमुख तथा दीक्षा या ज्ञान से स्थविर संत-सतियों के अलावा सबको नहीं करना चाहिये। बड़ों को कभी अवकाश नहीं हो और किसी को बात सुननी पड़े या किसी को कुछ कहना समझाना पड़े तो बड़ों के सामने या अनुमति से करना चाहिए। सारांश यह है कि धर्मोपदेश और ज्ञान-ध्यान के सिवा अन्य समय में स्त्रियों को खाली बिठाकर बातें करना मोह वृद्धि का कारण है, अत: साधुओं को मर्यादा विरुद्ध स्त्री-संसर्ग और साध्वियों को पुरुष-संसर्ग से सदा बचते रहना चाहिये। खास कर आज के युग में तो इसका अधिक सावधानी से पालन करना जरूरी है।
प्राचीन समय के संत महात्मा उपशम भाव के आदर्श थे। वे क्षमा और निरहंकार भाव का यथोचित रूप से पालन करते थे। वे शास्त्र के आदेशानुसार 'वंदे न से कुप्पे वंदिओ से समुक्कसे' वंदना नहीं करने वाले पर क्रोध नहीं करते और वंदना पाकर अहंकार नहीं करते थे। साधुओं के दशविध धर्म में क्षमा, निर्लोभता, सरलता, मार्दव, | निरभिमान आदि वृत्तियां प्रधान धर्म हैं। समूह में रहने वाले साधु-साध्वियों में क्रोध आदि कषायों की मन्दता नहीं होने से वे स्वपर को अशान्ति के कारण मान बैठते हैं। वर्तमान में दृष्टिगोचर होने वाले कलह, कदाग्रह और गुरुजनों की आज्ञा का तिरस्कार , ये क्रोध-मान के ही परिणाम हैं। क्योंकि अनुपशान्त कषायवाले को गण कैद और साधु-साध्वी शत्रु से दिखाई देते हैं। गण से पृथक् रहने वाले साधु-साध्वी अधिकांश इसी के प्रमाण हैं । त्यागी वर्ग की यह दशा देख कर गृहस्थों की श्रद्धा-भक्ति भी कम हो जाती है। लोग कहने लगते हैं कि संसार की झंझटों को छोड़ कर जब साधु बन गये, तब उनमें झगड़ा कैसा ? झगड़े तो मानापमान के होते हैं। जिन्होंने मान अपमान को छोड़ दिया उनकी अशान्ति कैसी? यह तो वैसी बात है कि ‘एक अंचंभो हो रह्यो, जल में लागी आग।' आजकल अधिकांश देखा जाता है कि विरक्त दशा में शान्त, दान्त और विनय शील दिखने वाले व्यक्ति भी संयम का बाना धारण करके ४-६ महीने में ही रंग बदल देते हैं जबकि पूजनीय संत-मंडली में आकर तो उन्हें अधिक सद्गुणों का विकास करना चाहिये। मुनिवरों को चाहिये कि वे अपने उपशम भाव को अबाधित बनाये रखें, और सबसे मिल