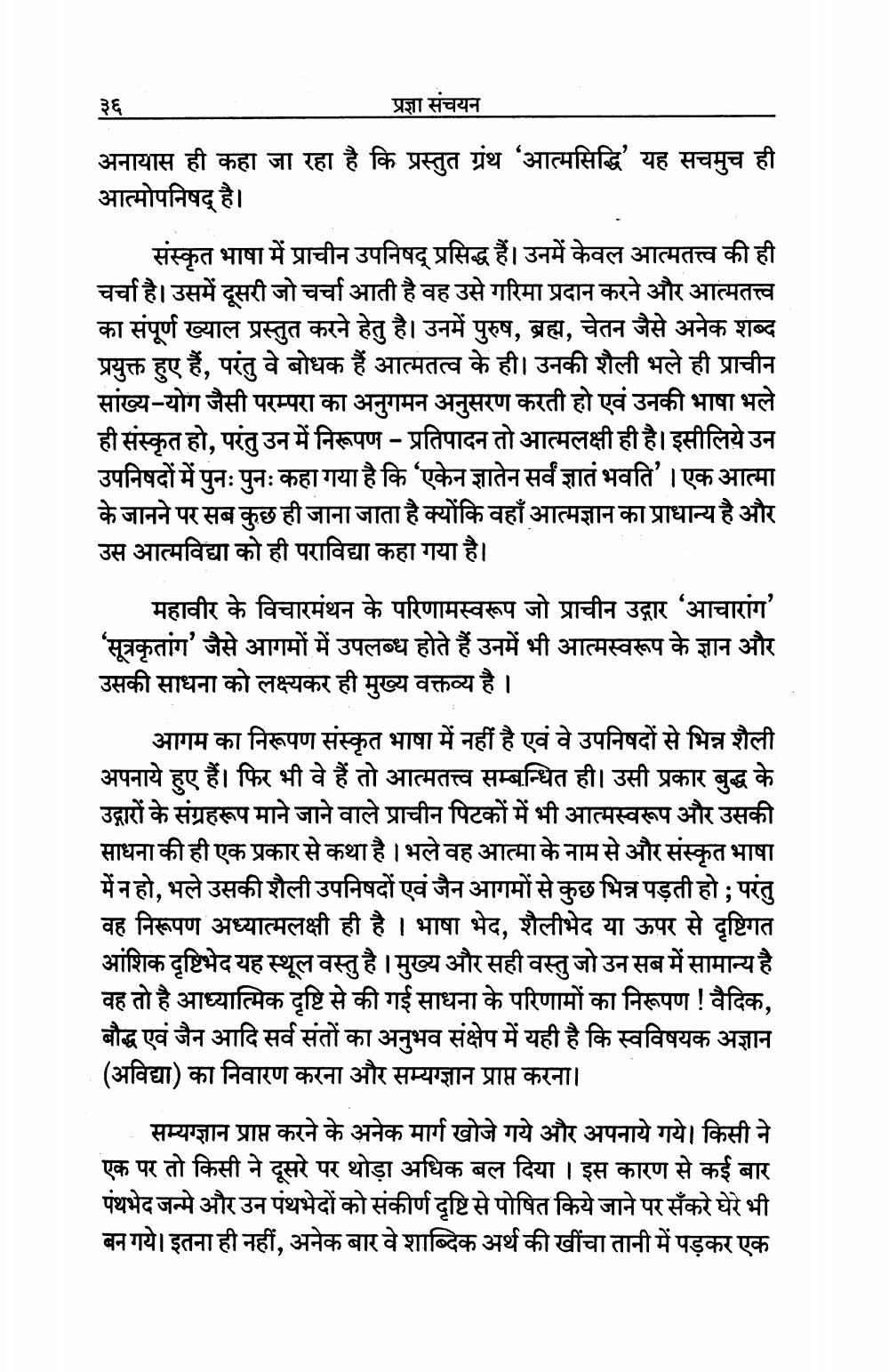________________
३६
प्रज्ञा संचयन
अनायास ही कहा जा रहा है कि प्रस्तुत ग्रंथ ' आत्मसिद्धि' यह सचमुच ही आत्मोपनिषद् है।
संस्कृत भाषा में प्राचीन उपनिषद् प्रसिद्ध हैं। उनमें केवल आत्मतत्त्व की ही चर्चा है। उसमें दूसरी जो चर्चा आती है वह उसे गरिमा प्रदान करने और आत्मतत्त्व का संपूर्ण ख्याल प्रस्तुत करने हेतु है। उनमें पुरुष, ब्रह्म, चेतन जैसे अनेक शब्द प्रयुक्त हुए हैं, परंतु वे बोधक हैं आत्मतत्व के ही । उनकी शैली भले ही प्राचीन सांख्य-योग जैसी परम्परा का अनुगमन अनुसरण करती हो एवं उनकी भाषा भले ही संस्कृत हो, परंतु उन में निरूपण - प्रतिपादन तो आत्मलक्षी ही है। इसीलिये उन उपनिषदों में पुनः पुनः कहा गया है कि 'एकेन ज्ञातेन सर्वं ज्ञातं भवति' । एक आत्मा के जानने पर सब कुछ ही जाना जाता है क्योंकि वहाँ आत्मज्ञान का प्राधान्य है और आत्मविद्या को ही पराविद्या कहा गया है।
महावीर के विचारमंथन के परिणामस्वरूप जो प्राचीन उद्गार 'आचारांग' 'सूत्रकृतांग' जैसे आगमों में उपलब्ध होते हैं उनमें भी आत्मस्वरूप के ज्ञान और उसकी साधना को लक्ष्यकर ही मुख्य वक्तव्य है ।
आगम का निरूपण संस्कृत भाषा में नहीं है एवं वे उपनिषदों से भिन्न शैली अपनाये हुए हैं। फिर भी वे हैं तो आत्मतत्त्व सम्बन्धित ही । उसी प्रकार बुद्ध के उद्गारों के संग्रहरूप माने जाने वाले प्राचीन पिटकों में भी आत्मस्वरूप और उसकी साधना की ही एक प्रकार से कथा है । भले वह आत्मा के नाम से और संस्कृत भाषा हो, भले उसकी शैली उपनिषदों एवं जैन आगमों से कुछ भिन्न पड़ती हो ; परंतु वह निरूपण अध्यात्मलक्षी ही है । भाषा भेद, शैलीभेद या ऊपर से दृष्टिगत आंशिक दृष्टिभेद यह स्थूल वस्तु है। मुख्य और सही वस्तु जो उन सब में सामान्य है वह तो है आध्यात्मिक दृष्टि से की गई साधना के परिणामों का निरूपण ! वैदिक, बौद्ध एवं जैन आदि सर्व संतों का अनुभव संक्षेप में यही है कि स्वविषयक अज्ञान (अविद्या) का निवारण करना और सम्यग्ज्ञान प्राप्त करना ।
सम्यग्ज्ञान प्राप्त करने के अनेक मार्ग खोजे गये और अपनाये गये। किसी ने एक पर तो किसी ने दूसरे पर थोड़ा अधिक बल दिया । इस कारण से कई बार पंथभेद जन्मे और उन पंथभेदों को संकीर्ण दृष्टि से पोषित किये जाने पर सँकरे घेरे भी बन गये। इतना ही नहीं, अनेक बार वे शाब्दिक अर्थ की खींचा तानी में पड़कर एक