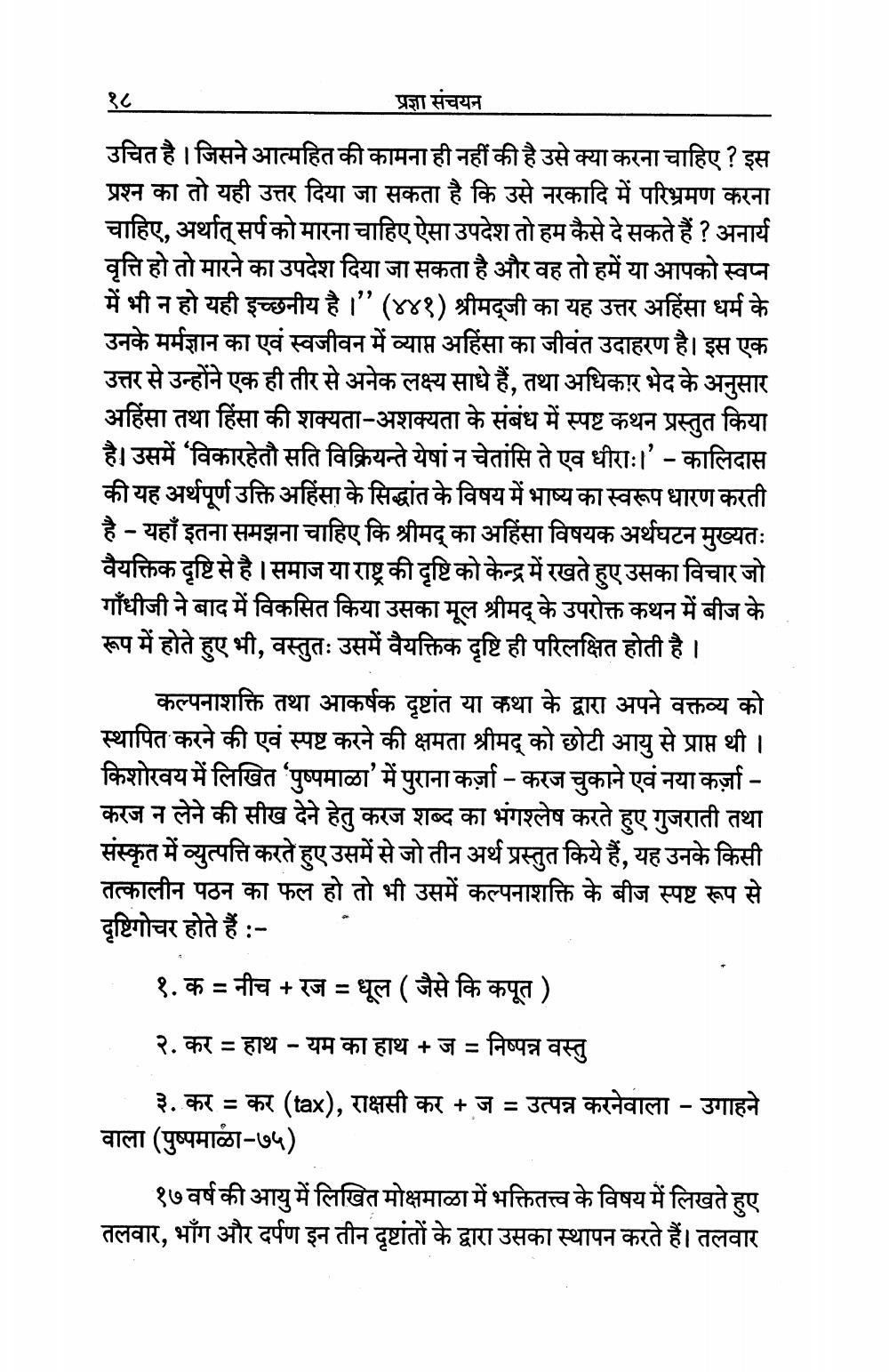________________
प्रज्ञा संचयन उचित है । जिसने आत्महित की कामना ही नहीं की है उसे क्या करना चाहिए ? इस प्रश्न का तो यही उत्तर दिया जा सकता है कि उसे नरकादि में परिभ्रमण करना चाहिए, अर्थात् सर्पको मारना चाहिए ऐसा उपदेश तो हम कैसे दे सकते हैं ? अनार्य वृत्ति हो तो मारने का उपदेश दिया जा सकता है और वह तो हमें या आपको स्वप्न में भी न हो यही इच्छनीय है।" (४४१) श्रीमद्जी का यह उत्तर अहिंसा धर्म के उनके मर्मज्ञान का एवं स्वजीवन में व्याप्त अहिंसा का जीवंत उदाहरण है। इस एक उत्तर से उन्होंने एक ही तीर से अनेक लक्ष्य साधे हैं, तथा अधिकार भेद के अनुसार अहिंसा तथा हिंसा की शक्यता-अशक्यता के संबंध में स्पष्ट कथन प्रस्तुत किया है। उसमें 'विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि ते एव धीराः।' - कालिदास की यह अर्थपूर्ण उक्ति अहिंसा के सिद्धांत के विषय में भाष्य का स्वरूप धारण करती है - यहाँ इतना समझना चाहिए कि श्रीमद् का अहिंसा विषयक अर्थघटन मुख्यतः वैयक्तिक दृष्टि से है। समाज या राष्ट्र की दृष्टि को केन्द्र में रखते हुए उसका विचार जो गाँधीजी ने बाद में विकसित किया उसका मूल श्रीमद् के उपरोक्त कथन में बीज के रूप में होते हुए भी, वस्तुतः उसमें वैयक्तिक दृष्टि ही परिलक्षित होती है ।
कल्पनाशक्ति तथा आकर्षक दृष्टांत या कथा के द्वारा अपने वक्तव्य को स्थापित करने की एवं स्पष्ट करने की क्षमता श्रीमद् को छोटी आयु से प्राप्त थी। किशोरवय में लिखित 'पुष्पमाळा' में पुराना कर्जा - करज चुकाने एवं नया कर्जा - करज न लेने की सीख देने हेतु करज शब्द का भंगश्लेष करते हुए गुजराती तथा संस्कृत में व्युत्पत्ति करते हुए उसमें से जो तीन अर्थ प्रस्तुत किये हैं, यह उनके किसी तत्कालीन पठन का फल हो तो भी उसमें कल्पनाशक्ति के बीज स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं :
१. क = नीच + रज = धूल ( जैसे कि कपूत ) २. कर = हाथ - यम का हाथ + ज = निष्पन्न वस्तु
३. कर = कर (tax), राक्षसी कर + ज = उत्पन्न करनेवाला - उगाहने वाला (पुष्पमाळा-७५)
१७ वर्ष की आयु में लिखित मोक्षमाळा में भक्तितत्त्व के विषय में लिखते हुए तलवार, भाँग और दर्पण इन तीन दृष्टांतों के द्वारा उसका स्थापन करते हैं। तलवार