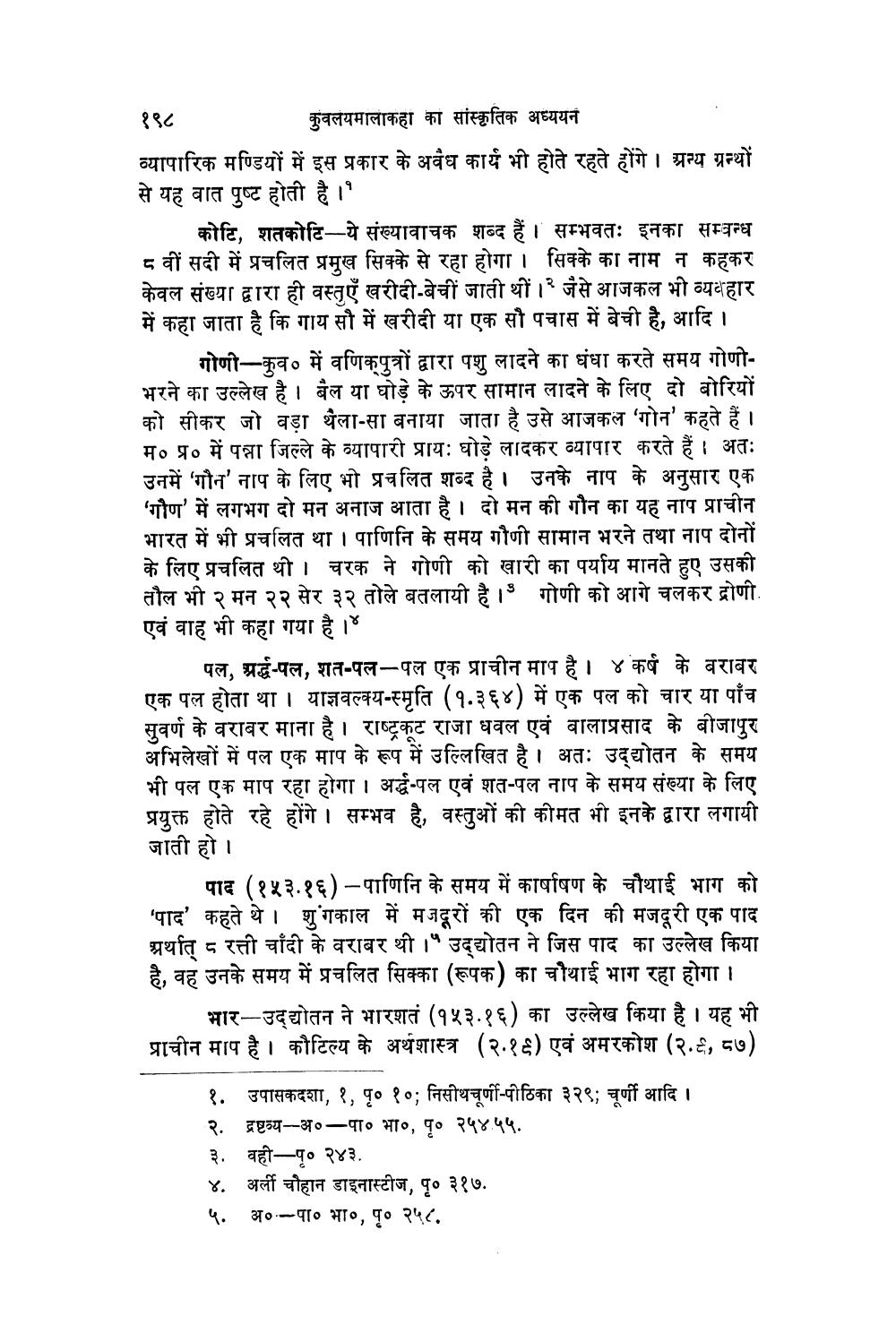________________
१९८
कुवलयमाला कहा का सांस्कृतिक अध्ययन
व्यापारिक मण्डियों में इस प्रकार के अवैध कार्य भी होते रहते होंगे । अन्य ग्रन्थों से यह बात पुष्ट होती है । '
कोटि, शतकोटि- ये संख्यावाचक शब्द हैं । सम्भवतः इनका सम्बन्ध ८वीं सदी में प्रचलित प्रमुख सिक्के से रहा होगा। सिक्के का नाम न कहकर केवल संख्या द्वारा ही वस्तुएँ खरीदी बेचीं जाती थीं । जैसे आजकल भी व्यवहार में कहा जाता है कि गाय सौ में खरीदी या एक सौ पचास में बेची है, आदि ।
गोणी - कुव० में वणिक्पुत्रों द्वारा पशु लादने का धंधा करते समय गोणीभरने का उल्लेख है । बैल या घोड़े के ऊपर सामान लादने के लिए दो बोरियों को सीकर जो बड़ा थैला - सा बनाया जाता है उसे आजकल 'गोन' कहते हैं । म०प्र० में पन्ना जिल्ले के व्यापारी प्रायः घोड़े लादकर व्यापार करते हैं । अतः उनमें 'गौन' नाप के लिए भी प्रचलित शब्द है । उनके नाप के अनुसार एक 'गौण' में लगभग दो मन अनाज आता है । दो मन की गौन का यह नाप प्राचीन भारत में भी प्रचलित था । पाणिनि के समय गौणी सामान भरने तथा नाप दोनों लिए प्रचलित थी । चरक ने गोणी को खारी का पर्याय मानते हुए उसकी तौल भी २ मन २२ सेर ३२ तोले बतलायी है । गोणी को आगे चलकर द्रोणी. एवं वाह भी कहा गया है । ४
पल, अर्द्ध- पल, शत- पल-पल एक प्राचीन माप है । ४ कर्ष के बराबर एक पल होता था । याज्ञवल्क्य स्मृति (१.३६४ ) में एक पल को चार या पाँच सुवर्ण के बराबर माना है । राष्ट्रकूट राजा धवल एवं बालाप्रसाद के बीजापुर अभिलेखों में पल एक माप के रूप में उल्लिखित है । अतः उद्योतन के समय भी पल एक माप रहा होगा । अर्द्ध-पल एवं शत - पल नाप के समय संख्या के लिए प्रयुक्त होते रहे होंगे । सम्भव है, वस्तुओं की कीमत भी इनके द्वारा लगायी जाती हो ।
पाद (१५३.१६ ) - पाणिनि के समय में कार्षाषण के चौथाई भाग को 'पाद' कहते थे । शु ंगकाल में मजदूरों की एक दिन की मजदूरी एक पाद अर्थात् ८ रत्ती चाँदी के बराबर थी । " उद्योतन ने जिस पाद का उल्लेख किया है, वह उनके समय में प्रचलित सिक्का (रूपक) का चौथाई भाग रहा होगा ।
भार- उद्योतन ने भारशतं ( १५३.१६) का उल्लेख किया है । यह भी प्राचीन माप है । कौटिल्य के अर्थशास्त्र ( २.१६) एवं अमरकोश (२.६, ८७ )
१. उपासकदशा, १, पृ० १०; निसीथचूर्णी - पीठिका ३२९; चूर्णी आदि ।
२.
द्रष्टव्य - अ० - पा० भा०, पृ० २५४५५. ३. वही — पृ० २४३.
४. अर्ली चौहान डाइनास्टीज, पृ० ३१७.
५. अ० पा० भा०, पृ० २५८.