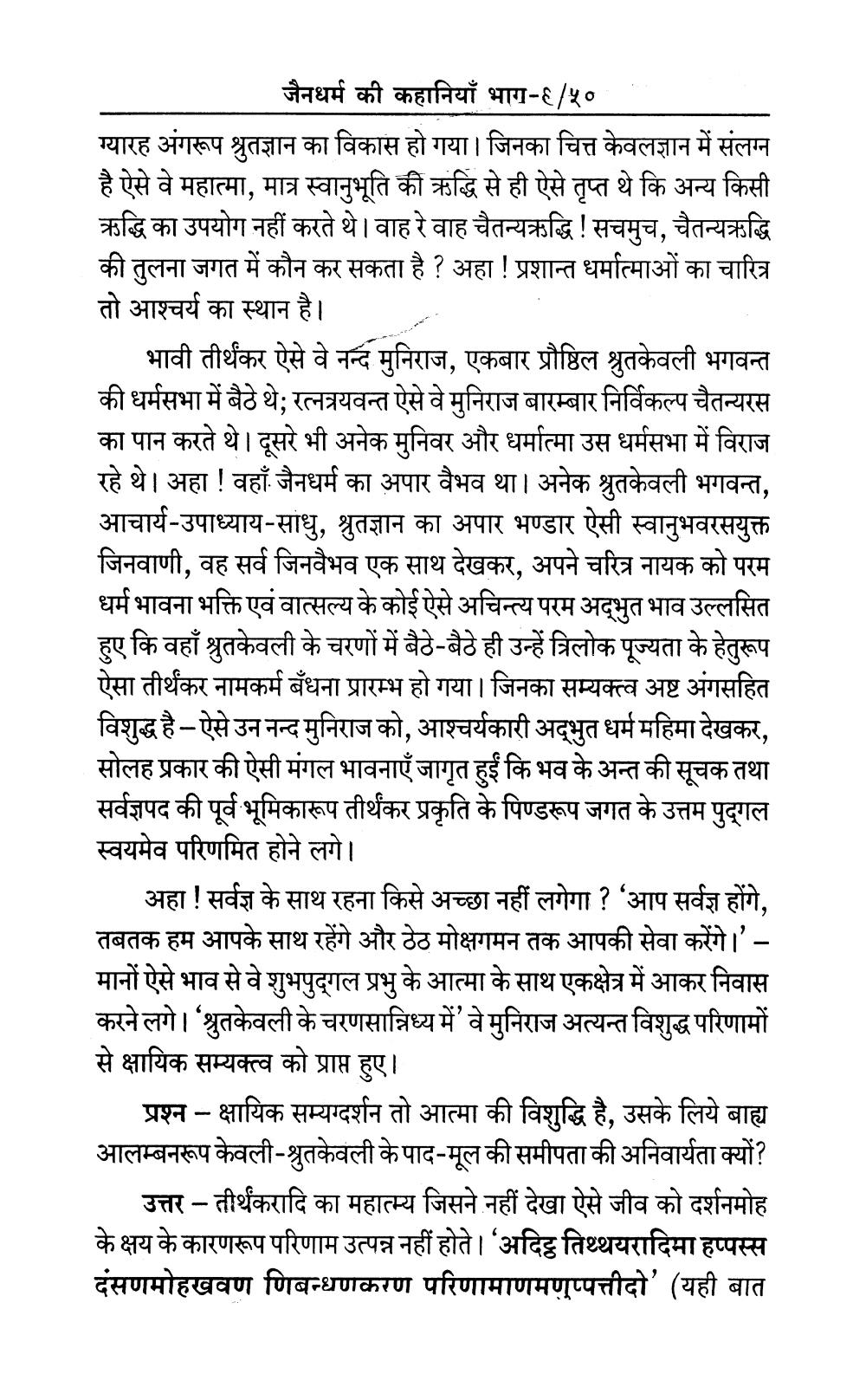________________
जैनधर्म की कहानियाँ भाग - ६/५०
ग्यारह अंगरूप श्रुतज्ञान का विकास हो गया। जिनका चित्त केवलज्ञान में संलग्न ऐसे वे महात्मा, मात्र स्वानुभूति की ऋद्धि से ही ऐसे तृप्त थे कि अन्य किसी ऋद्धि का उपयोग नहीं करते थे । वाह रे वाह चैतन्यऋद्धि ! सचमुच, चैतन्यऋद्धि की तुलना जगत में कौन कर सकता है ? अहा ! प्रशान्त धर्मात्माओं का चारित्र तो आश्चर्य का स्थान है।
भावी तीर्थंकर ऐसे वे नन्द मुनिराज, एकबार प्रौष्ठिल श्रुतकेवली भगवन्त की धर्मसभा में बैठे थे; रत्नत्रयवन्त ऐसे वे मुनिराज बारम्बार निर्विकल्प चैतन्यरस का पान करते थे। दूसरे भी अनेक मुनिवर और धर्मात्मा उस धर्मसभा में विराज रहे थे। अहा ! वहाँ जैनधर्म का अपार वैभव था । अनेक श्रुतकेवली भगवन्त, आचार्य-उपाध्याय-सांधु, श्रुतज्ञान का अपार भण्डार ऐसी स्वानुभवरसयुक्त जिनवाणी, वह सर्व जिनवैभव एक साथ देखकर, अपने चरित्र नायक को परम धर्म भावना भक्ति एवं वात्सल्य के कोई ऐसे अचिन्त्य परम अद्भुत भाव उल्लसित हुए कि वहाँ श्रुतकेवली के चरणों में बैठे-बैठे ही उन्हें त्रिलोक पूज्यता के हेतुरूप ऐसा तीर्थंकर नामकर्म बँधना प्रारम्भ हो गया । जिनका सम्यक्त्व अष्ट अंगसहित विशुद्ध है - ऐसे उन नन्द मुनिराज को, आश्चर्यकारी अद्भुत धर्म महिमा देखकर, सोलह प्रकार की ऐसी मंगल भावनाएँ जागृत हुईं कि भव के अन्त की सूचक तथा सर्वज्ञपद की पूर्व भूमिकारूप तीर्थंकर प्रकृति के पिण्डरूप जगत के उत्तम पुद्गल स्वयमेव परिणमित होने लगे ।
अहा ! सर्वज्ञ के साथ रहना किसे अच्छा नहीं लगेगा ? 'आप सर्वज्ञ होंगे, तबतक हम आपके साथ रहेंगे और ठेठ मोक्षगमन तक आपकी सेवा करेंगे।' मानों ऐसे भाव से वे शुभपुद्गल प्रभु के आत्मा के साथ एकक्षेत्र में आकर निवास करने लगे । 'श्रुतकेवली के चरणसान्निध्य में' वे मुनिराज अत्यन्त विशुद्ध परिणामों से क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त हुए ।
प्रश्न - क्षायिक सम्यग्दर्शन तो आत्मा की विशुद्धि है, उसके लिये बाह्य आलम्बनरूप केवली-श्रुतकेवली के पाद-मूल की समीपता की अनिवार्यता क्यों?
उत्तर - तीर्थंकरादि का महात्म्य जिसने नहीं देखा ऐसे जीव को दर्शनमोह के क्षय के कारणरूप परिणाम उत्पन्न नहीं होते । 'अदिट्ठ तिथ्थयरादिमा हप्पस्स दंसणमोहखवण णिबन्धणकरण परिणामाणमणुप्पत्तीदो' (यही बात