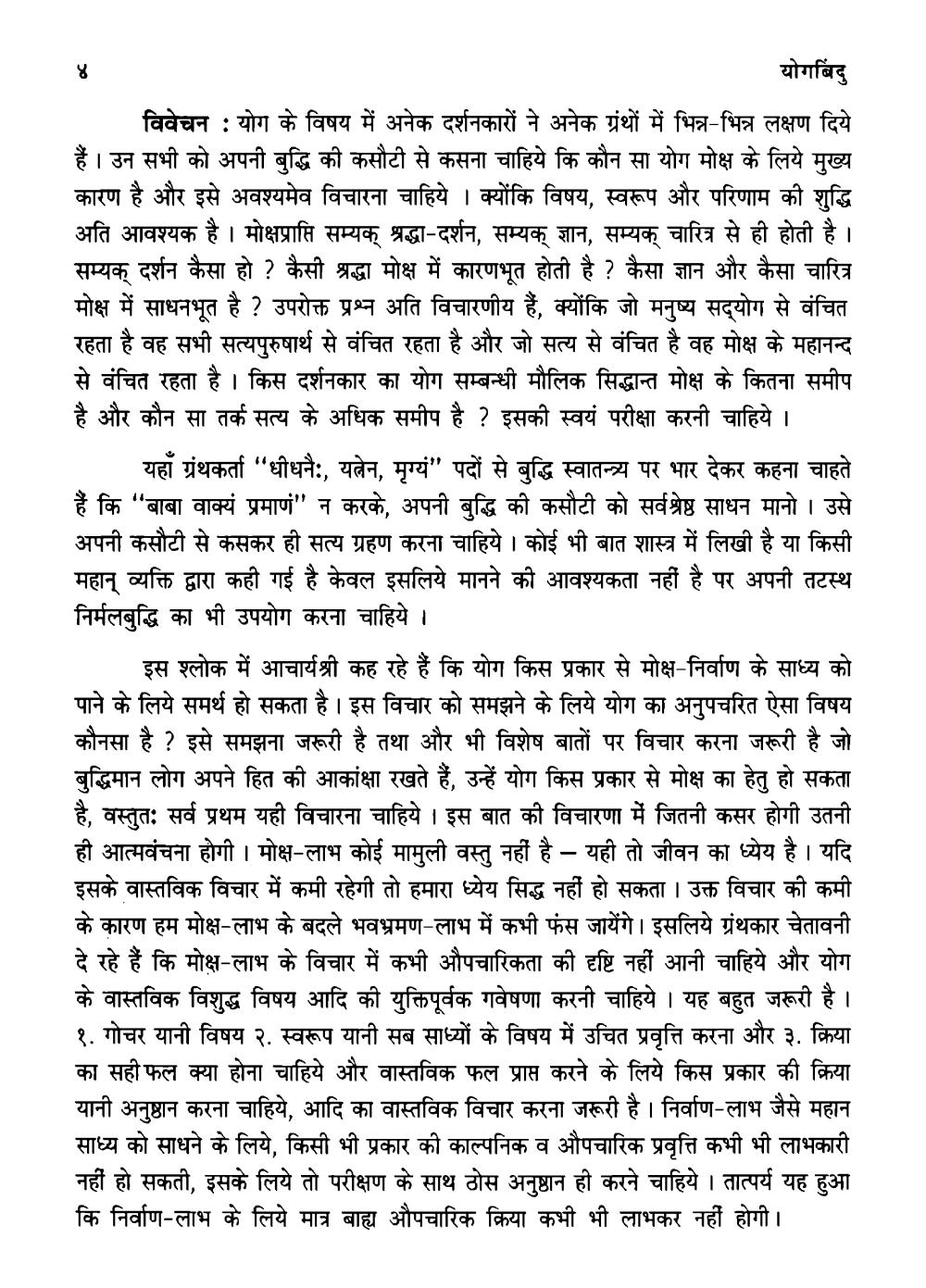________________
योगबिंदु विवेचन : योग के विषय में अनेक दर्शनकारों ने अनेक ग्रंथों में भिन्न-भिन्न लक्षण दिये हैं। उन सभी को अपनी बुद्धि की कसौटी से कसना चाहिये कि कौन सा योग मोक्ष के लिये मुख्य कारण है और इसे अवश्यमेव विचारना चाहिये । क्योंकि विषय, स्वरूप और परिणाम की शुद्धि अति आवश्यक है । मोक्षप्राप्ति सम्यक् श्रद्धा-दर्शन, सम्यक् ज्ञान, सम्यक् चारित्र से ही होती है। सम्यक् दर्शन कैसा हो? कैसी श्रद्धा मोक्ष में कारणभूत होती है ? कैसा ज्ञान और कैसा चारित्र मोक्ष में साधनभूत है ? उपरोक्त प्रश्न अति विचारणीय हैं, क्योंकि जो मनुष्य सद्योग से वंचित रहता है वह सभी सत्यपुरुषार्थ से वंचित रहता है और जो सत्य से वंचित है वह मोक्ष के महानन्द से वंचित रहता है। किस दर्शनकार का योग सम्बन्धी मौलिक सिद्धान्त मोक्ष के कितना समीप है और कौन सा तर्क सत्य के अधिक समीप है ? इसकी स्वयं परीक्षा करनी चाहिये ।
यहाँ ग्रंथकर्ता "धीधनैः, यत्नेन, मुग्यं" पदों से बुद्धि स्वातन्त्र्य पर भार देकर कहना चाहते हैं कि "बाबा वाक्यं प्रमाणं" न करके, अपनी बुद्धि की कसौटी को सर्वश्रेष्ठ साधन मानो । उसे अपनी कसौटी से कसकर ही सत्य ग्रहण करना चाहिये । कोई भी बात शास्त्र में लिखी है या किसी महान् व्यक्ति द्वारा कही गई है केवल इसलिये मानने की आवश्यकता नहीं है पर अपनी तटस्थ निर्मलबुद्धि का भी उपयोग करना चाहिये ।
___ इस श्लोक में आचार्यश्री कह रहे हैं कि योग किस प्रकार से मोक्ष-निर्वाण के साध्य को पाने के लिये समर्थ हो सकता है । इस विचार को समझने के लिये योग का अनुपचरित ऐसा विषय कौनसा है ? इसे समझना जरूरी है तथा और भी विशेष बातों पर विचार करना जरूरी है जो बुद्धिमान लोग अपने हित की आकांक्षा रखते हैं, उन्हें योग किस प्रकार से मोक्ष का हेतु हो सकता है, वस्तुतः सर्व प्रथम यही विचारना चाहिये । इस बात की विचारणा में जितनी कसर होगी उतनी ही आत्मवंचना होगी । मोक्ष-लाभ कोई मामुली वस्तु नहीं है - यही तो जीवन का ध्येय है । यदि इसके वास्तविक विचार में कमी रहेगी तो हमारा ध्येय सिद्ध नहीं हो सकता । उक्त विचार की कमी के कारण हम मोक्ष-लाभ के बदले भवभ्रमण-लाभ में कभी फंस जायेंगे। इसलिये ग्रंथकार चेतावनी दे रहे हैं कि मोक्ष-लाभ के विचार में कभी औपचारिकता की दृष्टि नहीं आनी चाहिये और योग के वास्तविक विशुद्ध विषय आदि की युक्तिपूर्वक गवेषणा करनी चाहिये । यह बहुत जरूरी है। १. गोचर यानी विषय २. स्वरूप यानी सब साध्यों के विषय में उचित प्रवृत्ति करना और ३. क्रिया का सही फल क्या होना चाहिये और वास्तविक फल प्राप्त करने के लिये किस प्रकार की क्रिया यानी अनुष्ठान करना चाहिये, आदि का वास्तविक विचार करना जरूरी है। निर्वाण-लाभ जैसे महान साध्य को साधने के लिये, किसी भी प्रकार की काल्पनिक व औपचारिक प्रवृत्ति कभी भी लाभकारी नहीं हो सकती, इसके लिये तो परीक्षण के साथ ठोस अनुष्ठान ही करने चाहिये । तात्पर्य यह हुआ कि निर्वाण-लाभ के लिये मात्र बाह्य औपचारिक क्रिया कभी भी लाभकर नहीं होगी।