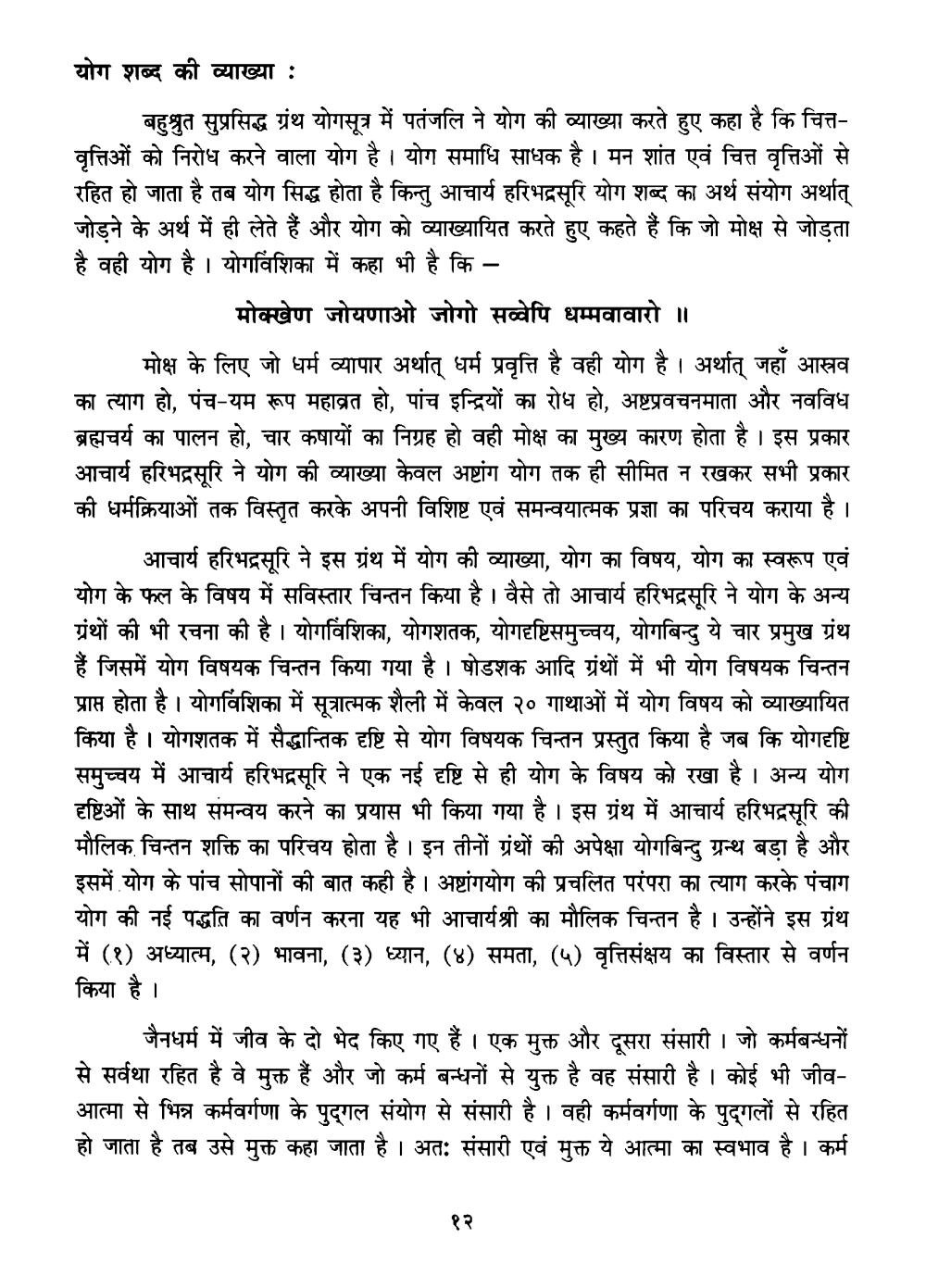________________
योग शब्द की व्याख्या :
बहुश्रुत सुप्रसिद्ध ग्रंथ योगसूत्र में पतंजलि ने योग की व्याख्या करते हुए कहा है कि चित्तवृत्तिओं को निरोध करने वाला योग है । योग समाधि साधक है । मन शांत एवं चित्त वृत्तिओं से रहित हो जाता है तब योग सिद्ध होता है किन्तु आचार्य हरिभद्रसूरि योग शब्द का अर्थ संयोग अर्थात् जोड़ने के अर्थ में ही लेते हैं और योग को व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि जो मोक्ष से जोड़ता है वही योग है। योगविंशिका में कहा भी है कि -
मोक्खेण जोयणाओ जोगो सव्वेपि धम्मवावारो ॥ मोक्ष के लिए जो धर्म व्यापार अर्थात् धर्म प्रवृत्ति है वही योग है। अर्थात् जहाँ आस्रव का त्याग हो, पंच-यम रूप महाव्रत हो, पांच इन्द्रियों का रोध हो, अष्टप्रवचनमाता और नवविध ब्रह्मचर्य का पालन हो, चार कषायों का निग्रह हो वही मोक्ष का मुख्य कारण होता है । इस प्रकार आचार्य हरिभद्रसूरि ने योग की व्याख्या केवल अष्टांग योग तक ही सीमित न रखकर सभी प्रकार की धर्मक्रियाओं तक विस्तृत करके अपनी विशिष्ट एवं समन्वयात्मक प्रज्ञा का परिचय कराया है।
आचार्य हरिभद्रसूरि ने इस ग्रंथ में योग की व्याख्या, योग का विषय, योग का स्वरूप एवं योग के फल के विषय में सविस्तार चिन्तन किया है। वैसे तो आचार्य हरिभद्रसूरि ने योग के अन्य ग्रंथों की भी रचना की है। योगविंशिका, योगशतक, योगदृष्टिसमुच्चय, योगबिन्दु ये चार प्रमुख ग्रंथ हैं जिसमें योग विषयक चिन्तन किया गया है । षोडशक आदि ग्रंथों में भी योग विषयक चिन्तन प्राप्त होता है। योगविशिका में सूत्रात्मक शैली में केवल २० गाथाओं में योग विषय को व्याख्यायित किया है। योगशतक में सैद्धान्तिक दृष्टि से योग विषयक चिन्तन प्रस्तुत किया है जब कि योगदृष्टि समुच्चय में आचार्य हरिभद्रसूरि ने एक नई दृष्टि से ही योग के विषय को रखा है। अन्य योग दृष्टिओं के साथ समन्वय करने का प्रयास भी किया गया है । इस ग्रंथ में आचार्य हरिभद्रसूरि की मौलिक चिन्तन शक्ति का परिचय होता है। इन तीनों ग्रंथों की अपेक्षा योगबिन्दु ग्रन्थ बड़ा है और इसमें योग के पांच सोपानों की बात कही है। अष्टांगयोग की प्रचलित परंपरा का त्याग करके पंचाग योग की नई पद्धति का वर्णन करना यह भी आचार्यश्री का मौलिक चिन्तन है । उन्होंने इस ग्रंथ में (१) अध्यात्म, (२) भावना, (३) ध्यान, (४) समता, (५) वृत्तिसंक्षय का विस्तार से वर्णन किया है।
जैनधर्म में जीव के दो भेद किए गए हैं । एक मुक्त और दूसरा संसारी । जो कर्मबन्धनों से सर्वथा रहित है वे मुक्त हैं और जो कर्म बन्धनों से युक्त है वह संसारी है । कोई भी जीवआत्मा से भिन्न कर्मवर्गणा के पुद्गल संयोग से संसारी है। वही कर्मवर्गणा के पुद्गलों से रहित हो जाता है तब उसे मुक्त कहा जाता है । अतः संसारी एवं मुक्त ये आत्मा का स्वभाव है । कर्म