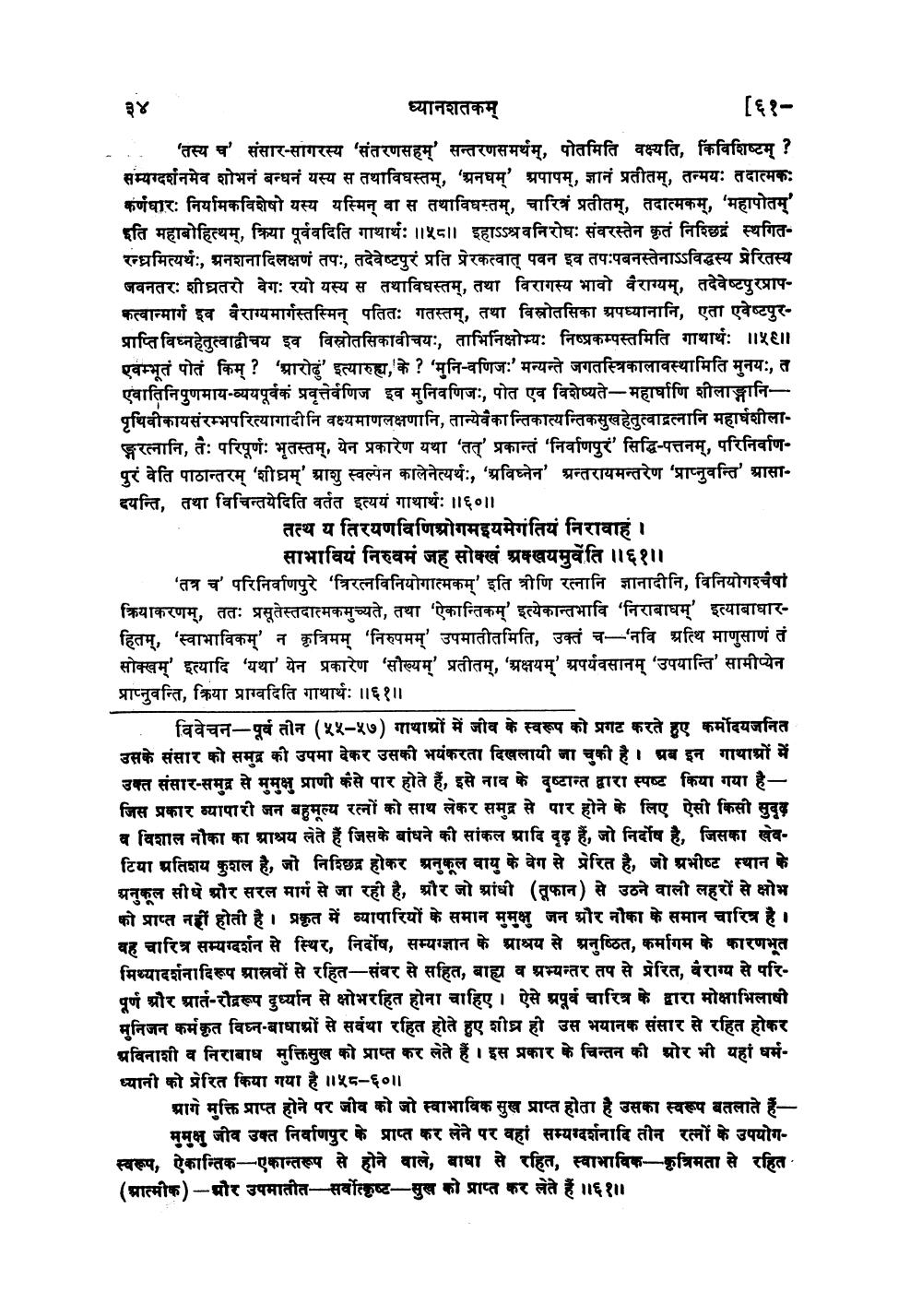________________
[६१
'तस्य च ' संसार - सागरस्य 'संतरणसहम्' सन्तरणसमर्थम्, पोतमिति वक्ष्यति, किंविशिष्टम् ? सम्यग्दर्शनमेव शोभनं बन्धनं यस्य स तथाविधस्तम्, 'अनघम्' अपापम्, ज्ञानं प्रतीतम्, तन्मयः तदात्मकः कर्णधारः निर्यामकविशेषो यस्य यस्मिन् वा स तथाविधस्तम्, चारित्रं प्रतीतम्, तदात्मकम्, 'महापोतम्’ इति महाबोहित्थम्, क्रिया पूर्ववदिति गाथार्थः ॥ ५८ ॥ इहाऽऽश्रवनिरोधः संवरस्तेन कृतं निश्छिद्रं स्थगित - रन्ध्रमित्यर्थः, अनशनादिलक्षणं तपः, तदेवेष्टपुरं प्रति प्रेरकत्वात् पवन इव तपः पबनस्तेनाऽऽविद्धस्य प्रेरितस्य जवनतरः शीघ्रतरो वेगः रयो यस्य स तथाविधस्तम्, तथा विरागस्य भावो वैराग्यम्, तदेवेष्टपुरप्रापकत्वान्मार्ग इव वैराग्यमार्गस्तस्मिन् पतितः गतस्तम्, तथा विस्रोतसिका श्रपध्यानानि, एता एवेष्टपुरप्राप्ति विघ्नहेतुत्वाद्वीचय इव विस्रोतसिकावीचयः, ताभिर्नक्षोभ्यः निष्प्रकम्पस्तमिति गाथार्थः ॥ ५६ ॥ एवम्भूतं पोतं किम् ? 'श्रारोढुं' इत्यारुह्य के ? 'मुनि वणिजः' मन्यन्ते जगतस्त्रिकालावस्थामिति मुनयः, त एवातिनिपुणमाय - व्ययपूर्वकं प्रवृत्तेर्वणिज इव मुनिवणिजः, पोत एव विशेष्यते - महार्षाणि शीलाङ्गानि - पृथिवीकाय संरम्भपरित्यागादीनि वक्ष्यमाणलक्षणानि, तान्येवैका न्तिकात्यन्तिकसुखहेतुत्वाद्रत्नानि महार्षशीलाङ्गरत्नानि तैः परिपूर्णः भृतस्तम्, येन प्रकारेण यथा 'तत्' प्रकान्तं 'निर्वाणपुरं' सिद्धि-पत्तनम्, परिनिर्वाणपुरं वेति पाठान्तरम् ' शीघ्रम्' आशु स्वल्पेन कालेनेत्यर्थः, 'अविघ्नेन' अन्तरायमन्तरेण 'प्राप्नुवन्ति श्रासादयन्ति तथा विचिन्तयेदिति वर्तत इत्ययं गाथार्थः ॥ ६० ॥
तत्थ य तिरयणविणिश्रोगमइयमेगंतियं निरावाहं । साभावियं निरुवमं जह सोक्खं श्रक्खयमुर्वेति ॥ ६१ ॥
'तत्र च' परिनिर्वाणपुरे 'त्रिरत्नविनियोगात्मकम्' इति त्रीणि रत्नानि ज्ञानादीनि विनियोगश्चैषां क्रियाकरणम्, ततः प्रसूतेस्तदात्मकमुच्यते, तथा 'ऐकान्तिकम्' इत्येकान्तभावि 'निराबाधम्' इत्याबाधारहितम् 'स्वाभाविकम्' न कृत्रिमम् 'निरुपमम्' उपमातीतमिति, उक्तं च- 'नवि श्रत्थि माणुसाणं तं सोक्खम्' इत्यादि 'यथा' येन प्रकारेण 'सौख्यम्' प्रतीतम्, 'अक्षयम्' श्रपर्यवसानम् 'उपयान्ति' सामीप्येन प्राप्नुवन्ति, क्रिया प्राग्वदिति गाथार्थः ।। ६१ ।।
३४
ध्यानशतकम्
वेग से प्रेरित है, जो अभीष्ट स्थान के तूफान ) से उठने वाली लहरों से क्षोभ
(
विवेचन - पूर्व तीन (५५ - ५७ ) गाथानों में जीव के स्वरूप को प्रगट करते हुए कर्मोदयजनित उसके संसार को समुद्र की उपमा देकर उसकी भयंकरता दिखलायी जा चुकी है। अब इन गाथानों में उक्त संसार-समुद्र से मुमुक्षु प्राणी कैसे पार होते हैं, इसे नाव के दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया गया हैजिस प्रकार व्यापारी जन बहुमूल्य रत्नों को साथ लेकर समुद्र से पार होने के लिए ऐसी किसी सुदृढ़ व विशाल नौका का श्राश्रय लेते हैं जिसके बांधने की सांकल आदि दृढ़ हैं, जो निर्दोष है, जिसका खेवटिया प्रतिशय कुशल है, जो निश्छिद्र होकर अनुकूल वायु के अनुकूल सीधे और सरल मार्ग से जा रही है, और जो श्रांधी को प्राप्त नहीं होती है । प्रकृत में व्यापारियों के समान मुमुक्षु जन और नौका के समान चारित्र है । वह चारित्र सम्यग्दर्शन से स्थिर, निर्दोष, सम्यग्ज्ञान के श्राश्रय से अनुष्ठित, कर्मागम के कारणभूत मिथ्यादर्शनादिरूप प्रात्रवों से रहित - संवर से सहित, बाह्य व अभ्यन्तर तप से प्रेरित, वैराग्य से परिपूर्ण और प्रातं रौद्ररूप दुर्ध्यान से क्षोभरहित होना चाहिए। ऐसे अपूर्व चारित्र के द्वारा मोक्षाभिलाषी मुनिजन कर्मकृत विघ्न-बाधानों से सर्वथा रहित होते हुए शीघ्र ही उस भयानक संसार से रहित होकर अविनाशी व निराबाध मुक्तिसुख को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के चिन्तन की ओर भी यहां धर्मध्यानी को प्रेरित किया गया है ।।५८-६०।।
श्रागे मुक्ति प्राप्त होने पर जीव को जो स्वाभाविक सुख प्राप्त होता है उसका स्वरूप बतलाते हैं— मुमुक्षु जीव उक्त निर्वाणपुर के प्राप्त कर लेने पर वहां सम्यग्दर्शनादि तीन रत्नों के उपयोगस्वरूप, ऐकान्तिक – एकान्तरूप से होने वाले, बाधा से रहित, स्वाभाविक — कृत्रिमता से रहित ( श्रात्मीक ) - और उपमातीत — सर्वोत्कृष्ट — सुख को प्राप्त कर लेते हैं ॥ ६१॥