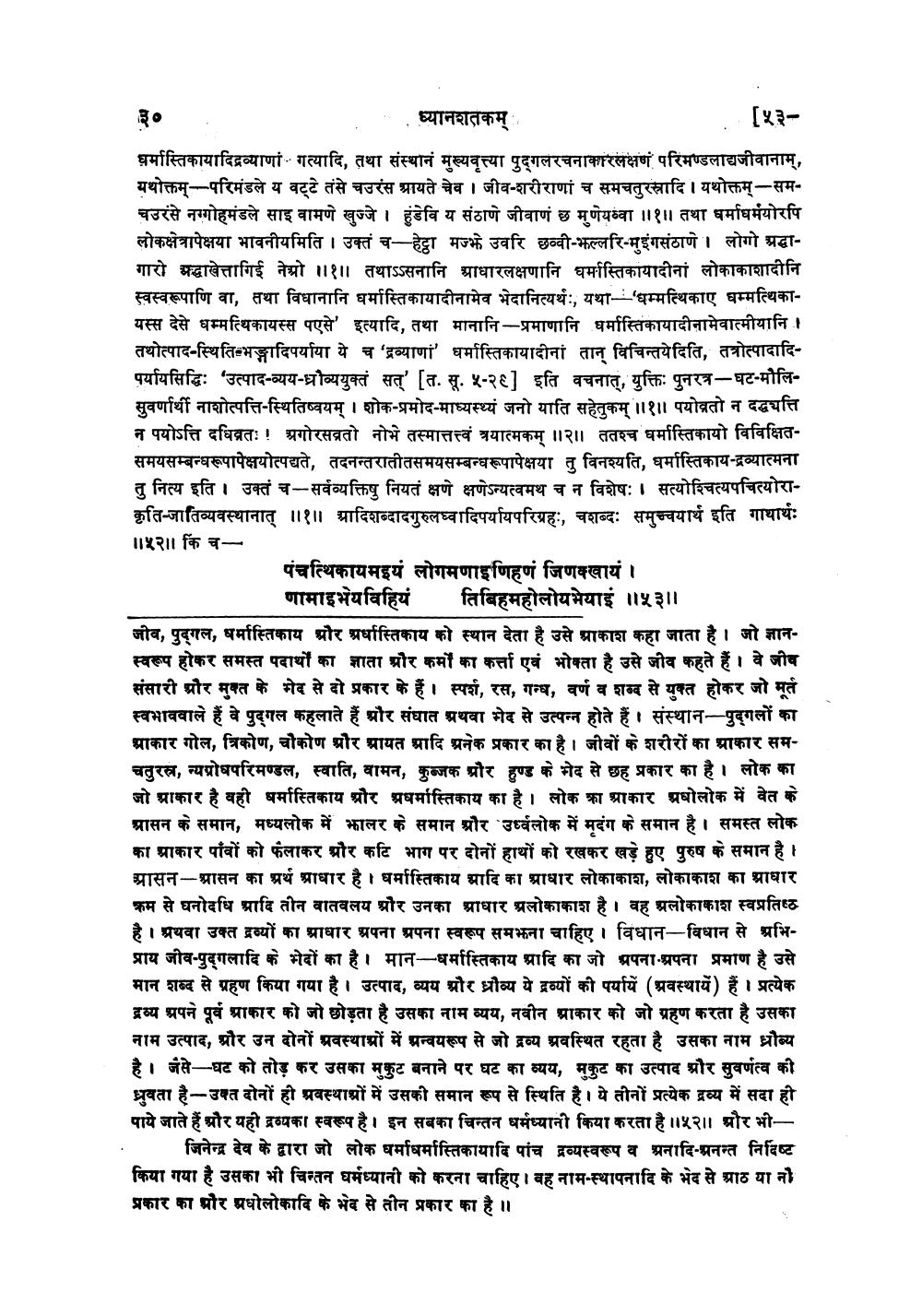________________
ध्यानशतकम्
. [५३
धर्मास्तिकायादिद्रव्याणां गत्यादि, तथा संस्थानं मुख्यवृत्त्या पुद्गलरचनाकारलक्षणं परिमण्डलाद्यजीवानाम्, यथोक्तम्-परिमंडले य वट्टे तंसे चउरंस प्रायते चेव । जीव-शरीराणां च समचतुरस्रादि । यथोक्तम्-समचउरंसे नग्गोहमंडले साइ वामणे खुज्जे। हुंडेवि य संठाणे जीवाणं छ मुणेयम्वा ॥१॥ तथा धर्माधर्मयोरपि लोकक्षेत्रापेक्षया भावनीयमिति । उक्तं च-हेद्रा मज्झे उवरि छन्वी-मल्लरि-मइंगसंठाणे। लोगो अद्धा गारो अद्धाखेत्तागिई नेग्रो ॥१॥ तथाऽऽसनानि आधारलक्षणानि धर्मास्तिकायादीनां लोकाकाशादीनि स्वस्वरूपाणि वा, तथा विधानानि धर्मास्तिकायादीनामेव भेदानित्यर्थः, यथा-'धम्मत्थिकाए धम्मत्थिकायस्स देसे धम्मत्थिकायस्स पएसे' इत्यादि, तथा मानानि-प्रमाणानि धर्मास्तिकायादीनामेवात्मीयानि । तथोत्पाद-स्थितिभङ्गादिपर्याया ये च 'द्रव्याणां' धर्मास्तिकायादीनां तान विचिन्तयेदिति, तत्रोत्पादादिपर्यायसिद्धिः 'उत्पाद-व्यय-ध्रौव्ययुक्तं सत्' [त. सू. ५-२६] इति वचनात, युक्तिः पुनरत्र-घट-मौलिसुवर्णार्थी नाशोत्पत्ति-स्थितिष्वयम् । शोक-प्रमोद-माध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम् ॥१॥ पयोव्रतो न दद्धयत्ति न पयोऽत्ति दधिव्रतः। अगोरसवतो नोभे तस्मात्तत्त्वं त्रयात्मकम् ॥२॥ ततश्च धर्मास्तिकायो विविक्षितसमयसम्बन्धरूपापेक्षयोत्पद्यते, तदनन्तरातीतसमयसम्बन्धरूपापेक्षया तु विनश्यति, धर्मास्तिकाय-द्रव्यात्मना तु नित्य इति । उक्तं च-सर्वव्यक्तिषु नियतं क्षणे क्षणेऽन्यत्वमथ च न विशेषः । सत्योश्चित्यपचित्योराकृति-जातिव्यवस्थानात् ॥१॥ आदिशब्दादगुरुलघ्वादिपर्यायपरिग्रहः, चशब्दः समुच्चयार्थ इति गाथार्थः ॥५२॥ किं च
पंचत्थिकायमइयं लोगमणाइणिहणं जिणक्खायं ।
णामाइभेयविहियं तिबिहमहोलोयभेयाइं ॥५३॥ जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय और अर्धास्तिकाय को स्थान देता है उसे आकाश कहा जाता है। जो ज्ञानस्वरूप होकर समस्त पदार्थों का ज्ञाता और कर्मों का कर्ता एवं भोक्ता है उसे जीव कहते हैं। वे जीव संसारी और मुक्त के भेद से दो प्रकार के हैं। स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण व शब्द से युक्त होकर जो मूर्त स्वभाववाले हैं वे पुद्गल कहलाते हैं और संघात अथवा भेद से उत्पन्न होते हैं। संस्थान-पुद्गलों का प्राकार गोल, त्रिकोण, चौकोण और प्रायत आदि अनेक प्रकार का है। जीवों के शरीरों का प्राकार समचतुरस्त्र, न्यग्रोधपरिमण्डल, स्वाति, वामन, कुब्जक और हण्ड के भेद से छह प्रकार का है। लोक का जो प्राकार है वही धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का है। लोक का आकार अधोलोक में वेत के प्रासन के समान, मध्यलोक में झालर के समान और उर्ध्वलोक में मृदंग के समान है। समस्त लोक का प्राकार पांवों को फैलाकर और कटि भाग पर दोनों हाथों को रखकर खड़े हुए पुरुष के समान है। आसन-पासन का अर्थ प्राधार है। धर्मास्तिकाय आदि का प्राधार लोकाकाश, लोकाकाश का प्राधार क्रम से घनोदधि आदि तीन वातवलय और उनका प्राधार अलोकाकाश है। वह प्रलोकाकाश स्वप्रतिष्ठ है। अथवा उक्त द्रव्यों का प्राधार अपना अपना स्वरूप समझना चाहिए। विधान-विधान से अभिप्राय जीव-पुद्गलादि के भेदों का है। मान-धर्मास्तिकाय प्रादि का जो अपना-अपना प्रमाण है उसे मान शब्द से ग्रहण किया गया है। उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य ये द्रव्यों की पर्याय (अवस्थायें) हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने पूर्व प्राकार को जो छोड़ता है उसका नाम व्यय, नवीन प्रकार को जो ग्रहण करता है उसका नाम उत्पाद, और उन दोनों प्रवस्थानों में अन्वयरूप से जो द्रव्य अवस्थित रहता है उसका नाम ध्रौव्य है। जैसे-घट को तोड़ कर उसका मुकुट बनाने पर घट का व्यय, मुकुट का उत्पाद और सुवर्णत्व की ध्रुवता है-उक्त दोनों ही अवस्थानों में उसकी समान रूप से स्थिति है। ये तीनों प्रत्येक द्रव्य में सदा ही पाये जाते हैं और यही द्रव्यका स्वरूप है। इन सबका चिन्तन धर्मध्यानी किया करता है ॥५२॥ और भी. जिनेन्द्र देव के द्वारा जो लोक धर्माधर्मास्तिकायादि पांच द्रव्यस्वरूप व अनादि-अनन्त निर्दिष्ट किया गया है उसका भी चिन्तन धर्मध्यानी को करना चाहिए। वह नाम-स्थापनादि के भेद से पाठ या नौ प्रकार का प्रोर प्रधोलोकादि के भेद से तीन प्रकार का है।