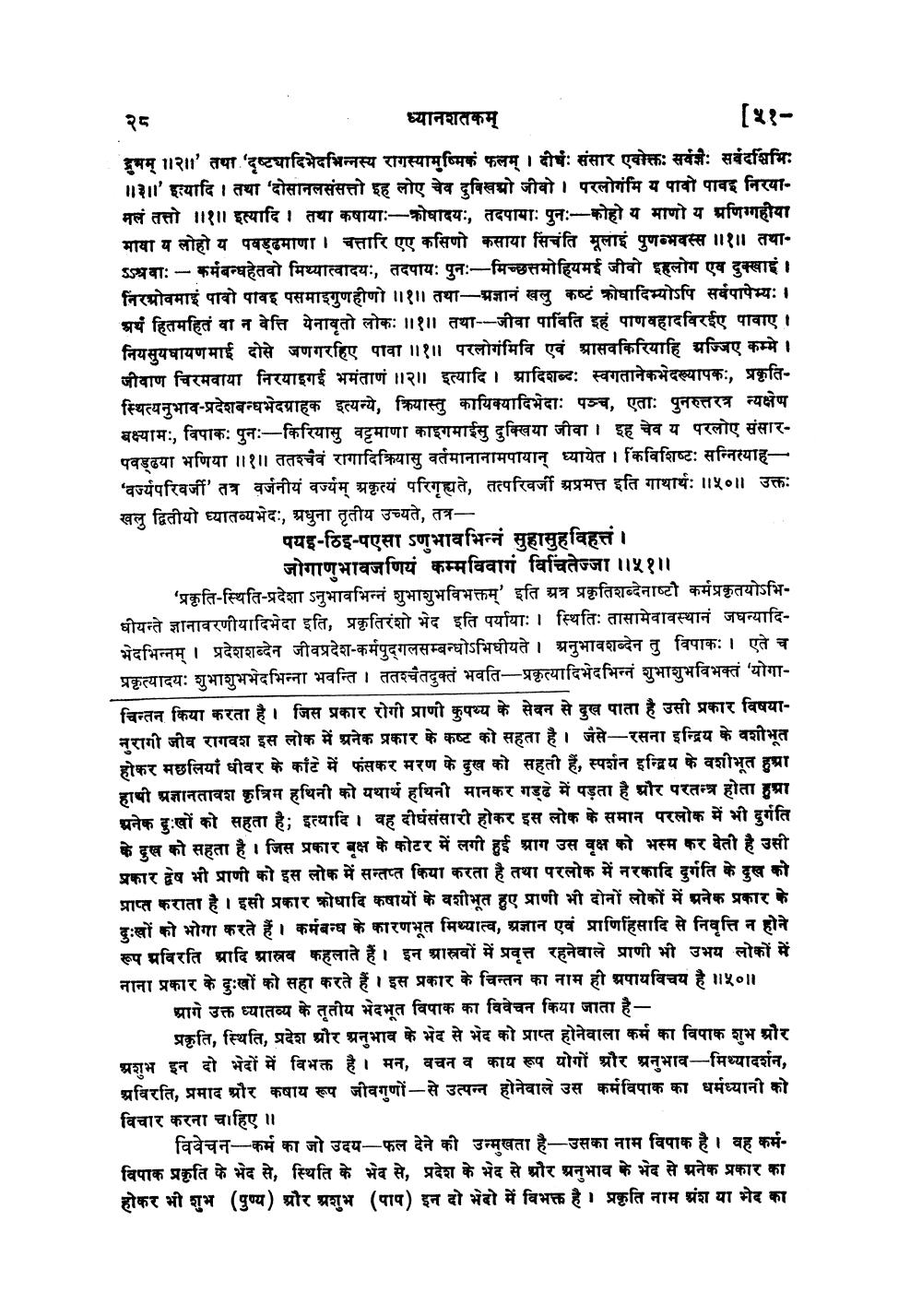________________
२८
ध्यानशतकम्
[ ५१
द्रुमम् ||२||' तथा 'दृष्ट्यादिभेदभिन्नस्य रागस्यामुष्मिकं फलम् । दीर्घः संसार एवोक्तः सर्वशेः सर्वदर्शिभिः ||३||' इत्यादि । तथा 'दोसानलसंसत्तो इह लोए चेव दुविखो जीवो। परलोगंमि य पावो पावइ निरयामलं तत्तो ॥ १॥ इत्यादि । तथा कषायाः क्रोधादयः, तदपायाः पुनः - कोहो य माणो य प्रणिग्गहीया माया य लोहो य पवड्ढमाणा । चत्तारि एए कसिणो कसाया सिंचंति मूलाई पुणन्भवस्स ॥१॥ तथाश्रवाः - कर्मबन्धहेतवो मिथ्यात्वादयः, तदपायः पुनः - मिच्छत्समो हियमई जीवो इहलोग एव दुखाइं । निरोवमाई पावो पावइ पसमाइगुणहीणो ॥ १ ॥ तथा — प्रज्ञानं खलु कष्टं क्रोधादिभ्योऽपि सर्वपापेभ्यः । अयं हितमहितं वा न वेत्ति येनावृतो लोकः ॥ १॥ तथा-- जीवा पाविति इहं पाणबहादविरईए पावाए । नियसुयधायण माई दोसे जणगरहिए पावा || १॥ परलोगंमिवि एवं प्रासवकिरियाहि प्रज्जिए कम्मे । जीवाण चिरमवाया निरयाइगई भमंताणं ||२|| इत्यादि । श्रादिशब्दः स्वगतानेकभेदख्यापकः, प्रकृतिस्थित्यनुभाव- प्रदेशबन्ध भेदग्राहक इत्यन्ये, क्रियास्तु कायिक्यादिभेदाः पञ्च एताः पुनरुत्तरत्र न्यक्षेण वक्ष्यामः, विपाकः पुनः किरियासु वट्टमाणा काइगमाईसु दुक्खिया जीवा । इह चैव य परलोए संसारपवड्ढया भणिया ।।१।। ततश्चैवं रागादिक्रियासु वर्तमानानामपायान् ध्यायेत । किविशिष्टः सन्निस्याह'वर्ण्य परिवर्जी' तत्र वर्जनीयं वर्ज्यम् प्रकृत्यं परिगृह्यते, तत्परिवर्जी अप्रमत्त इति गाथार्थः ॥ ५० ॥ उक्तः खलु द्वितीय ध्यातव्यभेदः, अधुना तृतीय उच्यते, तत्र -
-इ-पसाऽणुभावभिन्नं सुहासुहविहत्तं । जोगाणुभावजयं कम्मविवागं विचितेज्जा ॥ ५१ ॥
1
'प्रकृति-स्थिति- प्रदेशानुभावभिन्नं शुभाशुभविभक्तम्' इति प्रत्र प्रकृतिशब्देनाष्टौ कर्मप्रकृतयोऽभिधीयन्ते ज्ञानावरणीयादिभेदा इति, प्रकृतिरंशो भेद इति पर्यायाः । स्थितिः तासामेवावस्थानं जघन्यादिभेदभिन्नम् । प्रदेशशब्देन जीवप्रदेश- कर्मपुद्गलसम्बन्धोऽभिधीयते । अनुभावशब्देन तु विपाकः । एते च प्रकृत्यादयः शुभाशुभभेदभिन्ना भवन्ति । ततश्चैतदुक्तं भवति – प्रकृत्यादिभेदभिन्नं शुभाशुभविभक्तं ' योगाचिन्तन किया करता है। जिस प्रकार रोगी प्राणी कुपथ्य के सेवन से दुख पाता है उसी प्रकार विषयानुरागी जीव रागवश इस लोक में अनेक प्रकार के कष्ट को सहता है। जैसे— रसना इन्द्रिय के वशीभूत होकर मछलियाँ धीवर के कांटे में फंसकर मरण के दुख को सहती हैं, स्पर्शन इन्द्रिय के वशीभूत हुना हाथी अज्ञानतावश कृत्रिम हथिनी को यथार्थ हथिनी मानकर गड्ढे में पड़ता है और परतन्त्र होता हुश्रा अनेक दुःखों को सहता है; इत्यादि । वह दीर्घसंसारी होकर इस लोक के समान परलोक में भी दुर्गति के दुख को सहता । जिस प्रकार बृक्ष के कोटर में लगी हुई श्राग उस वृक्ष को भस्म कर देती है उसी प्रकार द्वेष भी प्राणी को इस लोक में सन्तप्त किया करता है तथा परलोक में नरकादि दुर्गति के को दुख प्राप्त कराता है । इसी प्रकार क्रोधादि कषायों के वशीभूत हुए प्राणी भी दोनों लोकों में अनेक प्रकार के दुःखों को भोगा करते हैं । कर्मबन्ध के कारणभूत मिथ्यात्व, प्रज्ञान एवं प्राणिहिंसादि से निवृत्ति न होने रूप प्रविरति श्रादि श्रास्रव कहलाते हैं। इन श्रास्रवों में प्रवृत्त रहनेवाले प्राणी भी उभय लोकों में नाना प्रकार के दुःखों को सहा करते हैं। इस प्रकार के चिन्तन का नाम ही अपायविचय है ॥५०॥
आगे उक्त ध्यातव्य के तृतीय भेदभूत विपाक का विवेचन किया जाता है
प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाव के भेद से भेद को प्राप्त होनेवाला कर्म का विपाक शुभ और अशुभ इन दो भेदों में विभक्त है। मन, वचन व काय रूप योगों और अनुभाव - मिथ्यादर्शन, श्रविरति, प्रमाद और कषाय रूप जीवगुणों से उत्पन्न होनेवाले उस कर्मविपाक का धर्मध्यानी को विचार करना चाहिए ॥
विवेचन - कर्म का जो उदय - फल देने की उन्मुखता है— उसका नाम विपाक है । वह कर्मविपाक प्रकृति के भेद से, स्थिति के भेद से, प्रदेश के भेद से और अनुभाव के भेद से अनेक प्रकार का होकर भी शुभ (पुण्य) और अशुभ (पाप) इन दो भेदो में विभक्त है। प्रकृति नाम अंश या भेद का