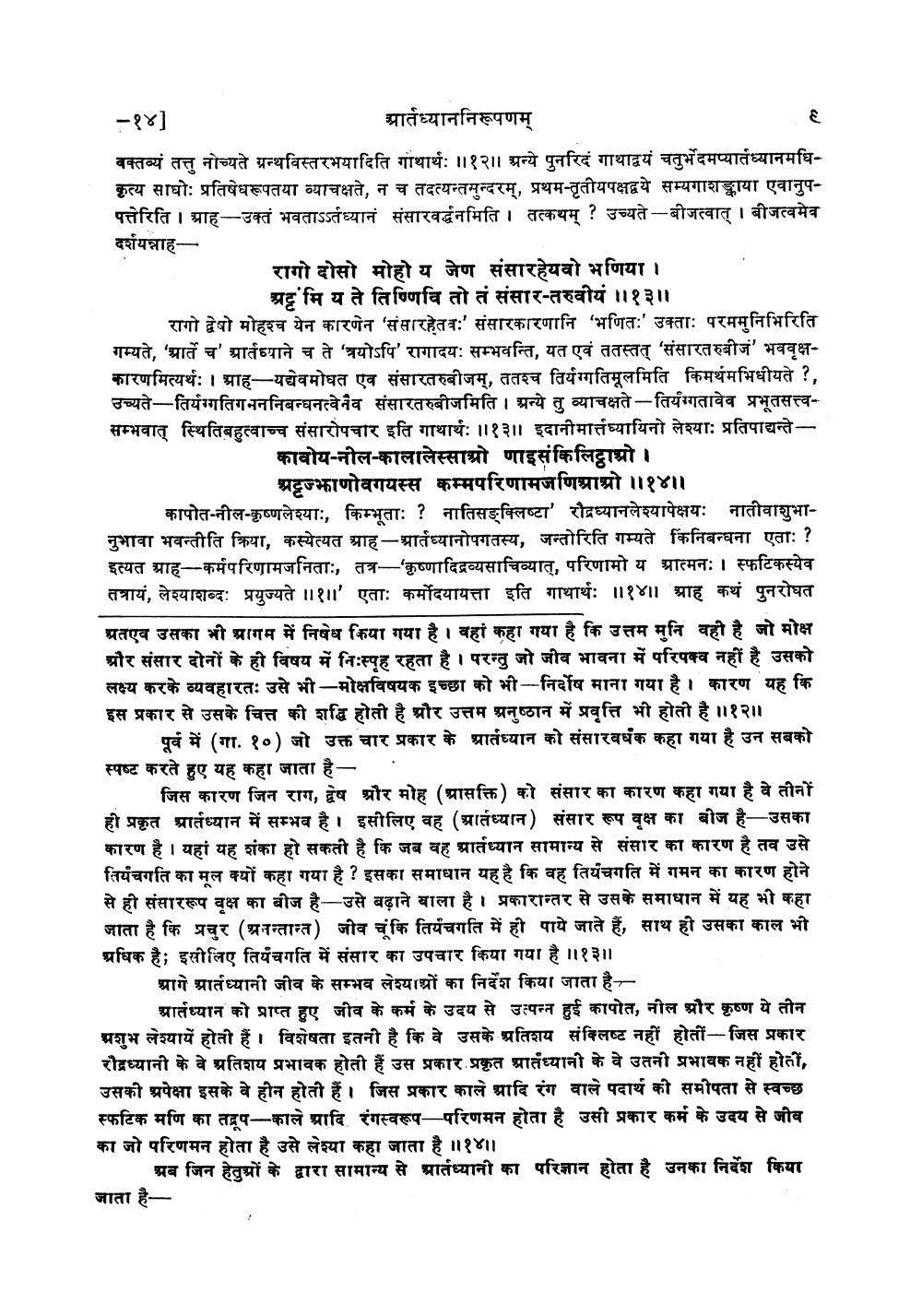________________
-१४]
आर्तध्याननिरूपणम्
वक्तव्यं तत्तु नोच्यते ग्रन्थविस्तरभयादिति गाथार्थः ॥१२।। अन्ये पुनरिदं गाथाद्वयं चतुर्भेदमप्यार्तध्यानमधिकृत्य साधोः प्रतिषेधरूपतया व्याचक्षते, न च तदत्यन्तमुन्दरम्, प्रथम-तृतीयपक्षद्वये सम्यगाशङ्काया एवानुपपत्तेरिति । आह-उक्तं भवताऽऽर्तध्यानं संसारवर्द्धनमिति । तत्कथम् ? उच्यते-बीजत्वात् । बीजत्वमेव दर्शयन्नाह
रागो दोसो मोहो य जेण संसारहेयवो भणिया।
अट्टमि य ते तिण्णिवि तो तं संसार-तरुवीयं ॥१३॥ रागो द्वेषो मोहश्च येन कारणेन 'संसारहेतवः' संसारकारणानि 'भणित:' उक्ताः परममुनिभिरिति गम्यते, 'पार्ते च' प्रार्तध्याने च ते 'त्रयोऽपि' रागादयः सम्भवन्ति, यत एवं ततस्तत् 'संसारतरुबीज' भववृक्षकारणमित्यर्थः । पाह-यद्येवमोधत एव संसारतरुबीजम्, ततश्च तिर्यग्गतिमूलमिति किमर्थमभिधीयते ?, उच्यते-तिर्यग्गतिगमननिबन्धनत्वेनैव संसारतरुबीजमिति । अन्ये तु व्याचक्षते-तिर्यग्गतावेव प्रभूतसत्त्वसम्भवात् स्थितिबहुत्वाच्च संसारोपचार इति गाथार्थः ॥१३॥ इदानीमार्तघ्यायिनो लेश्याः प्रतिपाद्यन्ते
कावोय-नील-कालालेस्साओ पाइसंकिलिट्ठायो।
अट्टज्झाणोवगयस्स कम्मपरिणामजणिप्रानो ॥१४॥ कापोत-नील-कृष्णलेश्याः, किम्भताः ? नातिसक्लिष्टा' रौद्रध्यानलेश्यापेक्षयः नातीवाशुभानुभावा भवन्तीति क्रिया, कस्येत्यत आह-पार्तध्यानोपगतस्य, जन्तोरिति गम्यते किंनिबन्धना एताः ? इत्यत आह-कर्मपरिणामजनिताः, तत्र—'कृष्णादिद्रव्यसाचिव्यात्, परिणामो य आत्मनः । स्फटिकस्येव तत्रायं, लेश्याशब्दः प्रयुज्यते ॥१॥' एताः कर्मोदयायत्ता इति गाथार्थः ॥१४॥ आह कथं पुनरोघत
प्रतएव उसका भी प्रागम में निषेध किया गया है। वहां कहा गया है कि उत्तम मुनि वही है जो मोक्ष और संसार दोनों के ही विषय में निःस्पह रहता है। परन्तु जो जीव भावना में परिपक्व नहीं है उसको लक्ष्य करके व्यवहारतः उसे भी-मोक्षविषयक इच्छा को भी-निर्दोष माना गया है। कारण यह कि इस प्रकार से उसके चित्त की शद्धि होती है और उत्तम अनुष्ठान में प्रवृत्ति भी होती है ॥१२॥
पूर्व में (गा. १०) जो उक्त चार प्रकार के प्रार्तध्यान को संसारवर्धक कहा गया है उन सबको स्पष्ट करते हुए यह कहा जाता है
जिस कारण जिन राग, द्वेष और मोह (प्रासक्ति) को संसार का कारण कहा गया है वे तीनों ही प्रकृत प्रार्तध्यान में सम्भव है। इसीलिए वह (मार्तध्यान) संसार रूप वृक्ष का बीज है-उसका कारण है। यहां यह शंका हो सकती है कि जब वह प्रार्तध्यान सामान्य से संसार का कारण है तब तियंचगति का मूल क्यों कहा गया है ? इसका समाधान यह है कि वह तियंचगति में गमन का कारण होने से ही संसाररूप वृक्ष का बीज है-उसे बढ़ाने वाला है। प्रकारान्तर से उसके समाधान में यह भी कहा जाता है कि प्रचुर (अनन्तान्त) जीव चूंकि तिर्यंचगति में ही पाये जाते हैं, साथ ही उसका काल भी अधिक है। इसीलिए तिर्यंचगति में संसार का उपचार किया गया है ॥१३॥
आगे पार्तध्यानी जीव के सम्भव लेश्याओं का निर्देश किया जाता है
प्रार्तध्यान को प्राप्त हुए जीव के कर्म के उदय से उत्पन्न हुई कापोत, नील और कृष्ण ये तीन प्रशुभ लेश्यायें होती हैं। विशेषता इतनी है कि वे उसके अतिशय संक्लिष्ट नहीं होती-जिस प्रकार रौद्रध्यानी के वे अतिशय प्रभावक होती हैं उस प्रकार प्रकृत प्रार्तध्यानी के वे उतनी प्रभावक नहीं होती, उसकी अपेक्षा इसके वे हीन होती हैं। जिस प्रकार काले प्रादि रंग वाले पदार्थ की समीपता से स्वच्छ स्फटिक मणि का तद्रप-काले प्रादि रंगस्वरूप—परिणमन होता है उसी प्रकार कर्म के उदय से जीव का जो परिणमन होता है उसे लेश्या कहा जाता है ॥१४॥
अब जिन हेतुओं के द्वारा सामान्य से प्रार्तध्यानी का परिज्ञान होता है उनका निर्देश किया जाता है