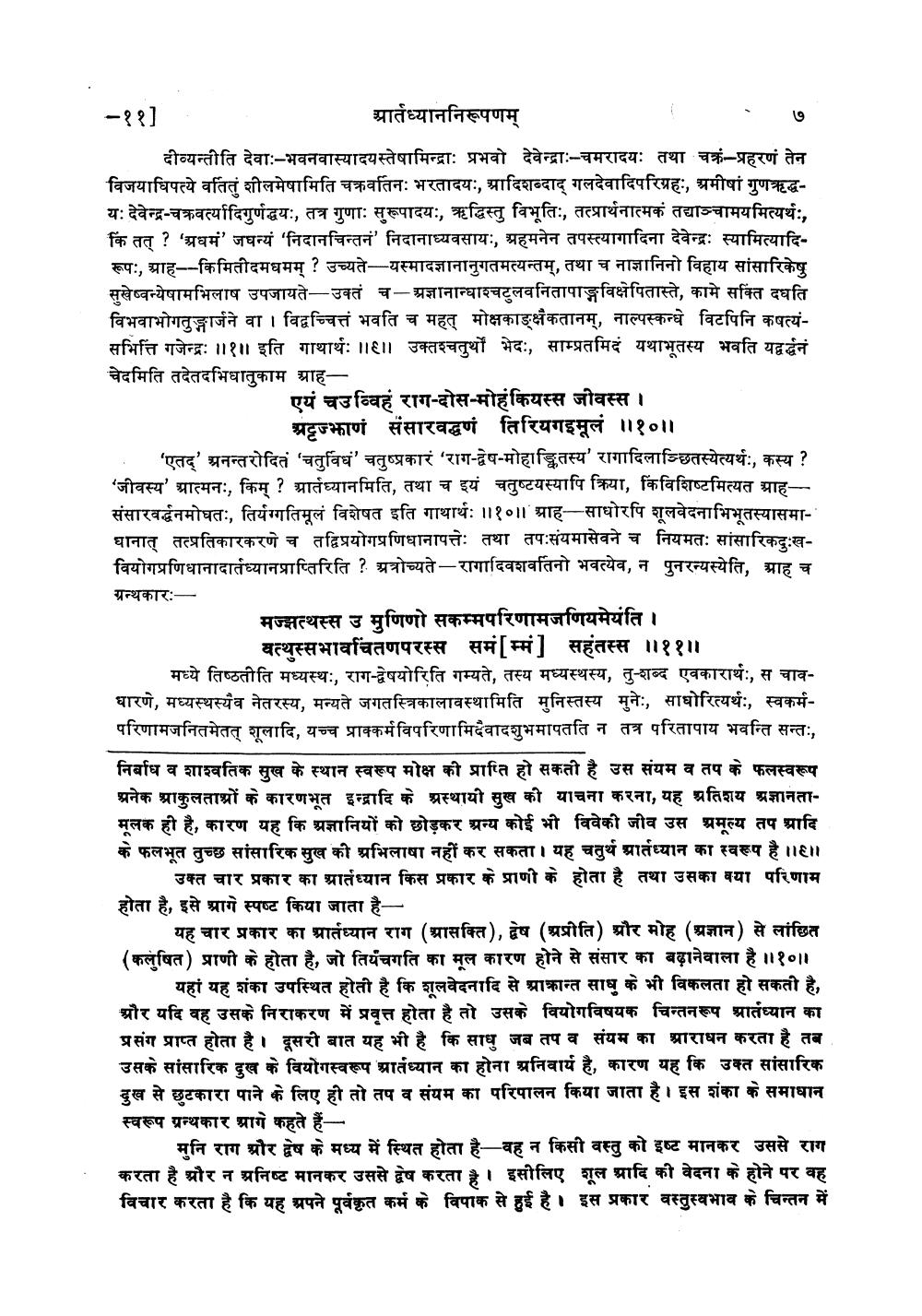________________
-११]
प्रार्तध्याननिरूपणम् दीव्यन्तीति देवा:-भवनवास्यादयस्तेषामिन्द्राः प्रभवो देवेन्द्राः-चमरादयः तथा चक्र-प्रहरणं तेन विजयाधिपत्ये वर्तितुं शीलमेषामिति चक्रवर्तिनः भरतादयः, आदिशब्दाद् गलदेवादिपरिग्रहः, अमीषां गुणऋद्धयः देवेन्द्र-चक्रवादिगुर्णद्धयः, तत्र गुणाः सुरूपादयः, ऋद्धिस्तु विभूतिः, तत्प्रार्थनात्मकं तद्याञ्चामयमित्यर्थः, किं तत् ? 'अधम' जघन्यं "निदानचिन्तनं' निदानाध्यवसायः, अहमनेन तपस्त्यागादिना देवेन्द्रः स्यामित्यादिरूपः, आह--किमितीदमधमम् ? उच्यते-यस्मादज्ञानानुगतमत्यन्तम्, तथा च नाज्ञानिनो विहाय सांसारिकेषु सुखेष्वन्येषामभिलाष उपजायते-उक्तं च–अज्ञानान्धाश्चटुलवनितापाङ्गविक्षेपितास्ते, कामे सक्ति दधति विभवाभोगतुङ्गार्जने वा । विद्वच्चित्तं भवति च महत् मोक्षकाङ्ककतानम्, नाल्पस्कन्धे विटपिनि कषत्यंसभित्ति गजेन्द्रः ॥१॥ इति गाथार्थः ॥६॥ उक्तश्चतुर्थों भेदः, साम्प्रतमिदं यथाभूतस्य भवति यद्वर्द्धनं चेदमिति तदेतदभिधातुकाम आह
एयं चउव्विहं राग-दोस-मोहंकियस्स जीवस्स ।
अट्टज्झाणं संसारवद्धणं तिरियगइमूलं ॥१०॥ . 'एतद्' अनन्तरोदितं 'चतुर्विधं' चतुष्प्रकारं 'राग-द्वेष-मोहाङ्कितस्य' रागादिलाञ्छितस्येत्यर्थः, कस्य? 'जीवस्य' आत्मनः, किम् ? आर्तध्यानमिति, तथा च इयं चतुष्टयस्यापि क्रिया, किंविशिष्टमित्यत आहसंसारवर्द्धनमोघतः, तिर्यग्गतिमूलं विशेषत इति गाथार्थः ॥१०॥ पाह-साधोरपि शूलवेदनाभिभतस्यासमाघानात् तत्प्रतिकारकरणे च तद्विप्रयोगप्रणिधानापत्तेः तथा तपःसंयमासेवने च नियमतः सांसारिकदःखवियोगप्रणिधानादार्तध्यानप्राप्तिरिति ? अत्रोच्यते-रागादिवशवतिनो भवत्येव, न पुनरन्यस्येति, आह च ग्रन्थकार:
मज्झत्थस्स उ मुणिणो सकम्मपरिणामजणियमेयंति ।
वत्थुस्सभावचितणपरस्स समं[म्मं] सहतस्स ॥११॥ मध्ये तिष्ठतीति मध्यस्थः, राग-द्वेषयोरिति गम्यते, तस्य मध्यस्थस्य, तु-शब्द एवकारार्थः, स चावधारणे, मध्यस्थस्यैव नेतरस्य, मन्यते जगतस्त्रिकालावस्थामिति मुनिस्तस्य मुनेः, साधोरित्यर्थः, स्वकर्मपरिणामजनितमेतत् शूलादि, यच्च प्राक्कर्म विपरिणामिदैवादशुभमापतति न तत्र परितापाय भवन्ति सन्तः, निर्बाध व शाश्वतिक सुख के स्थान स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है उस संयम व तप के फलस्वरूप अनेक प्राकुलताओं के कारणभूत इन्द्रादि के अस्थायी सुख की याचना करना, यह अतिशय अज्ञानतामूलक ही है, कारण यह कि अज्ञानियों को छोड़कर अन्य कोई भी विवेकी जीव उस अमूल्य तप आदि के फलभूत तुच्छ सांसारिक सुख की अभिलाषा नहीं कर सकता। यह चतुर्थ प्रार्तध्यान का स्वरूप है।
उक्त चार प्रकार का प्रार्तध्यान किस प्रकार के प्राणी के होता है तथा उसका क्या परिणाम होता है, इसे पागे स्पष्ट किया जाता है
यह चार प्रकार का प्रार्तध्यान राग (प्रासक्ति), द्वेष (अप्रीति) और मोह (अज्ञान) से लांछित (कलुषित) प्राणी के होता है, जो तियंचगति का मूल कारण होने से संसार का बढ़ानेवाला है ॥१०॥
यहां यह शंका उपस्थित होती है कि शूलवेदनादि से आक्रान्त साधु के भी विकलता हो सकती है, और यदि वह उसके निराकरण में प्रवृत्त होता है तो उसके वियोगविषयक चिन्तनरूप प्रार्तध्यान का प्रसंग प्राप्त होता है। दूसरी बात यह भी है कि साधु जब तप व संयम का पाराधन करता है तब उसके सांसारिक दुख के वियोगस्वरूप प्रार्तध्यान का होना अनिवार्य है, कारण यह कि उक्त सांसारिक दुख से छुटकारा पाने के लिए ही तो तप व संयम का परिपालन किया जाता है। इस शंका के समाधान स्वरूप ग्रन्थकार आगे कहते हैं
मुनि राग और द्वेष के मध्य में स्थित होता है वह न किसी वस्तु को इष्ट मानकर उससे राग करता है और न अनिष्ट मानकर उससे द्वेष करता है। इसीलिए शूल आदि की वेदना के होने पर वह विचार करता है कि यह अपने पूर्वकृत कर्म के विपाक से हुई है। इस प्रकार वस्तुस्वभाव के चिन्तन में