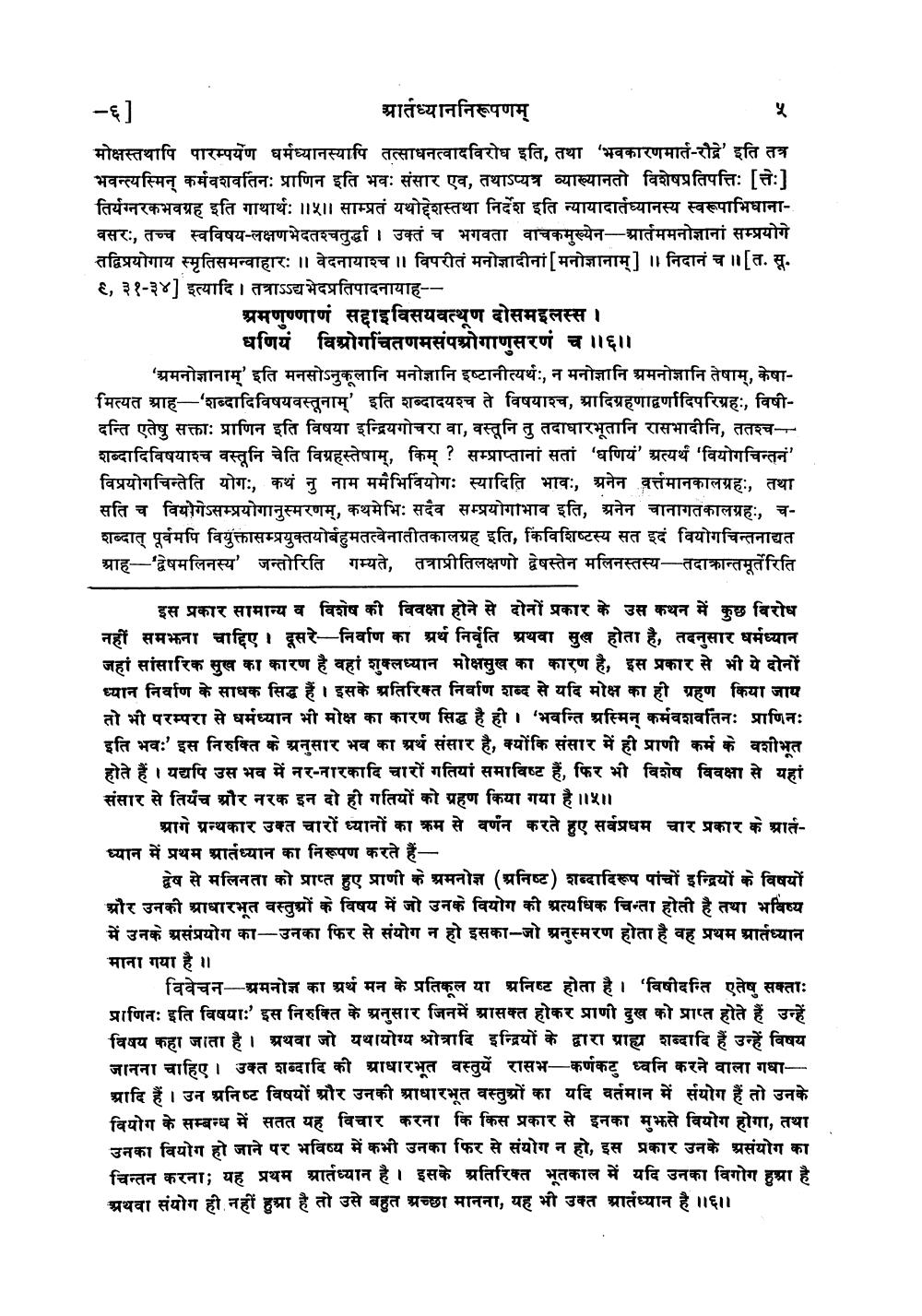________________
-६]
आर्तध्याननिरूपणम्
५
मोक्षस्तथापि पारम्पर्येण धर्मध्यानस्यापि तत्साधनत्वादविरोध इति, तथा 'भवकारणमार्त- रौद्रे' इति तत्र भवन्त्यस्मिन् कर्मवशवर्तिनः प्राणिन इति भवः संसार एव, तथाऽप्यत्र व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः [त्तेः ] तिर्यग्नरकभवग्रह इति गाथार्थः ||५|| साम्प्रतं यथोद्देशस्तथा निर्देश इति न्यायादार्तध्यानस्य स्वरूपाभिधानावसरः, तच्च स्वविषय- लक्षणभेदतश्चतुर्द्धा । उक्तं च भगवता वाचकमुख्येन - आर्तममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः । वेदनायाश्च ॥ विपरीतं मनोज्ञादीनां [ मनोज्ञानाम् ] ॥ निदानं च ॥ [त. सू. ६, ३१-३४] इत्यादि । तत्राऽऽद्य भेदप्रतिपादनायाह-
श्रमणाणं सद्दाइविसयवत्थूण दोसमइलस्स । धणियं विश्रोर्गाचितणमसंपश्रोगाणुसरणं च ॥६॥
‘अमनोज्ञानाम्' इति मनसोऽनुकूलानि मनोज्ञानि इष्टानीत्यर्थः, न मनोज्ञानि अमनोज्ञानि तेषाम्, केषामित्यत आह— 'शब्दादिविषयवस्तूनाम्' इति शब्दादयश्च ते विषयाश्च, आदिग्रहणाद्वर्णादिपरिग्रहः, विषीदन्ति तेषु सक्ताः प्राणिन इति विषया इन्द्रियगोचरा वा, वस्तूनि तु तदाधारभूतानि रासभादीनि ततश्च--- शब्दादिविषयाश्च वस्तूनि चेति विग्रहस्तेषाम् किम् ? सम्प्राप्तानां सतां 'घणियं' प्रत्यर्थं 'वियोगचिन्तनं' विप्रयोगचिन्तेति योगः, कथं नु नाम ममैभिर्वियोगः स्यादिति भावः अनेन वर्त्तमानकालग्रहः, तथा सति च वियोगेऽसम्प्रयोगानुस्मरणम्, कथमेभिः सदैव सम्प्रयोगाभाव इति, अनेन चानागतकालग्रहः, चशब्दात् पूर्वमपि वियुक्तासम्प्रयुक्तयोर्बहुमतत्वेनातीतकालग्रह इति, किंविशिष्टस्य सत इदं वियोगचिन्तनाद्यत आह— 'द्वेषमलिनस्य' जन्तोरिति गम्यते, तत्राप्रीतिलक्षणो द्वेषस्तेन मलिनस्तस्य –— तदाक्रान्तमूर्तेरिति
इस प्रकार सामान्य व विशेष की विवक्षा होने से दोनों प्रकार के उस कथन में कुछ विरोध नहीं समझना चाहिए। दूसरे — निर्वाण का अर्थ निर्वृति अथवा सुख होता है, तदनुसार धर्मध्यान जहां सांसारिक सुख का कारण है वहां शुक्लध्यान मोक्षसुख का कारण है, इस प्रकार से भी ये दोनों ध्यान निर्वाण के साधक सिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त निर्वाण शब्द से यदि मोक्ष का ही ग्रहण किया जाय तो भी परम्परा से धर्मध्यान भी मोक्ष का कारण सिद्ध है ही । 'भवन्ति श्रस्मिन् कर्मवशवर्तिनः प्राणिनः इति भव:' इस निरुक्ति के अनुसार भव का अर्थ संसार है, क्योंकि संसार में ही प्राणी कर्म के वशीभूत होते हैं । यद्यपि उस भव में नर-नारकादि चारों गतियां समाविष्ट हैं, फिर भी विशेष विवक्षा से यहां संसार से तिथंच और नरक इन दो हो गतियों को ग्रहण किया गया है ॥ ५ ॥
नागे ग्रन्थकार उक्त चारों ध्यानों का क्रम से वर्णन करते हुए सर्वप्रथम चार प्रकार के प्रार्तध्यान में प्रथम श्रार्तध्यान का निरूपण करते हैं
द्वेष से मलिनता को प्राप्त हुए प्राणी के अमनोज्ञ ( अनिष्ट) शब्दादिरूप पांचों इन्द्रियों के विषयों और उनकी आधारभूत वस्तुनों के विषय में जो उनके वियोग की अत्यधिक चिन्ता होती है तथा भविष्य में उनके असंप्रयोग का उनका फिर से संयोग न हो इसका जो अनुस्मरण होता है वह प्रथम श्रार्तध्यान माना गया है ॥
विवेचन – अमनोज्ञ का अर्थ मन के प्रतिकूल या अनिष्ट होता है । 'विषीदन्ति एतेषु सक्ताः प्राणिनः इति विषया:' इस निरुक्ति के अनुसार जिनमें आसक्त होकर प्राणी दुख को प्राप्त होते हैं उन्हें विषय कहा जाता है । अथवा जो यथायोग्य श्रोत्रादि इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्य शब्दादि हैं उन्हें विषय जानना चाहिए । उक्त शब्दादि की प्राधारभूत वस्तुयें रासभ— कर्णकटु ध्वनि करने वाला गधाआदि हैं । उन अनिष्ट विषयों और उनकी प्राधारभूत वस्तुनों का यदि वर्तमान में संयोग हैं तो उनके वियोग के सम्बन्ध में सतत यह विचार करना कि किस प्रकार से इनका मुझसे वियोग होगा, तथा उनका वियोग हो जाने पर भविष्य में कभी उनका फिर से संयोग न हो, इस प्रकार उनके प्रसंयोग का चिन्तन करना; यह प्रथम श्रार्तध्यान । इसके अतिरिक्त भूतकाल में यदि उनका विगोग हुआ है अथवा संयोग ही नहीं हुआ है तो उसे बहुत अच्छा मानना, यह भी उक्त प्रार्तध्यान है ॥ ६ ॥