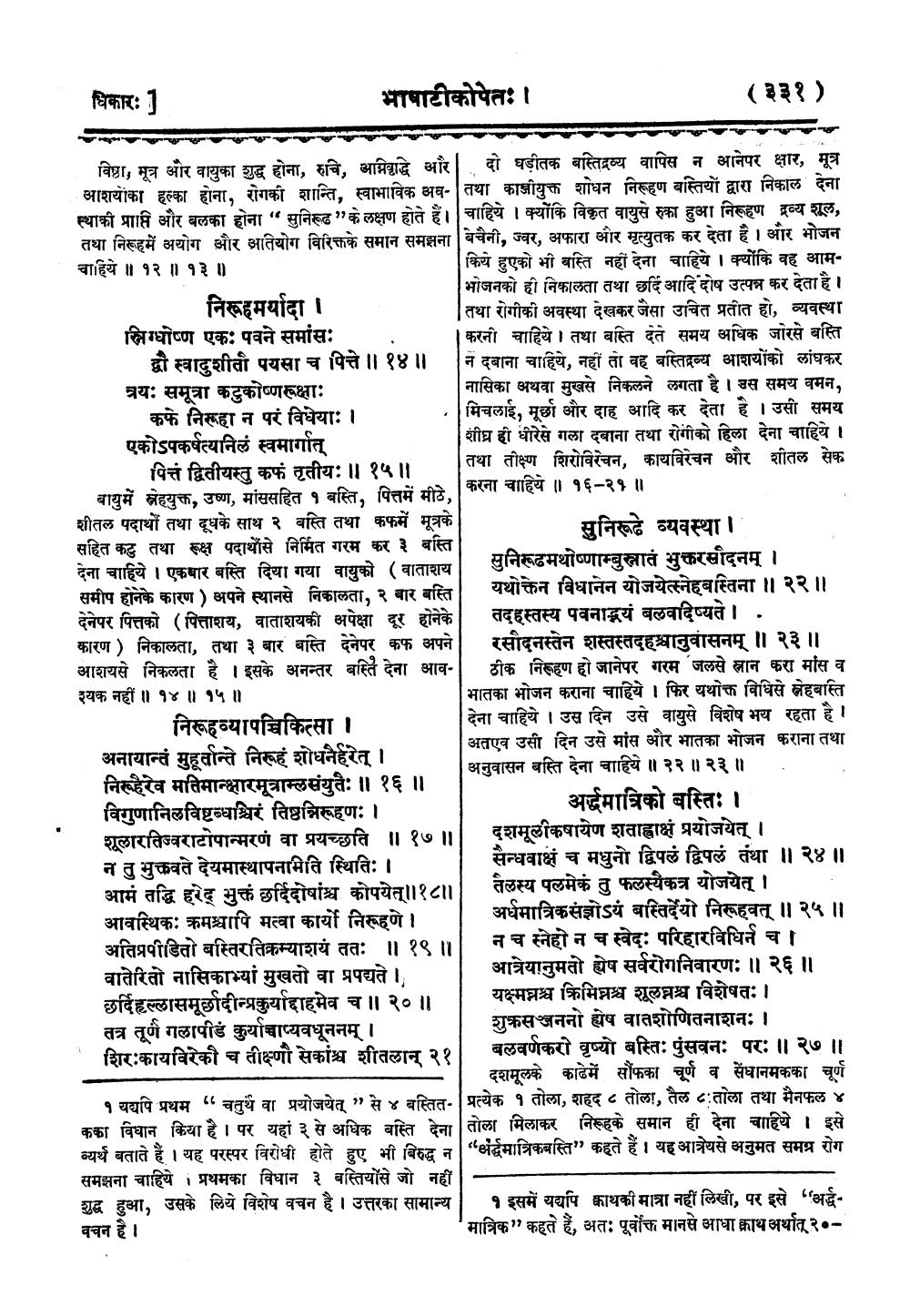________________
धिकारः]
भाषाटीकोपेतः।
(३३१)
विष्ठा, मूत्र और वायुका शुद्ध होना, रुचि, आग्निवाद्ध और दो घड़ीतक बस्तिद्रव्य वापिस न आनेपर क्षार, मूत्र आशयोंका हल्का होना, रोगकी शान्ति, स्वाभाविक अव- तथा काजीयुक्त शोधन निरूहण बस्तियों द्वारा निकाल देना स्थाकी प्राप्ति और बलका होना “ सुनिरूढ" के लक्षण होते हैं। चाहिये । क्योंकि विकृत वायुसे रुका हुआ निरूहण द्रव्य शूल, तथा निरूहमें अयोग और अतियोग विरिक्तके समान समझना | बेचैनी, ज्वर, अफारा और मृत्युतक कर देता है । और भोजन चाहिये ॥ १२ ॥१३॥
|किये हुएको भी बस्ति नहीं देना चाहिये । क्योंकि वह आम
भोजनको ही निकालता तथा छर्दि आदि दोष उत्पन्न कर देता है । निरूहमर्यादा ।
तथा रोगीकी अवस्था देखकर जैसा उचित प्रतीत हो, व्यवस्था स्निग्धोष्ण एकः पवने समांसः . करनी चाहिये। तथा बस्ति देते समय अधिक जोरसे बस्ति
द्वौ स्वादुशीती पयसा च पित्ते ॥१४॥ न दबाना चाहिये, नहीं तो वह बस्तिद्रव्य आशयोंको लांघकर त्रयः समूत्रा कटुकोष्णरूक्षाः
नासिका अथवा मुखसे निकलने लगता है। उस समय वमन, __ कफे निरूहा न परं विधेयाः।
मिचलाई, मूर्छा और दाह आदि कर देता है । उसी समय एकोऽपकर्षत्यनिलं स्वमार्गात्
शीघ्र ही धीरेसे गला दबाना तथा रोगीको हिला देना चाहिये । पित्तं द्वितीयस्तु कर्फ तृतीयः ॥ १५॥
तथा तीक्ष्ण शिरोविरेचन, कायविरेचन और शीतल सेक बायुमें स्नेहयुक्त, उष्ण, मांससहित १ बस्ति, पित्तमें मीठे. करना चाहिये ॥ १६-२१॥ शीतल पदार्थों तथा दूधके साथ २ बस्ति तथा कफमें मूत्रके
सुनिरूढे व्यवस्था। सहित कटु तथा रूक्ष पदार्थोंसे निर्मित गरम कर ३ बस्ति देना चाहिये । एकबार बस्ति दिया गया वायुको (वाताशय
सुनिरूढमथोष्णाम्बुस्नातं भुक्तरसीदनम् । समीप होनेके कारण) अपने स्थानसे निकालता, २ बार बस्ति
यथोक्तेन विधानेन योजयेत्स्नेहबस्तिना ॥ २२॥ देनेपर पित्तको (पित्ताशय, वाताशयकी अपेक्षा दूर होनेके तदहस्तस्य पवनाद्भयं बलवदिष्यते। . कारण) निकालता, तथा ३ बार बस्ति देनेपर कफ अपने रसीदनस्तेन शस्तस्तदहश्वानुवासनम् ॥ २३ ॥ आशयसे निकलता है । इसके अनन्तर बस्ति देना आव- ठीक निरूहण हो जानेपर गरम जलसे स्नान करा मांस व श्यक नहीं ॥ १४ ॥ १५॥
भातका भोजन कराना चाहिये । फिर यथोक्त विधिसे स्नेहबस्ति निरूहव्यापचिकित्सा ।
देना चाहिये । उस दिन उसे वायुसे विशेष भय रहता है ।
अतएव उसी दिन उसे मांस और भातका भोजन कराना तथा अनायान्तं मुहूर्तान्ते निरूहं शोधनहरेत् ।
अनुवासन बस्ति देना चाहिये ॥२२॥२३॥ . निरूहैरेव मतिमान्क्षारमूत्राम्लसंयुतैः ॥ १६ ॥ विगुणानिलविष्टब्धश्चिरं तिष्ठन्निरूहणः ।
__ अर्द्धमात्रिको बस्तिः। शूलारतिज्वराटोपान्मरणं वा प्रयच्छति ॥ १७॥ दशमूलीकषायेण शताह्वाक्षं प्रयोजयेत् । न तु भुक्तवते देयमास्थापनामिति स्थितिः।
सैन्धवाक्षं च मधुनो द्विपलं द्विपलं तथा ॥ २४ ॥ आमं तद्धि हरेद् भुक्तं छर्दिदोषांश्च कोपयेत्॥१८॥ तैलस्य पलमेकं तु फलस्यैकत्र योजयेत् । आवस्थिकः क्रमश्चापि मत्वा कार्यो निरूहणे । अर्धमात्रिकसंज्ञोऽयं बस्तिर्देयो निरूहवत् ॥ २५ ॥ अतिप्रपीडितो बस्तिरतिक्रम्याशयं ततः ॥ १९ ॥
न च स्नेहो न च स्वेदः परिहारविधिर्न च । वातेरितो नासिकाभ्यां मुखतो वा प्रपद्यते ।
आत्रेयानुमतो ह्येष सर्वरोगनिवारणः ॥२६॥ छर्दिहल्लासमू दीन्प्रकुर्याद्दाहमेव च ॥ २०॥ यक्ष्मन्नश्च क्रिमिन्नश्च शूलनश्च विशेषतः। तत्र तूर्ण गलापीडं कुर्याच्चाप्यवधूननम् ।
शुक्रसजननो ह्येष वातशोणितनाशनः । शिरःकायविरेको च तीक्ष्णौ सेकांश्च शीतलान् २१] बलवर्णकरो वृष्यो बस्तिः पुंसवनः परः ॥२७ ।।
दशमूलके काढेमें सौंफका चूर्ण व सेंधानमकका चूर्ण १ यद्यपि प्रथम " चतुर्थ वा प्रयोजयेत् " से ४ बस्तित- प्रत्येक १ तोला, शहद ८ तोला, तैल ८:तोला तथा मैनफल ४ कका विधान किया है । पर यहां ३ से अधिक बस्ति देना | तोला मिलाकर निरूहके समान ही देना चाहिये । इसे व्यर्थ बताते हैं । यह परस्पर विरोधी होते हुए भी बिरुद्ध न | "अर्द्धमात्रिकबस्ति" कहते हैं । यह आत्रेयसे अनुमत समग्र रोग समझना चाहिये । प्रथमका विधान ३ बस्तियोंसे जो नहीं|शुद्ध हुआ, उसके लिये विशेष वचन है। उत्तरका सामान्य | १ इसमें यद्यपि काथकी मात्रा नहीं लिखी, पर इसे "अर्द्धवचन है।
मात्रिक" कहते हैं, अतः पूर्वोक्त मानसे आधा वाथअर्थात् २०