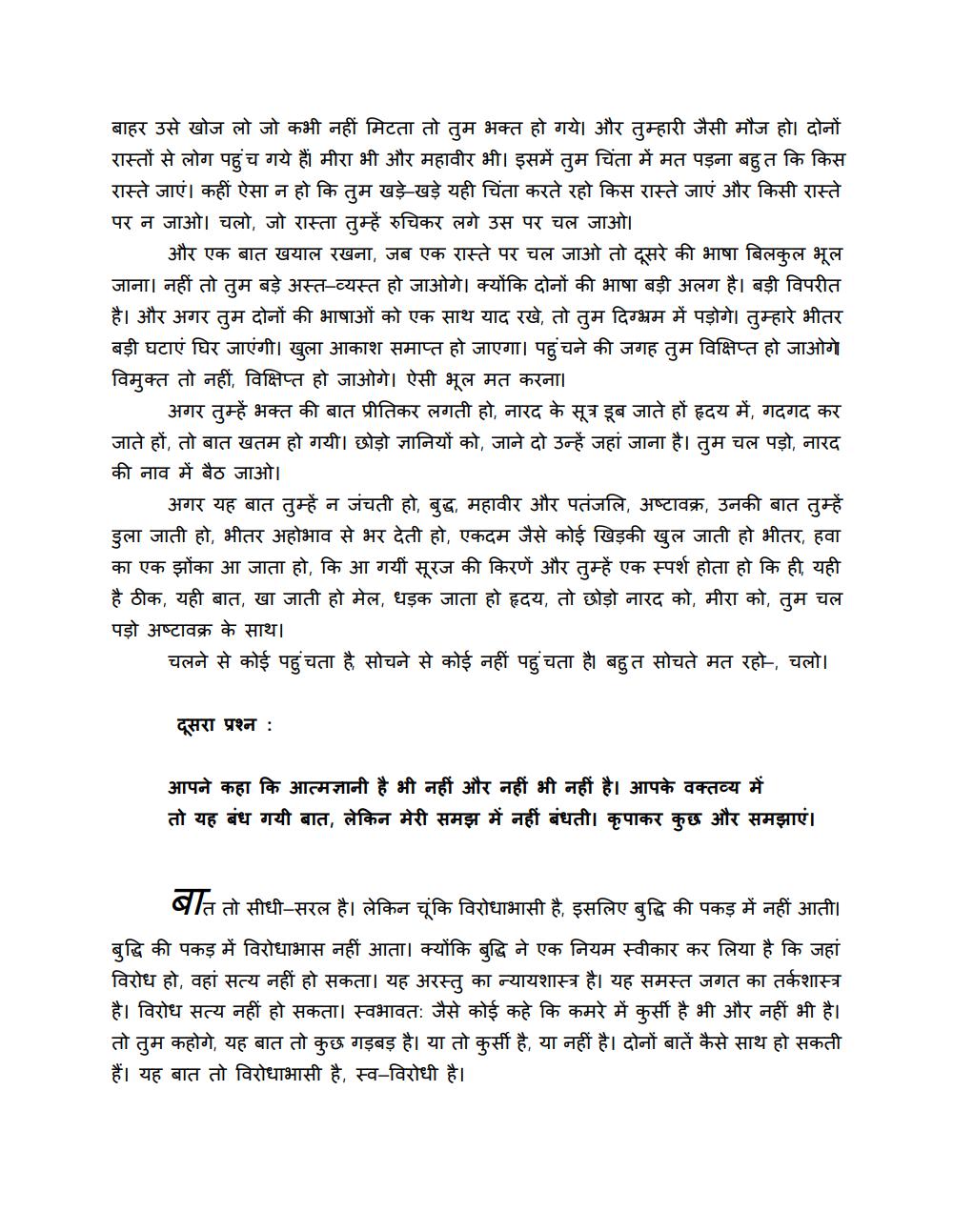________________
बाहर उसे खोज लो जो कभी नहीं मिटता तो तुम भक्त हो गये। और तुम्हारी जैसी मौज हो। दोनों रास्तों से लोग पहुंच गये हैं। मीरा भी और महावीर भी। इसमें तुम चिंता में मत पड़ना बहुत कि किस रास्ते जाएं। कहीं ऐसा न हो कि तुम खड़े-खड़े यही चिंता करते रहो किस रास्ते जाएं और किसी रास्ते पर न जाओ। चलो, जो रास्ता तुम्हें रुचिकर लगे उस पर चल जाओ।
और एक बात खयाल रखना, जब एक रास्ते पर चल जाओ तो दूसरे की भाषा बिलकुल भूल जाना। नहीं तो तुम बड़े अस्त-व्यस्त हो जाओगे। क्योंकि दोनों की भाषा बड़ी अलग है। बड़ी विपरीत है। और अगर तुम दोनों की भाषाओं को एक साथ याद रखे, तो तुम दिग्भ्रम में पड़ोगे। तुम्हारे भीतर बड़ी घटाएं घिर जाएंगी। खुला आकाश समाप्त हो जाएगा। पहुंचने की जगह तुम विक्षिप्त हो जाओगे विमुक्त तो नहीं, विक्षिप्त हो जाओगे। ऐसी भूल मत करना।
अगर तुम्हें भक्त की बात प्रीतिकर लगती हो, नारद के सूत्र इब जाते हों हृदय में, गदगद कर जाते हों, तो बात खतम हो गयी। छोड़ो ज्ञानियों को, जाने दो उन्हें जहां जाना है। तुम चल पड़ो, नारद की नाव में बैठ जाओ।
अगर यह बात तुम्हें न जंचती हो, बुद्ध, महावीर और पतंजलि, अष्टावक्र, उनकी बात तुम्हें डुला जाती हो, भीतर अहोभाव से भर देती हो, एकदम जैसे कोई खिड़की खुल जाती हो भीतर, हवा का एक झोंका आ जाता हो, कि आ गयीं सूरज की किरणें और तुम्हें एक स्पर्श होता हो कि ही, यही है ठीक, यही बात, खा जाती हो मेल, धड़क जाता हो हृदय, तो छोड़ो नारद को, मीरा को, तुम चल पड़ो अष्टावक्र के साथ।
चलने से कोई पहुंचता है सोचने से कोई नहीं पहुंचता है। बहुत सोचते मत रहो, चलो।
दूसरा प्रश्न :
आपने कहा कि आत्मज्ञानी है भी नहीं और नहीं भी नहीं है। आपके वक्तव्य में तो यह बंध गयी बात, लेकिन मेरी समझ में नहीं बंधती| कृपाकर कुछ और समझाएं।
बात तो सीधी-सरल है। लेकिन चूंकि विरोधाभासी है, इसलिए बुद्धि की पकड़ में नहीं आती। बुद्धि की पकड़ में विरोधाभास नहीं आता। क्योंकि बुद्धि ने एक नियम स्वीकार कर लिया है कि जहां विरोध हो, वहां सत्य नहीं हो सकता। यह अरस्तु का न्यायशास्त्र है। यह समस्त जगत का तर्कशास्त्र है। विरोध सत्य नहीं हो सकता। स्वभावत: जैसे कोई कहे कि कमरे में कुर्सी है भी और नहीं भी है। तो तुम कहोगे, यह बात तो कुछ गड़बड़ है। या तो की है, या नहीं है। दोनों बातें कैसे साथ हो सकती हैं। यह बात तो विरोधाभासी है, स्व-विरोधी है।