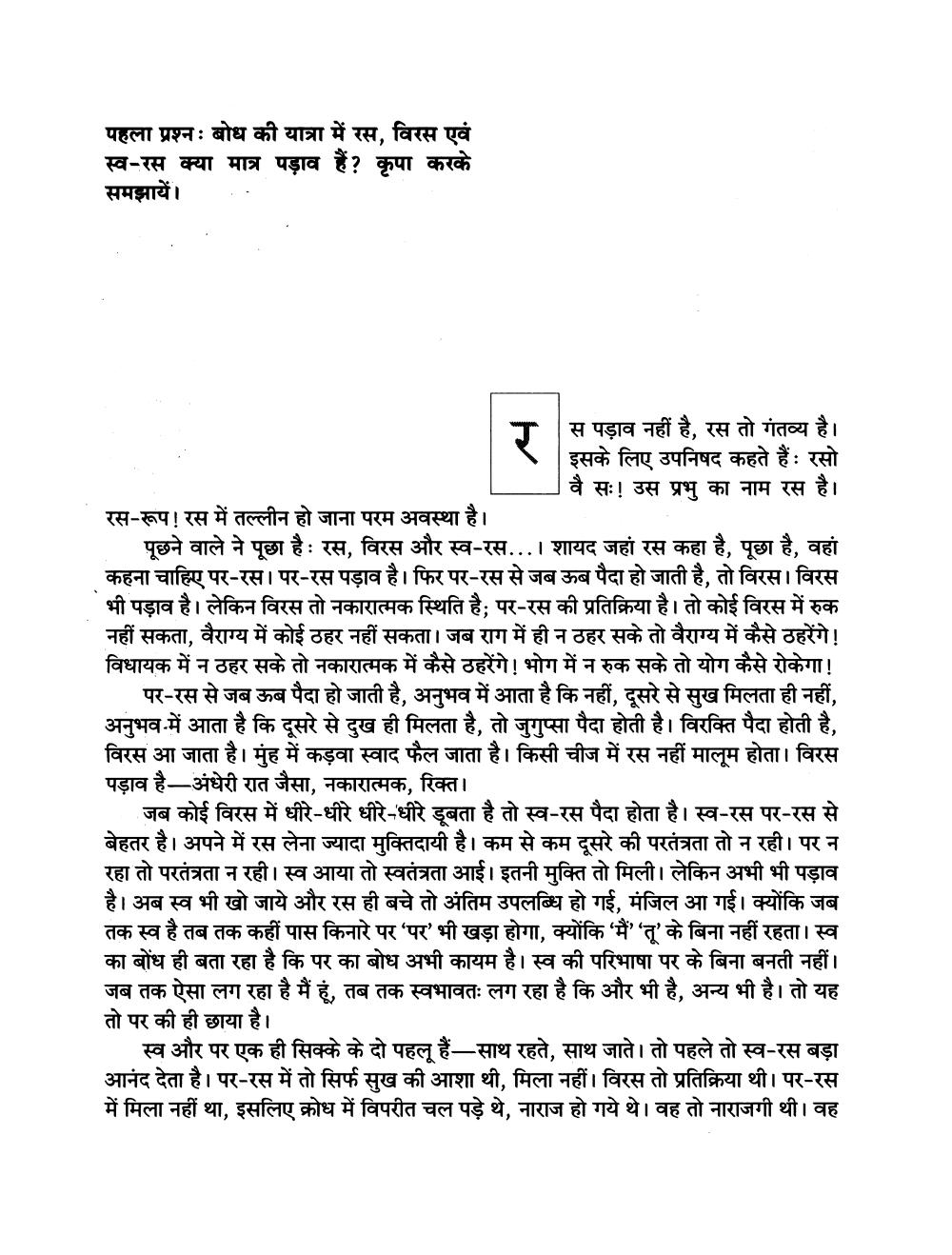________________
पहला प्रश्नः बोध की यात्रा में रस, विरस एवं स्व-रस क्या मात्र पड़ाव हैं? कृपा करके समझायें।
स पड़ाव नहीं है, रस तो गंतव्य है। | इसके लिए उपनिषद कहते हैं : रसो
- वै सः! उस प्रभु का नाम रस है। रस-रूप! रस में तल्लीन हो जाना परम अवस्था है।
पूछने वाले ने पूछा है : रस, विरस और स्व-रस... । शायद जहां रस कहा है, पूछा है, वहां कहना चाहिए पर-रस। पर-रस पड़ाव है। फिर पर-रस से जब ऊब पैदा हो जाती है, तो विरस। विरस भी पड़ाव है। लेकिन विरस तो नकारात्मक स्थिति है; पर-रस की प्रतिक्रिया है। तो कोई विरस में रुक नहीं सकता, वैराग्य में कोई ठहर नहीं सकता। जब राग में ही न ठहर सके तो वैराग्य में कैसे ठहरेंगे! विधायक में न ठहर सके तो नकारात्मक में कैसे ठहरेंगे! भोग में न रुक सके तो योग कैसे रोकेगा!
पर-रस से जब ऊब पैदा हो जाती है, अनुभव में आता है कि नहीं, दूसरे से सुख मिलता ही नहीं, अनुभव में आता है कि दूसरे से दुख ही मिलता है, तो जुगुप्सा पैदा होती है। विरक्ति पैदा होती है, विरस आ जाता है। मुंह में कड़वा स्वाद फैल जाता है। किसी चीज में रस नहीं मालूम होता। विरस पड़ाव है-अंधेरी रात जैसा. नकारात्मक. रिक्त।
जब कोई विरस में धीरे-धीरे धीरे-धीरे डूबता है तो स्व-रस पैदा होता है। स्व-रस पर-रस से बेहतर है। अपने में रस लेना ज्यादा मुक्तिदायी है। कम से कम दूसरे की परतंत्रता तो न रही। पर न रहा तो परतंत्रता न रही। स्व आया तो स्वतंत्रता आई। इतनी मुक्ति तो मिली। लेकिन अभी भी पड़ाव है। अब स्व भी खो जाये और रस ही बचे तो अंतिम उपलब्धि हो गई, मंजिल आ गई। क्योंकि जब तक स्व है तब तक कहीं पास किनारे पर 'पर' भी खड़ा होगा, क्योंकि 'मैं' 'तू' के बिना नहीं रहता। स्व का बोध ही बता रहा है कि पर का बोध अभी कायम है। स्व की परिभाषा पर के बिना बनती नहीं। जब तक ऐसा लग रहा है मैं हूं, तब तक स्वभावतः लग रहा है कि और भी है, अन्य भी है। तो यह तो पर की ही छाया है। __स्व और पर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं—साथ रहते, साथ जाते। तो पहले तो स्व-रस बड़ा आनंद देता है। पर-रस में तो सिर्फ सुख की आशा थी, मिला नहीं। विरस तो प्रतिक्रिया थी। पर-रस में मिला नहीं था, इसलिए क्रोध में विपरीत चल पड़े थे, नाराज हो गये थे। वह तो नाराजगी थी। वह