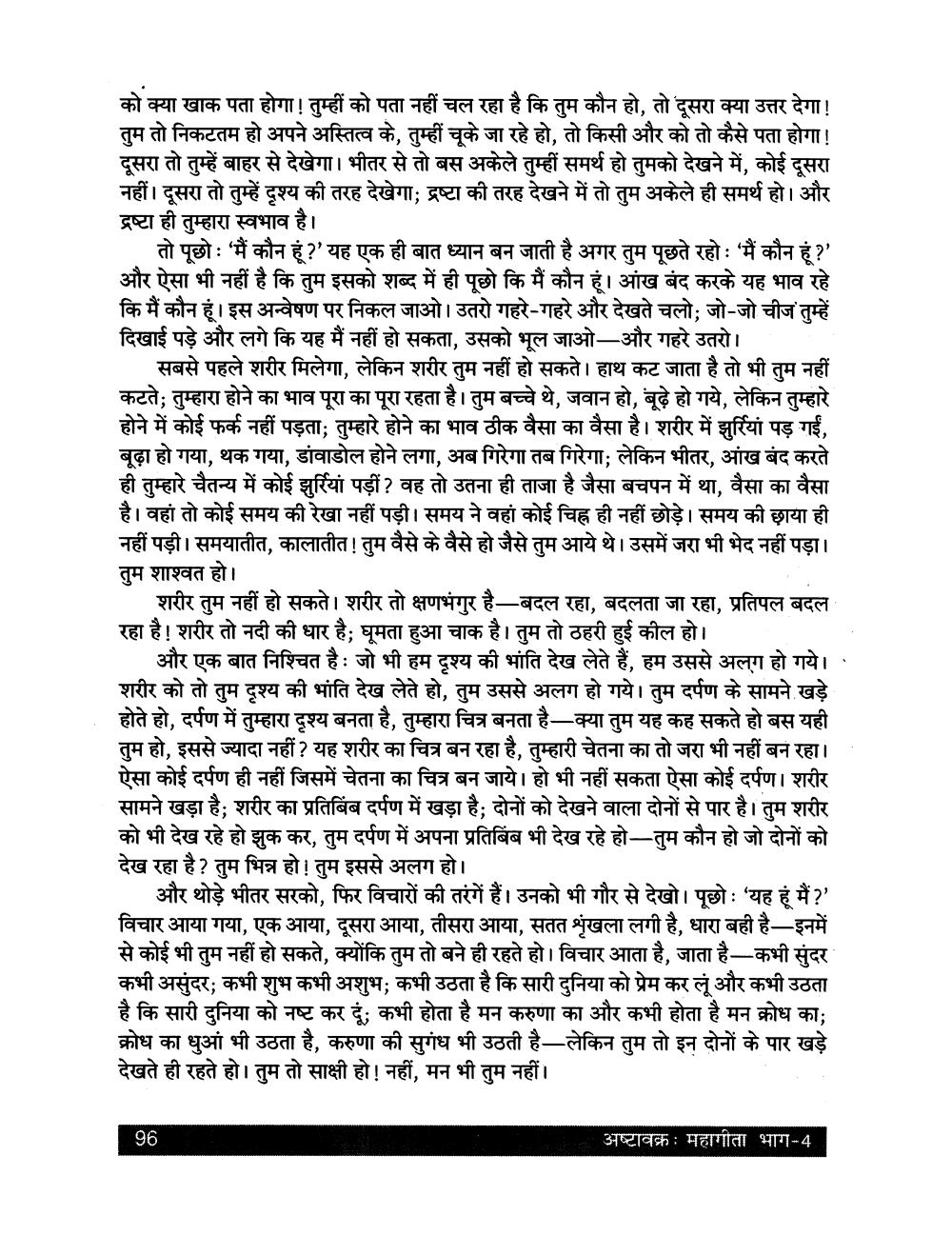________________
को क्या खाक पता होगा ! तुम्हीं को पता नहीं चल रहा है कि तुम कौन हो, तो दूसरा क्या उत्तर देगा! तुम तो निकटतम हो अपने अस्तित्व के, तुम्हीं चूके जा रहे हो, तो किसी और को तो कैसे पता होगा ! दूसरा तो तुम्हें बाहर से देखेगा। भीतर से तो बस अकेले तुम्हीं समर्थ हो तुमको देखने में, कोई दूसरा नहीं। दूसरा तो तुम्हें दृश्य की तरह देखेगा; द्रष्टा की तरह देखने में तो तुम अकेले ही समर्थ हो। और द्रष्टा ही तुम्हारा स्वभाव है।
तो पूछो: 'मैं कौन हूं?' यह एक ही बात ध्यान बन जाती है अगर तुम पूछते रहो : 'मैं कौन हूं ?' और ऐसा भी नहीं है कि तुम इसको शब्द में ही पूछो कि मैं कौन हूं। आंख बंद करके यह भाव रहे कि कौन हूं। इस अन्वेषण पर निकल जाओ । उतरो गहरे-गहरे और देखते चलो; जो-जो चीज तुम्हें दिखाई पड़े और लगे कि यह मैं नहीं हो सकता, उसको भूल जाओ – और गहरे उतरो ।
-
था,
सबसे पहले शरीर मिलेगा, लेकिन शरीर तुम नहीं हो सकते। हाथ कट जाता है तो भी तुम नहीं कटते; तुम्हारा होने का भाव पूरा का पूरा रहता है। तुम बच्चे थे, जवान हो, बूढ़े हो गये, लेकिन तुम्हारे होने में कोई फर्क नहीं पड़ता; तुम्हारे होने का भाव ठीक वैसा का वैसा है। शरीर में झुर्रियां पड़ गईं, बूढ़ा हो गया, थक गया, डांवाडोल होने लगा, अब गिरेगा तब गिरेगा; लेकिन भीतर, आंख बंद करते ही तुम्हारे चैतन्य में कोई झुर्रियां पड़ीं? वह तो उतना ही ताजा है जैसा बचपन में वैसा का वैसा है। वहां तो कोई समय की रेखा नहीं पड़ी। समय ने वहां कोई चिह्न ही नहीं छोड़े। समय की छाया ही नहीं पड़ी। समयातीत, कालातीत! तुम वैसे के वैसे हो जैसे तुम आये थे। उसमें जरा भी भेद नहीं पड़ा। तुम शाश्वत हो ।
शरीर तुम नहीं हो सकते। शरीर तो क्षणभंगुर है— बदल रहा, बदलता जा रहा, प्रतिपल बदल रहा है ! शरीर तो नदी की धार है; घूमता हुआ चाक है। तुम तो ठहरी हुई कील हो ।
और एक बात निश्चित है : जो भी हम दृश्य की भांति देख लेते हैं, हम उससे अलग हो गये । शरीर को तो तुम दृश्य की भांति देख लेते हो, तुम उससे अलग हो गये। तुम दर्पण के सामने खड़े होते हो, दर्पण में तुम्हारा दृश्य बनता है, तुम्हारा चित्र बनता है- - क्या तुम यह कह सकते हो बस यही तुम हो, इससे ज्यादा नहीं ? यह शरीर का चित्र बन रहा है, तुम्हारी चेतना का तो जरा भी नहीं बन रहा। ऐसा कोई दर्पण ही नहीं जिसमें चेतना का चित्र बन जाये । हो भी नहीं सकता ऐसा कोई दर्पण । शरीर सामने खड़ा है; शरीर का प्रतिबिंब दर्पण में खड़ा है; दोनों को देखने वाला दोनों से पार है। तुम शरीर को भी देख रहे हो झुक कर, तुम दर्पण में अपना प्रतिबिंब भी देख रहे हो – तुम कौन हो जो दोनों को देख रहा है? तुम भिन्न हो ! तुम इससे अलग हो ।
T
-
और थोड़े भीतर सरको, फिर विचारों की तरंगें हैं । उनको भी गौर से देखो। पूछो: 'यह हूं मैं?' विचार आया गया, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सतत श्रृंखला लगी है, धारा बही है – इनमें से कोई भी तुम नहीं हो सकते, क्योंकि तुम तो बने ही रहते हो । विचार आता है, जाता है— कभी सुंदर कभी असुंदर; कभी शुभ कभी अशुभ; कभी उठता है कि सारी दुनिया को प्रेम कर लूं और कभी उठता है कि सारी दुनिया को नष्ट कर दूं; कभी होता है मन करुणा का और कभी होता है मन क्रोध का; क्रोध का धुआं भी उठता है, करुणा की सुगंध भी उठती है - लेकिन तुम तो इन दोनों के पार खड़े देखते ही रहते हो। तुम तो साक्षी हो ! नहीं, मन भी तुम नहीं।
96
अष्टावक्र: महागीता भाग-4