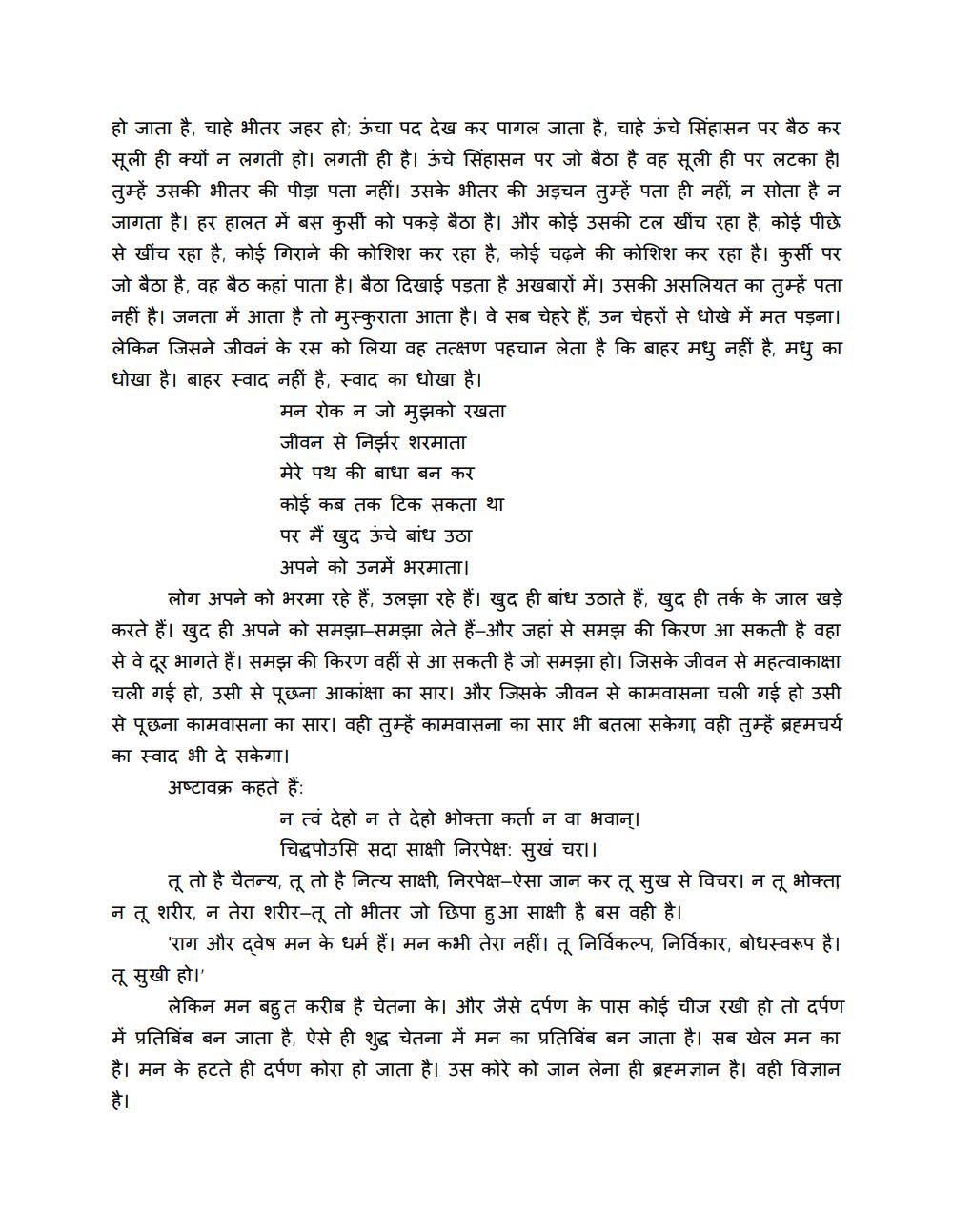________________
हो जाता है, चाहे भीतर जहर हो; ऊंचा पद देख कर पागल जाता है, चाहे ऊंचे सिंहासन पर बैठ कर सूली ही क्यों न लगती हो। लगती ही है। ऊंचे सिंहासन पर जो बैठा है वह सूली ही पर लटका है। तुम्हें उसकी भीतर की पीड़ा पता नहीं। उसके भीतर की अड़चन तुम्हें पता ही नहीं, न सोता है न जागता है। हर हालत में बस कुर्सी को पकड़े बैठा है। और कोई उसकी टल खींच रहा है, कोई पीछे से खींच रहा है, कोई गिराने की कोशिश कर रहा है, कोई चढ़ने की कोशिश कर रहा है। कुर्सी पर जो बैठा है, वह बैठ कहां पाता है। बैठा दिखाई पड़ता है अखबारों में। उसकी असलियत का तुम्हें पता नहीं है। जनता में आता है तो मुस्कुराता आता है। वे सब चेहरे हैं, उन चेहरों से धोखे में मत पड़ना। लेकिन जिसने जीवनं के रस को लिया वह तत्क्षण पहचान लेता है कि बाहर मधु नहीं है, मधु का धोखा है। बाहर स्वाद नहीं है, स्वाद का धोखा है।
मन रोक न जो मुझको रखता जीवन से निर्झर शरमाता मेरे पथ की बाधा बन कर कोई कब तक टिक सकता था पर मैं खुद ऊंचे बांध उठा
अपने को उनमें भरमाता। लोग अपने को भरमा रहे हैं, उलझा रहे हैं। खुद ही बांध उठाते हैं, खुद ही तर्क के जाल खड़े करते हैं। खुद ही अपने को समझा समझा लेते हैं और जहां से समझ की किरण आ सकती है वहा से वे दूर भागते हैं। समझ की किरण वहीं से आ सकती है जो समझा हो। जिसके जीवन से महत्वाकाक्षा चली गई हो, उसी से पूछना आकांक्षा का सार। और जिसके जीवन से कामवासना चली गई हो उसी से पूछना कामवासना का सार। वही तुम्हें कामवासना का सार भी बतला सकेगा वही तुम्हें ब्रह्मचर्य का स्वाद भी दे सकेगा। अष्टावक्र कहते हैं:
न त्वं देहो न ते देहो भोक्ता कर्ता न वा भवान्।
चिद्धपोउसि सदा साक्षी निरपेक्ष: सुखं चर।। तू तो है चैतन्य, तू तो है नित्य साक्षी, निरपेक्ष-ऐसा जान कर तू सुख से विचर। न तू भोक्ता न तू शरीर, न तेरा शरीर-तू तो भीतर जो छिपा हुआ साक्षी है बस वही है।
'राग और द्वेष मन के धर्म हैं। मन कभी तेरा नहीं। तू निर्विकल्प, निर्विकार, बोधस्वरूप है। तू सुखी हो।'
लेकिन मन बहुत करीब है चेतना के। और जैसे दर्पण के पास कोई चीज रखी हो तो दर्पण में प्रतिबिंब बन जाता है, ऐसे ही शुद्ध चेतना में मन का प्रतिबिंब बन जाता है। सब खेल मन का है। मन के हटते ही दर्पण कोरा हो जाता है। उस कोरे को जान लेना ही ब्रह्मज्ञान है। वही विज्ञान