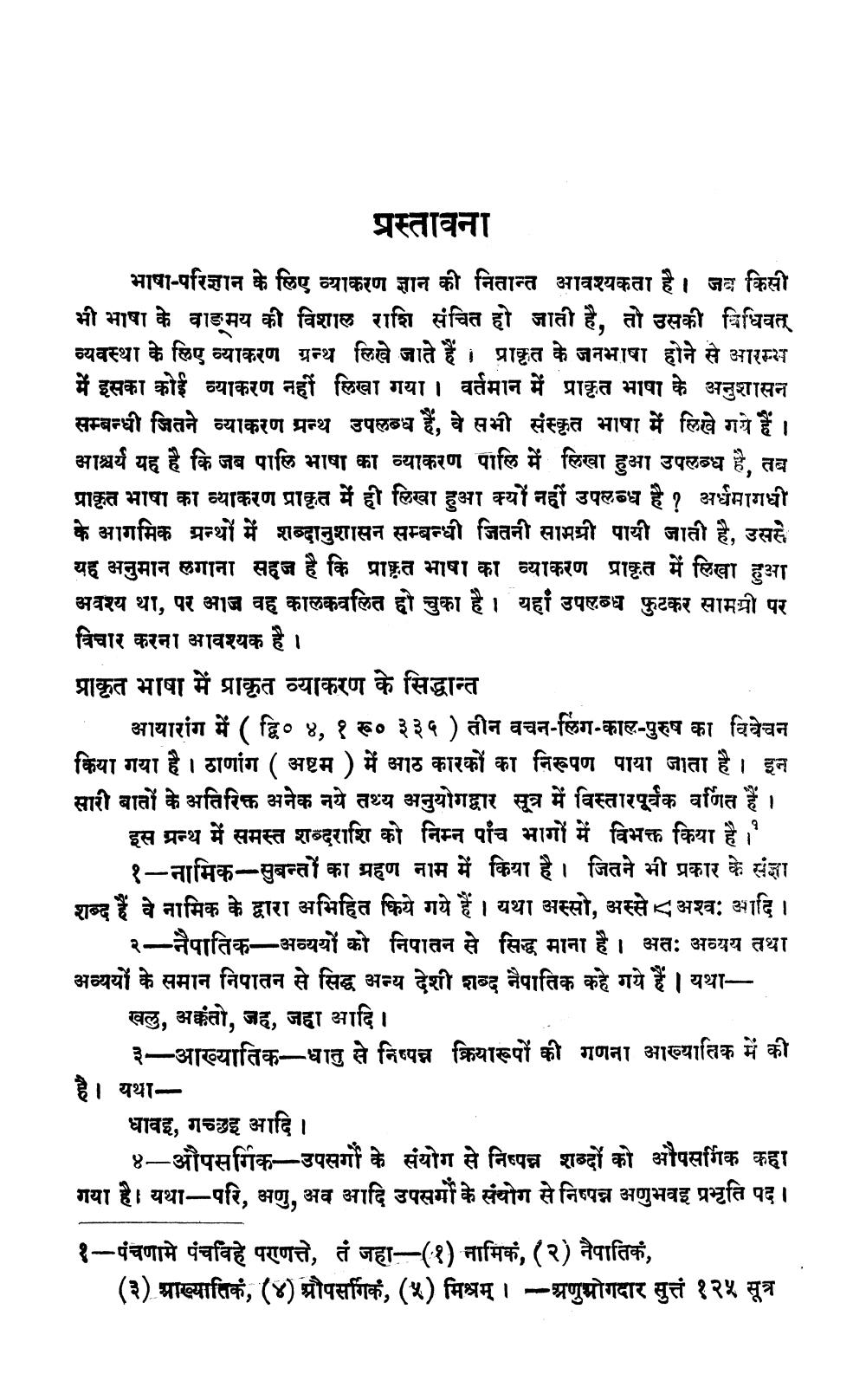________________
प्रस्तावना
भाषा-परिज्ञान के लिए व्याकरण ज्ञान की नितान्त आवश्यकता है। जब किसी भी भाषा के वाङ्मय की विशाल राशि संचित हो जाती है, तो उसकी विधिवत् व्यवस्था के लिए व्याकरण ग्रन्थ लिखे जाते हैं। प्राकृत के जनभाषा होने से आरम्भ में इसका कोई व्याकरण नहीं लिखा गया । वर्तमान में प्राकृत भाषा के अनुशासन सम्बन्धी जितने व्याकरण ग्रन्थ उपलब्ध हैं, वे सभी संस्कृत भाषा में लिखे गये हैं । आश्चर्य यह है कि जब पालि भाषा का व्याकरण पालि में लिखा हुआ उपलब्ध है, तब प्राकृत भाषा का व्याकरण प्राकृत में ही लिखा हुआ क्यों नहीं उपलब्ध है ? अर्धमागधी के आगमिक ग्रन्थों में शब्दानुशासन सम्बन्धी जितनी सामग्री पायी जाती है, उससे यह अनुमान लगाना सहज है कि प्राकृत भाषा का व्याकरण प्राकृत में लिखा हुआ अवश्य था, पर आज वह कालकवलित हो चुका है । यहां उपलब्ध फुटकर सामग्री पर विचार करना आवश्यक है ।
प्राकृत भाषा में प्राकृत व्याकरण के सिद्धान्त
9
रांग में (द्वि०४, १ रू० ३३५ ) तीन वचन-लिंग-काल-पुरुष का विवेचन किया गया है। ठाणांग ( अष्टम ) में आठ कारकों का निरूपण पाया जाता है । इन सारी बातों के अतिरिक्त अनेक नये तथ्य अनुयोगद्वार सूत्र में विस्तारपूर्वक वर्णित हैं । इस ग्रन्थ में समस्त शब्दराशि को निम्न पांच भागों में विभक्त किया है १ - नामिक- सुबन्तों का ग्रहण नाम में किया है। जितने भी प्रकार के संज्ञा शब्द हैं वे नामिक के द्वारा अभिहित किये गये हैं २ – नैपातिक — अव्ययों को निपातन से
।
यथा अस्सो, अस्से । अश्वः आदि । सिद्ध माना है । अतः अव्यय तथा
अव्ययों के समान निपातन से सिद्ध अन्य देशी शब्द नैपातिक कहे गये हैं । यथा
खलु, अक्कंतो, जह, जहा आदि ।
३- आख्यातिक— धातु से निष्पन्न क्रियारूपों की गणना आख्यातिक में की है । यथा
धाव, गच्छ आदि ।
४
- औपसर्गिक — उपसर्गों के संयोग से निष्पन्न शब्दों को औपसर्गिक कहा गया है । यथा-परि, अणु, अव आदि उपसर्गों के संयोग से निष्पन्न अणुभवइ प्रभृति पद ।
१ - पंचनामे पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा – (१) नामिकं, (२) नैपातिकं,
(३) श्राख्यातिकं, (४) प्रौपसर्गिकं, (५) मिश्रम् । अणुभोगदार सुत्तं १२५ सूत्र
-