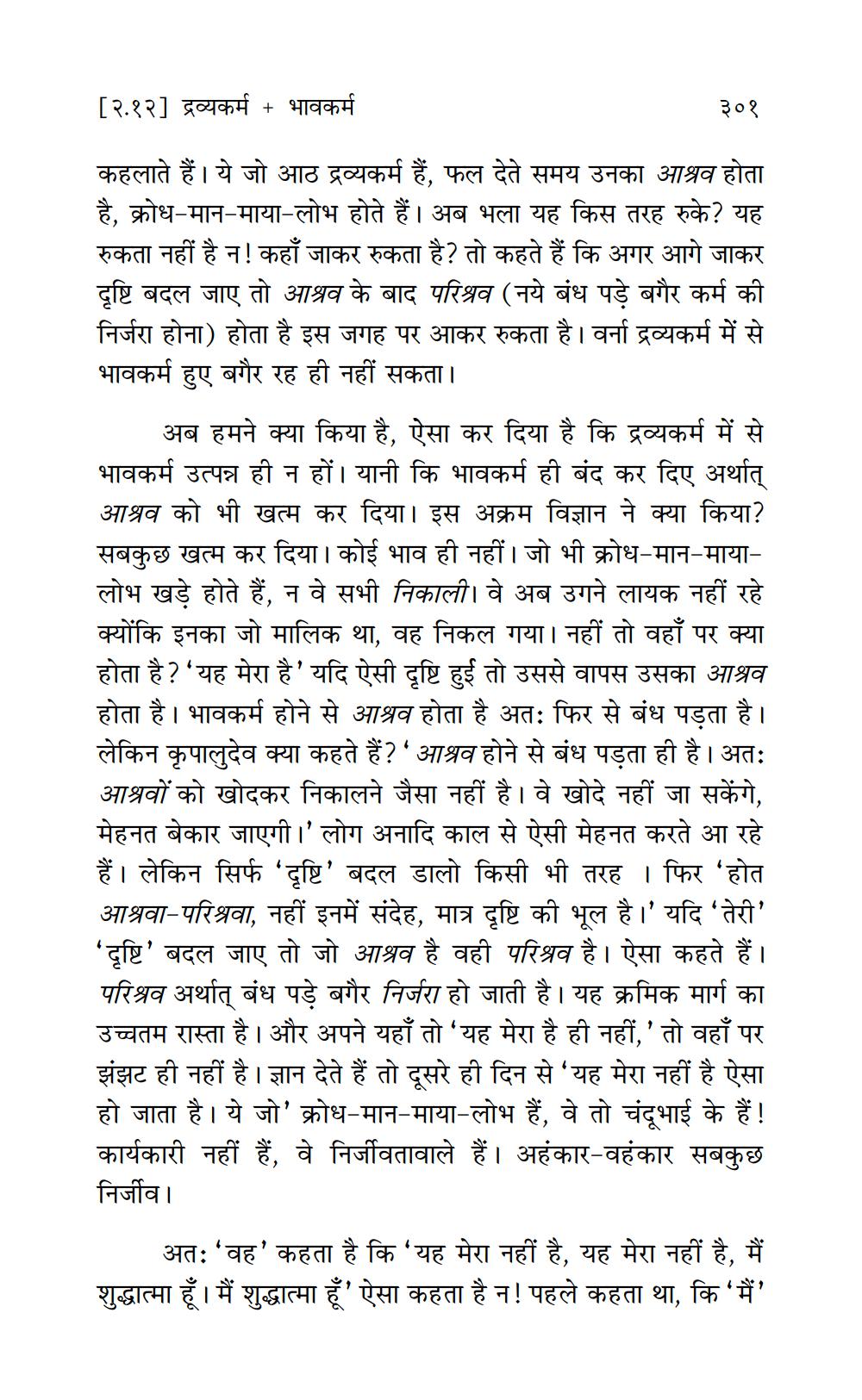________________
[२.१२] द्रव्यकर्म + भावकर्म
३०१
कहलाते हैं। ये जो आठ द्रव्यकर्म हैं, फल देते समय उनका आश्रव होता है, क्रोध-मान-माया-लोभ होते हैं। अब भला यह किस तरह रुके? यह रुकता नहीं है न! कहाँ जाकर रुकता है? तो कहते हैं कि अगर आगे जाकर दृष्टि बदल जाए तो आश्रव के बाद परिश्रव (नये बंध पड़े बगैर कर्म की निर्जरा होना) होता है इस जगह पर आकर रुकता है। वर्ना द्रव्यकर्म में से भावकर्म हुए बगैर रह ही नहीं सकता।
अब हमने क्या किया है, ऐसा कर दिया है कि द्रव्यकर्म में से भावकर्म उत्पन्न ही न हों। यानी कि भावकर्म ही बंद कर दिए अर्थात् आश्रव को भी खत्म कर दिया। इस अक्रम विज्ञान ने क्या किया? सबकुछ खत्म कर दिया। कोई भाव ही नहीं। जो भी क्रोध-मान-मायालोभ खडे होते हैं, न वे सभी निकाली। वे अब उगने लायक नहीं रहे क्योंकि इनका जो मालिक था, वह निकल गया। नहीं तो वहाँ पर क्या होता है? यह मेरा है' यदि ऐसी दृष्टि हुई तो उससे वापस उसका आश्रव होता है। भावकर्म होने से आश्रव होता है अतः फिर से बंध पड़ता है। लेकिन कृपालुदेव क्या कहते हैं? 'आश्रव होने से बंध पड़ता ही है। अतः आश्रवों को खोदकर निकालने जैसा नहीं है। वे खोदे नहीं जा सकेंगे, मेहनत बेकार जाएगी।' लोग अनादि काल से ऐसी मेहनत करते आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ 'दृष्टि' बदल डालो किसी भी तरह । फिर 'होत
आश्रवा-परिश्रवा, नहीं इनमें संदेह, मात्र दृष्टि की भूल है।' यदि 'तेरी' 'दृष्टि' बदल जाए तो जो आश्रव है वही परिश्रव है। ऐसा कहते हैं। परिश्रव अर्थात बंध पडे बगैर निर्जरा हो जाती है। यह क्रमिक मार्ग का उच्चतम रास्ता है। और अपने यहाँ तो 'यह मेरा है ही नहीं, तो वहाँ पर झंझट ही नहीं है। ज्ञान देते हैं तो दूसरे ही दिन से 'यह मेरा नहीं है ऐसा हो जाता है। ये जो' क्रोध-मान-माया-लोभ हैं, वे तो चंदूभाई के हैं! कार्यकारी नहीं हैं, वे निर्जीवतावाले हैं। अहंकार-वहंकार सबकुछ निर्जीव।
अतः 'वह' कहता है कि 'यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, मैं शुद्धात्मा हूँ। मैं शुद्धात्मा हूँ' ऐसा कहता है न! पहले कहता था, कि 'मैं'