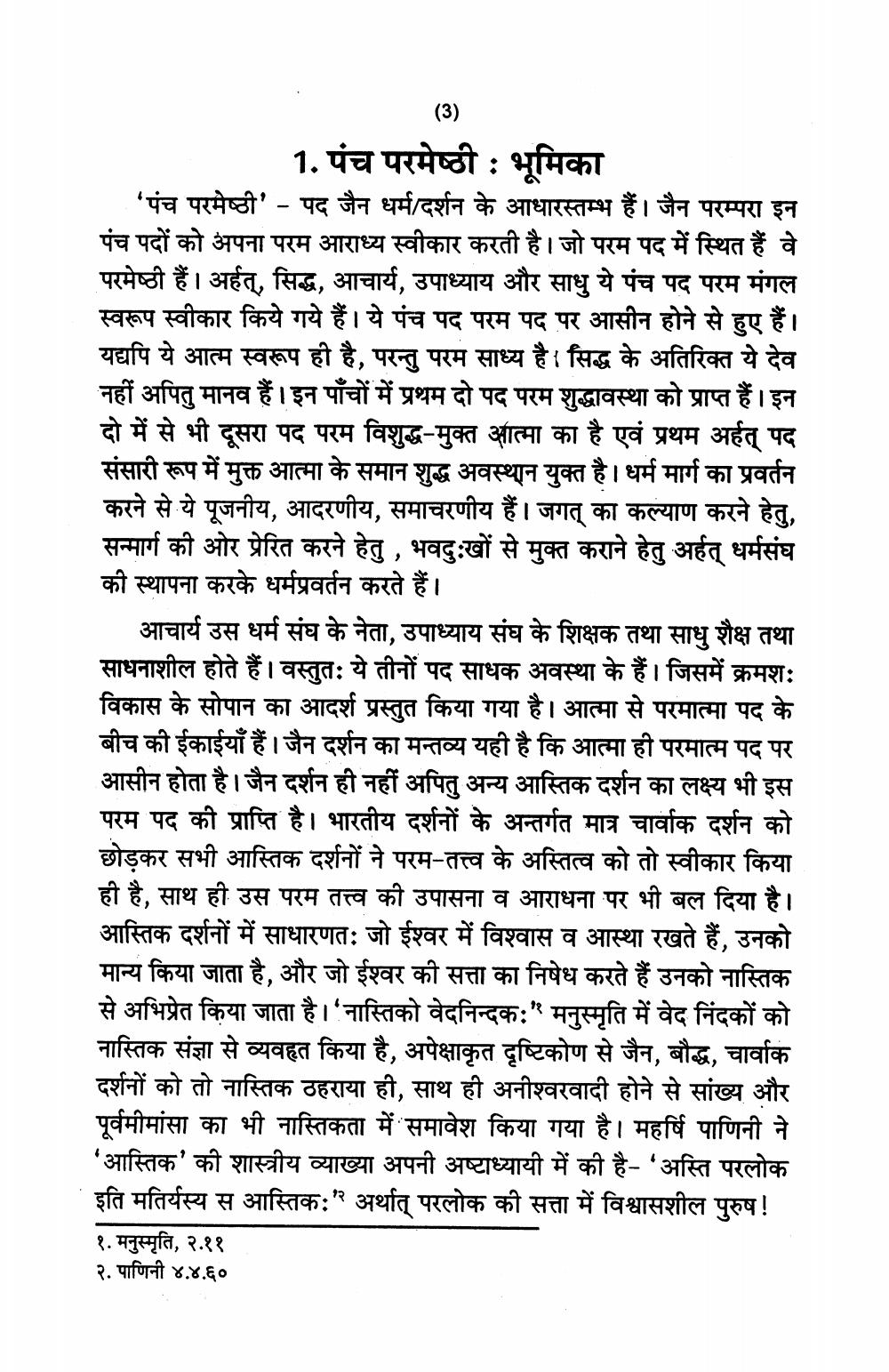________________ (3) 1. पंच परमेष्ठी : भूमिका 'पंच परमेष्ठी' - पद जैन धर्म/दर्शन के आधारस्तम्भ हैं। जैन परम्परा इन पंच पदों को अपना परम आराध्य स्वीकार करती है। जो परम पद में स्थित हैं वे परमेष्ठी हैं। अर्हत्, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये पंच पद परम मंगल स्वरूप स्वीकार किये गये हैं। ये पंच पद परम पद पर आसीन होने से हुए हैं। यद्यपि ये आत्म स्वरूप ही है, परन्तु परम साध्य है। सिद्ध के अतिरिक्त ये देव नहीं अपितु मानव हैं। इन पाँचों में प्रथम दो पद परम शुद्धावस्था को प्राप्त हैं। इन दो में से भी दूसरा पद परम विशुद्ध-मुक्त आत्मा का है एवं प्रथम अर्हत् पद संसारी रूप में मुक्त आत्मा के समान शुद्ध अवस्थान युक्त है। धर्म मार्ग का प्रवर्तन करने से ये पूजनीय, आदरणीय, समाचरणीय हैं। जगत् का कल्याण करने हेतु, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने हेतु , भवदुःखों से मुक्त कराने हेतु अर्हत् धर्मसंघ की स्थापना करके धर्मप्रवर्तन करते हैं। आचार्य उस धर्म संघ के नेता, उपाध्याय संघ के शिक्षक तथा साधु शैक्ष तथा साधनाशील होते हैं। वस्तुतः ये तीनों पद साधक अवस्था के हैं। जिसमें क्रमशः विकास के सोपान का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। आत्मा से परमात्मा पद के बीच की ईकाईयाँ हैं / जैन दर्शन का मन्तव्य यही है कि आत्मा ही परमात्म पद पर आसीन होता है। जैन दर्शन ही नहीं अपितु अन्य आस्तिक दर्शन का लक्ष्य भी इस परम पद की प्राप्ति है। भारतीय दर्शनों के अन्तर्गत मात्र चार्वाक दर्शन को छोड़कर सभी आस्तिक दर्शनों ने परम-तत्त्व के अस्तित्व को तो स्वीकार किया ही है, साथ ही उस परम तत्त्व की उपासना व आराधना पर भी बल दिया है। आस्तिक दर्शनों में साधारणतः जो ईश्वर में विश्वास व आस्था रखते हैं, उनको मान्य किया जाता है, और जो ईश्वर की सत्ता का निषेध करते हैं उनको नास्तिक से अभिप्रेत किया जाता है। 'नास्तिको वेदनिन्दकः' मनुस्मृति में वेद निंदकों को नास्तिक संज्ञा से व्यवहृत किया है, अपेक्षाकृत दृष्टिकोण से जैन, बौद्ध, चार्वाक दर्शनों को तो नास्तिक ठहराया ही, साथ ही अनीश्वरवादी होने से सांख्य और पूर्वमीमांसा का भी नास्तिकता में समावेश किया गया है। महर्षि पाणिनी ने 'आस्तिक' की शास्त्रीय व्याख्या अपनी अष्टाध्यायी में की है- 'अस्ति परलोक इति मतिर्यस्य स आस्तिक:२ अर्थात् परलोक की सत्ता में विश्वासशील पुरुष! 1. मनुस्मृति, 2.11 2. पाणिनी 4.4.60