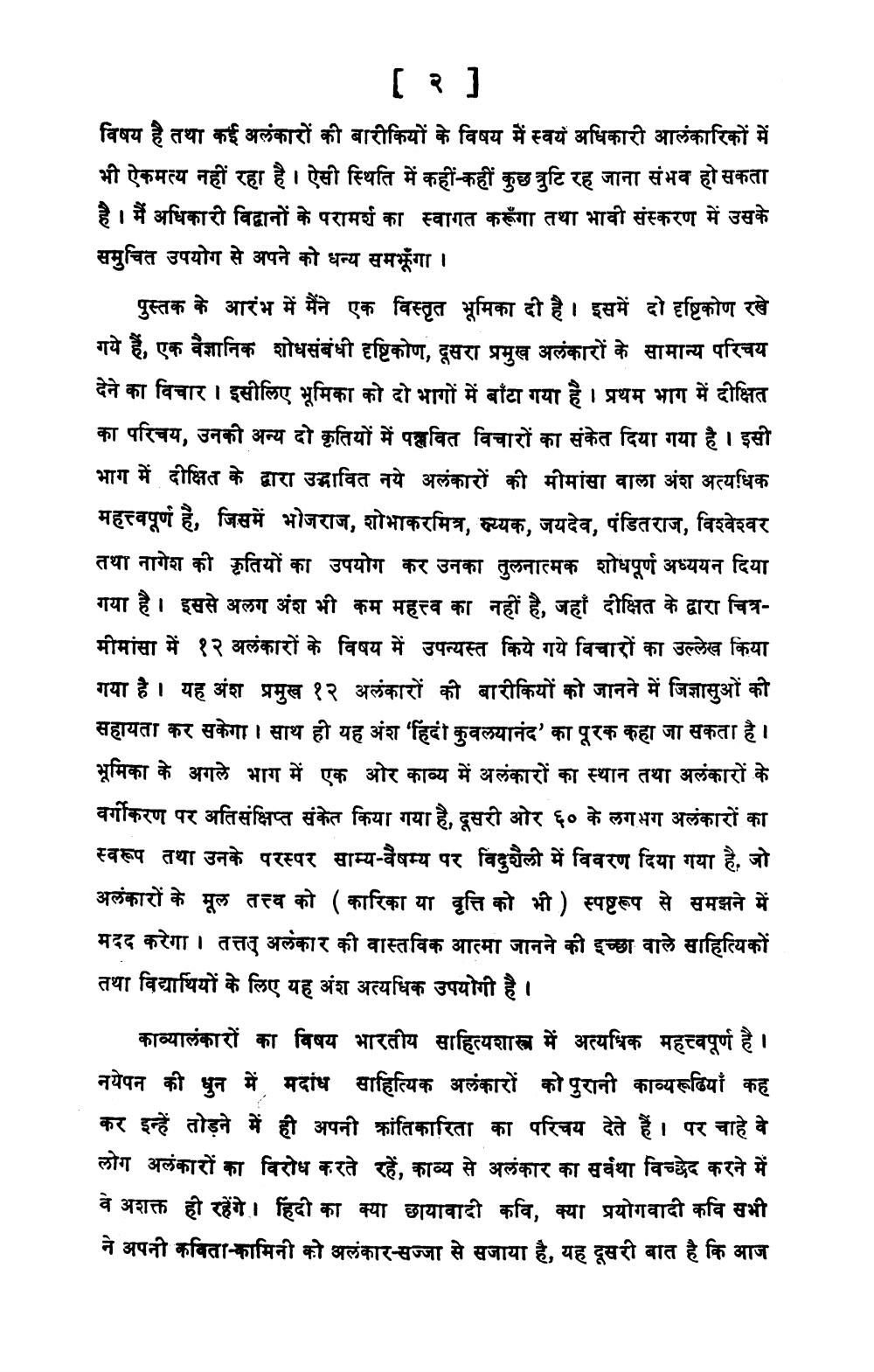________________
[ २ ]
विषय है तथा कई अलंकारों की बारीकियों के विषय में स्वयं अधिकारी आलंकारिकों में भी ऐकमत्य नहीं रहा है । ऐसी स्थिति में कहीं-कहीं कुछ त्रुटि रह जाना संभव हो सकता है । मैं अधिकारी विद्वानों के परामर्श का स्वागत करूँगा तथा भावी संस्करण में उसके समुचित उपयोग से अपने को धन्य समझँगा ।
पुस्तक के आरंभ में मैंने एक विस्तृत भूमिका दी है। इसमें दो दृष्टिकोण रखे गये हैं, एक वैज्ञानिक शोधसंबंधी दृष्टिकोण, दूसरा प्रमुख अलंकारों के सामान्य परिचय देने का विचार । इसीलिए भूमिका को दो भागों में बाँटा गया है। प्रथम भाग में दीक्षित का परिचय, उनकी अन्य दो कृतियों में पल्लवित विचारों का संकेत दिया गया है । इसी भाग में दीक्षित के द्वारा उद्भावित नये अलंकारों की मीमांसा वाला अंश अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, जिसमें भोजराज, शोभाकरमित्र, ख्य्यक, जयदेव, पंडितराज, विश्वेश्वर तथा नागेश की कृतियों का उपयोग कर उनका तुलनात्मक शोधपूर्ण अध्ययन दिया गया है। इससे अलग अंश भी कम महत्त्व का नहीं है, जहाँ दीक्षित के द्वारा चित्रमीमांसा में १२ अलंकारों के विषय में उपन्यस्त किये गये विचारों का उल्लेख किया गया है । यह अंश प्रमुख १२ अलंकारों की बारीकियों को जानने में जिज्ञासुओं की सहायता कर सकेगा। साथ ही यह अंश 'हिंदी कुवलयानंद' का पूरक कहा जा सकता है । भूमिका के अगले भाग में एक ओर काव्य में अलंकारों का स्थान तथा अलंकारों के वर्गीकरण पर अतिसंक्षिप्त संकेत किया गया है, दूसरी ओर ६० के लगभग अलंकारों का स्वरूप तथा उनके परस्पर साम्य वैषम्य पर विदुशैली में विवरण दिया गया है, जो अलंकारों के मूल तत्त्व को ( कारिका या वृत्ति को भी ) स्पष्टरूप से समझने में मदद करेगा । तत्तत् अलंकार की वास्तविक आत्मा जानने की इच्छा वाले साहित्यिकों तथा विद्यार्थियों के लिए यह अंश अत्यधिक उपयोगी है ।
काव्यालंकारों का विषय भारतीय साहित्यशास्त्र में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । नयेपन की धुन में मदांध साहित्यिक अलंकारों को पुरानी काव्यरूढियाँ कह कर इन्हें तोड़ने में ही अपनी क्रांतिकारिता का परिचय देते हैं। पर चाहे वे लोग अलंकारों का विरोध करते रहें, काव्य से अलंकार का सर्वथा विच्छेद करने में वे अशक्त ही रहेंगे। हिंदी का क्या छायावादी कवि, क्या प्रयोगवादी कवि सभी ने अपनी कविता- कामिनी को अलंकार-सज्जा से सजाया है, यह दूसरी बात है कि आज