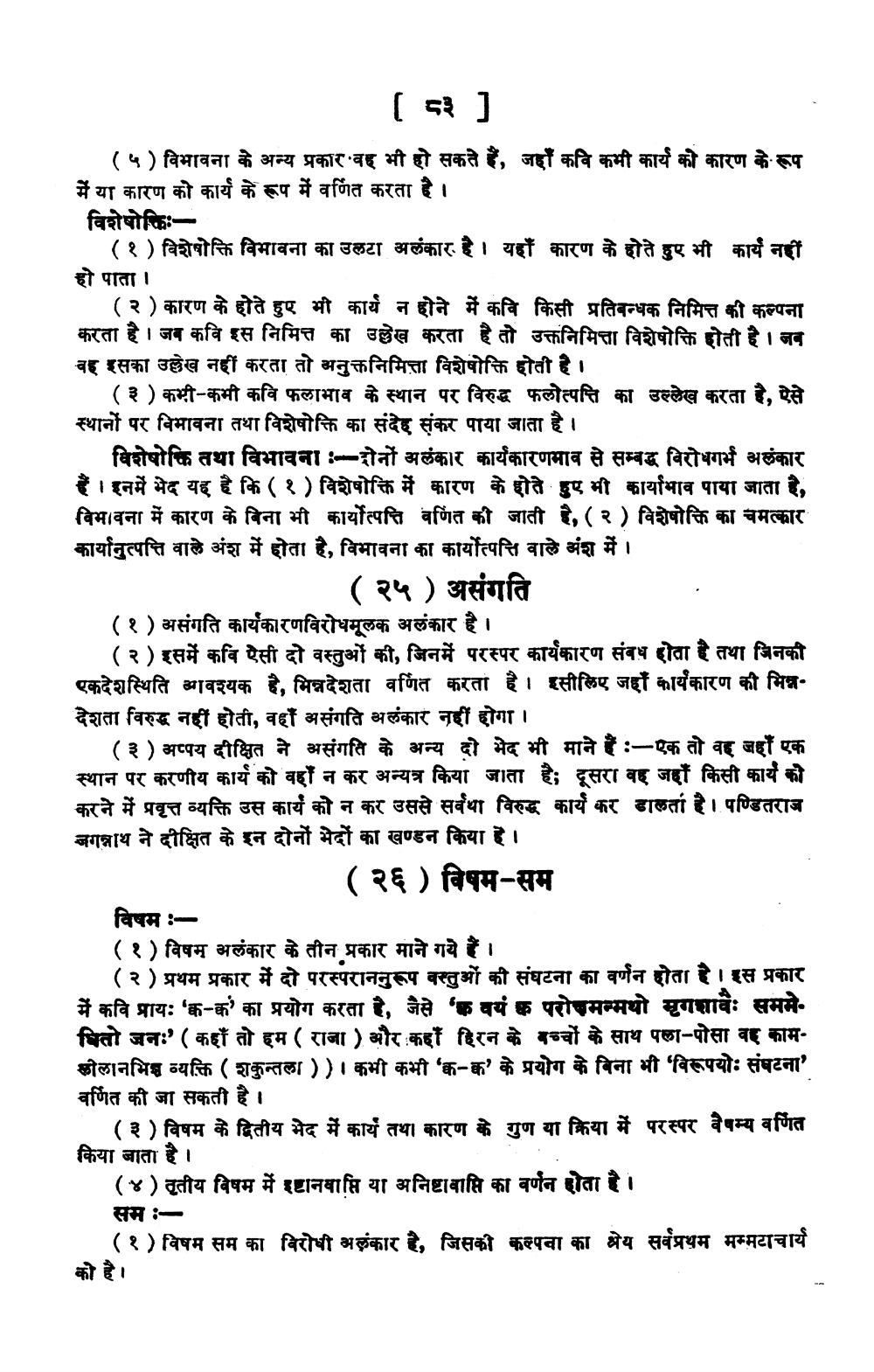________________
[ ६३ ]
(५) विभावना के अन्य प्रकार वह भी हो सकते हैं, जहाँ कवि कभी कार्य को कारण के रूप या कारण को कार्य के रूप में वर्णित करता है ।
विशेषोक्तिः
( १ ) विशेषोक्ति विभावना का उलटा अलंकार है । यहाँ कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हो पाता ।
( २ ) कारण के होते हुए भी कार्य न होने में कवि किसी प्रतिबन्धक निमित्त की कल्पना करता है । जब कवि इस निमित्त का उल्लेख करता है तो उक्तनिमित्ता विशेषोक्ति होती है । जब वह इसका उल्लेख नहीं करता तो अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति होती है ।
( ३ ) कभी-कभी कवि फलाभाव के स्थान पर विरुद्ध फलोत्पत्ति का उल्लेख करता है, ऐसे स्थानों पर विभावना तथा विशेषोक्ति का संदेह संकर पाया जाता है ।
विशेषोति तथा विभावना :-- दोनों अलंकार कार्यकारणभाव से सम्बद्ध विरोधगर्भ अलंकार हैं। इनमें भेद यह है कि ( १ ) विशेषोक्ति में कारण के होते हुए भी कार्याभाव पाया जाता है, विभावना में कारण के बिना भी कार्योत्पत्ति वर्णित की जाती है, ( २ ) विशेषोक्ति का चमत्कार कार्यानुत्पत्ति वाले अंश में होता है, विभावना का कार्योत्पत्ति वाले अंश में ।
(२५) असंगति
( १ ) असंगति कार्यकारणविरोधमूलक अलंकार है ।
( २ ) इसमें कवि ऐसी दो वस्तुओं की, जिनमें परस्पर कार्यकारण संबंध होता है तथा जिनकी एकदेशस्थिति आवश्यक है, मिन्नदेशता वर्णित करता है । इसीलिए जहाँ कार्यकारण की भिन्नदेशता विरुद्ध नहीं होती, वहाँ असंगति अलंकार नहीं होगा ।
(३) अप्पय दीक्षित ने असंगति के अन्य दो भेद भी माने हैं :- एक तो वह जहाँ एक स्थान पर करणीय कार्य को वहाँ न कर अन्यत्र किया जाता है; दूसरा वह जहाँ किसी कार्य को करने में प्रवृत्त व्यक्ति उस कार्य को न कर उससे सर्वथा विरुद्ध कार्य कर डालता है। पण्डितराज जगन्नाथ ने दीक्षित के इन दोनों भेदों का खण्डन किया है।
(२६) विषम- सम
विषम :
( १ ) विषम अलंकार के तीन प्रकार माने गये हैं ।
(२) प्रथम प्रकार में दो परस्पराननुरूप वस्तुओं की संघटना का वर्णन होता है। इस प्रकार कवि प्रायः 'क्क - क्क' का प्रयोग करता है, जैसे 'व वयं व परोचमन्मथो मृगशावैः सममेधितो जनः' ( कहाँ तो हम ( राजा ) और कहाँ हिरन के बच्चों के साथ पला-पोसा वह कामकीलानभित्र व्यक्ति ( शकुन्तला ) ) | कभी कभी 'क-क' के प्रयोग के बिना भी 'विरूपयोः संघटना' वर्णित की जा सकती है ।
(३) विषम के द्वितीय भेद में कार्य तथा कारण के गुण या क्रिया में परस्पर वैषम्य वर्णित किया जाता है ।
( ४ ) तृतीय विषम में इष्टानवाप्ति या अनिष्टावाप्ति का वर्णन होता है ।
सम :
( १ ) विषम सम का विरोधी अलंकार है, जिसकी कल्पना का श्रेय सर्वप्रथम मम्मटाचार्य
को है ।