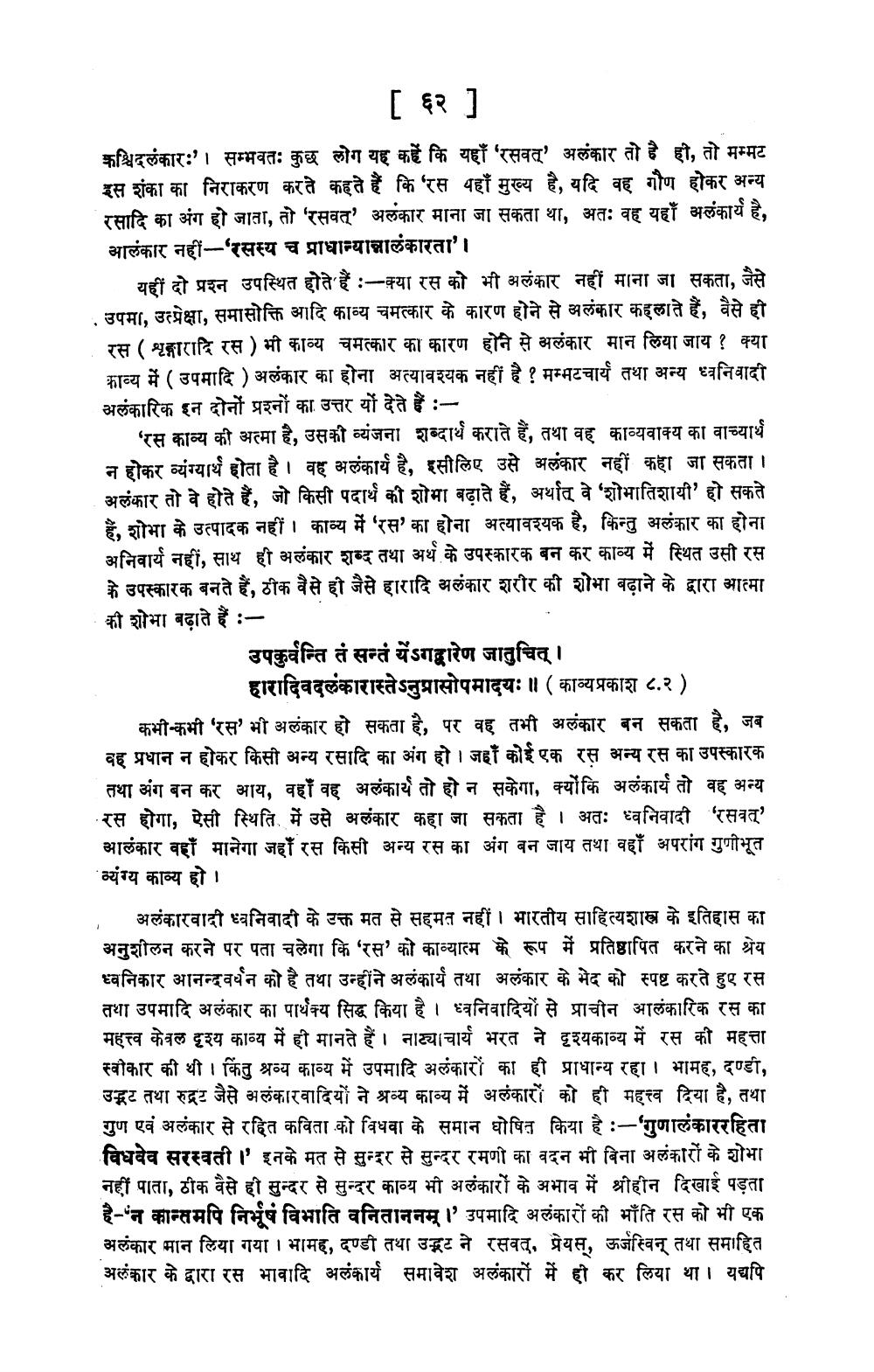________________
[ ६२ ] कश्चिदलंकारः'। सम्भवतः कुछ लोग यह कहें कि यहाँ 'रसवत्' अलंकार तो है हो, तो मम्मट इस शंका का निराकरण करते कहते हैं कि 'रस यहाँ मुख्य है, यदि वह गौण होकर अन्य रसादि का अंग हो जाता, तो 'रसवत्' अलंकार माना जा सकता था, अतः वह यहाँ अलंकार्य है, आलंकार नहीं-'रसस्य च प्राधान्यानालंकारता'।
यहीं दो प्रश्न उपस्थित होते हैं :-क्या रस को भी अलंकार नहीं माना जा सकता, जैसे . उपमा, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति आदि काव्य चमत्कार के कारण होने से अलंकार कहलाते हैं, वैसे ही रस (शृङ्गारादि रस) भी काव्य चमत्कार का कारण होने से अलंकार मान लिया जाय ? क्या काव्य में ( उपमादि ) अलंकार का होना अत्यावश्यक नहीं है ? मम्मटचार्य तथा अन्य ध्वनिवादी अलंकारिक इन दोनों प्रश्नों का उत्तर यों देते हैं :
'रस काव्य की अत्मा है, उसकी व्यंजना शब्दार्थ कराते हैं, तथा वह काव्यवाक्य का वाच्यार्थ न होकर व्यंग्यार्थ होता है। वह अलंकार्य है, इसीलिए उसे अलंकार नहीं कहा जा सकता। अलंकार तो वे होते हैं, जो किसी पदार्थ की शोभा बढ़ाते हैं, अर्थात् वे 'शोभातिशायी' हो सकते हैं, शोभा के उत्पादक नहीं। काव्य में 'रस' का होना अत्यावश्यक है, किन्तु अलंकार का होना अनिवार्य नहीं, साथ ही अलंकार शब्द तथा अर्थ के उपस्कारक बन कर काव्य में स्थित उसी रस के उपस्कारक बनते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हारादि अलंकार शरीर की शोभा बढ़ाने के द्वारा आत्मा की शोभा बढ़ाते हैं :
उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽगद्वारेण जातुचित् ।
हारादिवदलंकारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ ( काव्यप्रकाश ८.२ ) कभी-कभी 'रस' भी अलंकार हो सकता है, पर वह तभी अलंकार बन सकता है, जब वह प्रधान न होकर किसी अन्य रसादि का अंग हो । जहाँ कोई एक रस अन्य रस का उपस्कारक तथा अंग बन कर आय, वहाँ वह अलंकार्य तो हो न सकेगा, क्योंकि अलंकार्य तो वह अन्य रस होगा, ऐसी स्थिति में उसे अलंकार कहा जा सकता है । अतः ध्वनिवादी 'रसवत्' आलंकार वहाँ मानेगा जहाँ रस किसी अन्य रस का अंग बन जाय तथा वहाँ अपरांग गुणीभूत व्यंग्य काव्य हो। __ अलंकारवादी ध्वनिवादी के उक्त मत से सहमत नहीं। भारतीय साहित्यशास्त्र के इतिहास का अनुशीलन करने पर पता चलेगा कि 'रस' को काव्यात्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने का श्रेय ध्वनिकार आनन्दवर्धन को है तथा उन्हींने अलंकार्य तथा अलंकार के भेद को स्पष्ट करते हुए रस तथा उपमादि अलंकार का पार्थक्य सिद्ध किया है । ध्वनिवादियों से प्राचीन आलंकारिक रस का महत्त्व केवल दृश्य काव्य में ही मानते हैं। नाट्याचार्य भरत ने दृश्यकाव्य में रस की महत्ता स्वीकार की थी। किंतु श्रव्य काव्य में उपमादि अलंकारों का ही प्राधान्य रहा। भामह, दण्डी, उद्भट तथा रुद्रट जैसे अलंकारवादियों ने श्रव्य काव्य में अलंकारों को ही महत्त्व दिया है, तथा गुण एवं अलंकार से रहित कविता को विधवा के समान घोषित किया है :-गुणालंकाररहिता विधवेव सरस्वती।' इनके मत से सुन्दर से सुन्दर रमणी का वदन भी बिना अलंकारों के शोभा नहीं पाता, ठीक वैसे ही सुन्दर से सुन्दर काव्य भी अलंकारों के अभाव में श्रीहीन दिखाई पड़ता है-'न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम् ।' उपमादि अलंकारों की भाँति रस को भी एक अलंकार मान लिया गया । भामह, दण्डी तथा उद्भट ने रसवत्, प्रेयस, ऊर्जस्विन् तथा समाहित अलंकार के द्वारा रस भावादि अलंकार्य समावेश अलंकारों में ही कर लिया था। यद्यपि