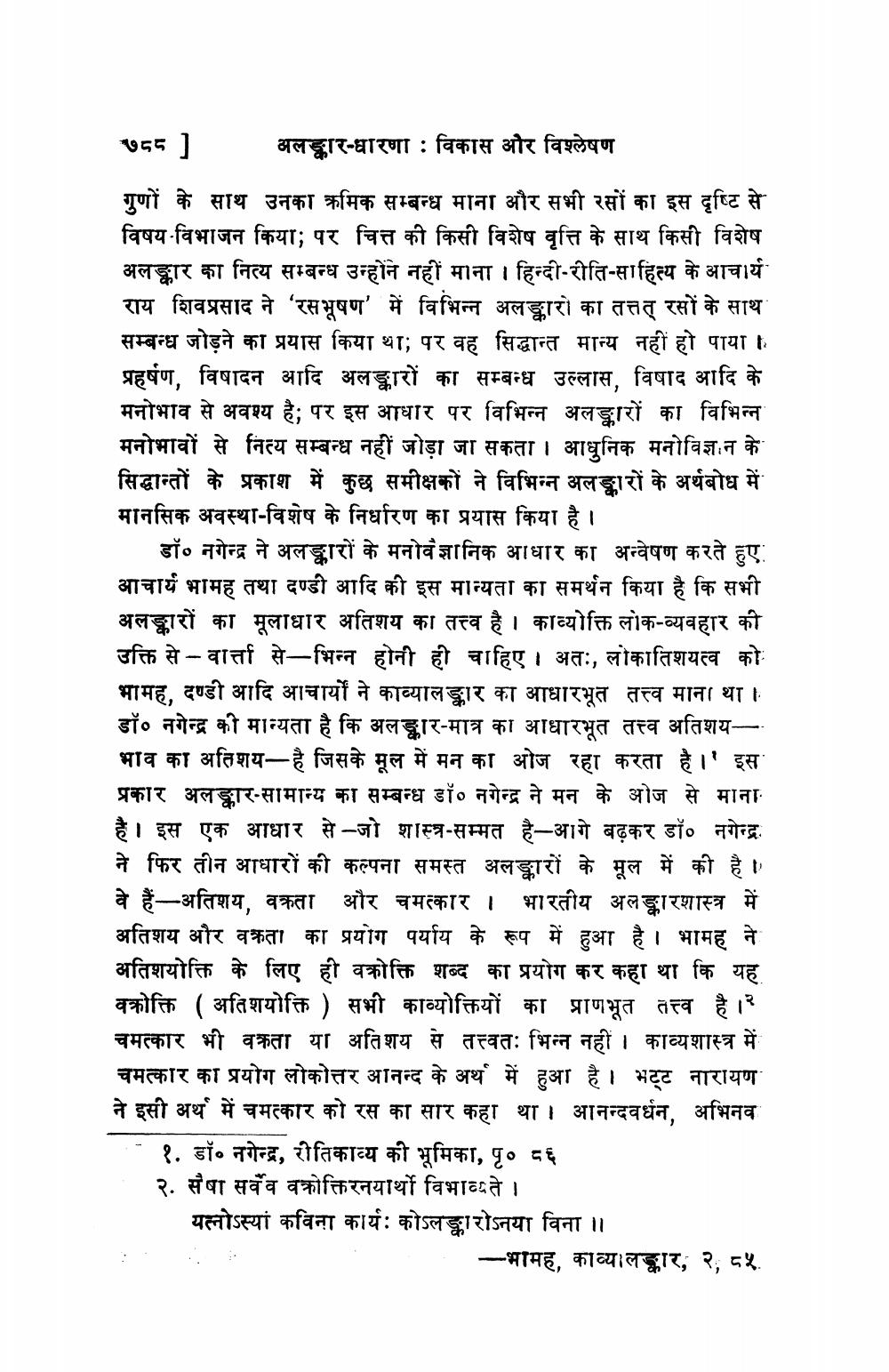________________
७८८ ] अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण गुणों के साथ उनका क्रमिक सम्बन्ध माना और सभी रसों का इस दृष्टि से विषय विभाजन किया; पर चित्त की किसी विशेष वृत्ति के साथ किसी विशेष अलङ्कार का नित्य सम्बन्ध उन्होंने नहीं माना । हिन्दी-रीति-साहित्य के आचार्य राय शिवप्रसाद ने 'रसभूषण' में विभिन्न अलङ्कारो का तत्तत् रसों के साथ सम्बन्ध जोड़ने का प्रयास किया था; पर वह सिद्धान्त मान्य नहीं हो पाया । प्रहर्षण, विषादन आदि अलङ्कारों का सम्बन्ध उल्लास, विषाद आदि के मनोभाव से अवश्य है; पर इस आधार पर विभिन्न अलङ्कारों का विभिन्न मनोभावों से नित्य सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता। आधुनिक मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के प्रकाश में कुछ समीक्षकों ने विभिन्न अलङ्कारों के अर्थबोध में मानसिक अवस्था-विशेष के निर्धारण का प्रयास किया है। __ डॉ० नगेन्द्र ने अलङ्कारों के मनोवैज्ञानिक आधार का अन्वेषण करते हुए आचार्य भामह तथा दण्डी आदि की इस मान्यता का समर्थन किया है कि सभी अलङ्कारों का मूलाधार अतिशय का तत्त्व है । काव्योक्ति लोक-व्यवहार की उक्ति से - वार्ता से-भिन्न होनी ही चाहिए। अतः, लोकातिशयत्व को भामह, दण्डी आदि आचार्यों ने काव्यालङ्कार का आधारभूत तत्त्व माना था। डॉ० नगेन्द्र की मान्यता है कि अलङ्कार-मात्र का आधारभूत तत्त्व अतिशयभाव का अतिशय-है जिसके मूल में मन का ओज रहा करता है।' इस प्रकार अलङ्कार-सामान्य का सम्बन्ध डॉ० नगेन्द्र ने मन के ओज से माना है। इस एक आधार से -जो शास्त्र-सम्मत है-आगे बढ़कर डॉ० नगेन्द्र. ने फिर तीन आधारों की कल्पना समस्त अलङ्कारों के मूल में की है। वे हैं-अतिशय, वक्रता और चमत्कार । भारतीय अलङ्कारशास्त्र में अतिशय और वक्रता का प्रयोग पर्याय के रूप में हुआ है। भामह ने अतिशयोक्ति के लिए ही वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग कर कहा था कि यह वक्रोक्ति ( अतिशयोक्ति ) सभी काव्योक्तियों का प्राणभूत तत्त्व है। चमत्कार भी वक्रता या अतिशय से तत्त्वतः भिन्न नहीं। काव्यशास्त्र में चमत्कार का प्रयोग लोकोत्तर आनन्द के अर्थ में हुआ है। भट्ट नारायण ने इसी अर्थ में चमत्कार को रस का सार कहा था। आनन्दवर्धन, अभिनव - १. डॉ. नगेन्द्र, रीतिकाव्य की भूमिका, पृ० ८६ २. सैषा सर्वव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते । __ यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया विना ॥
-भामह, काव्यालङ्कार, २, ८५.