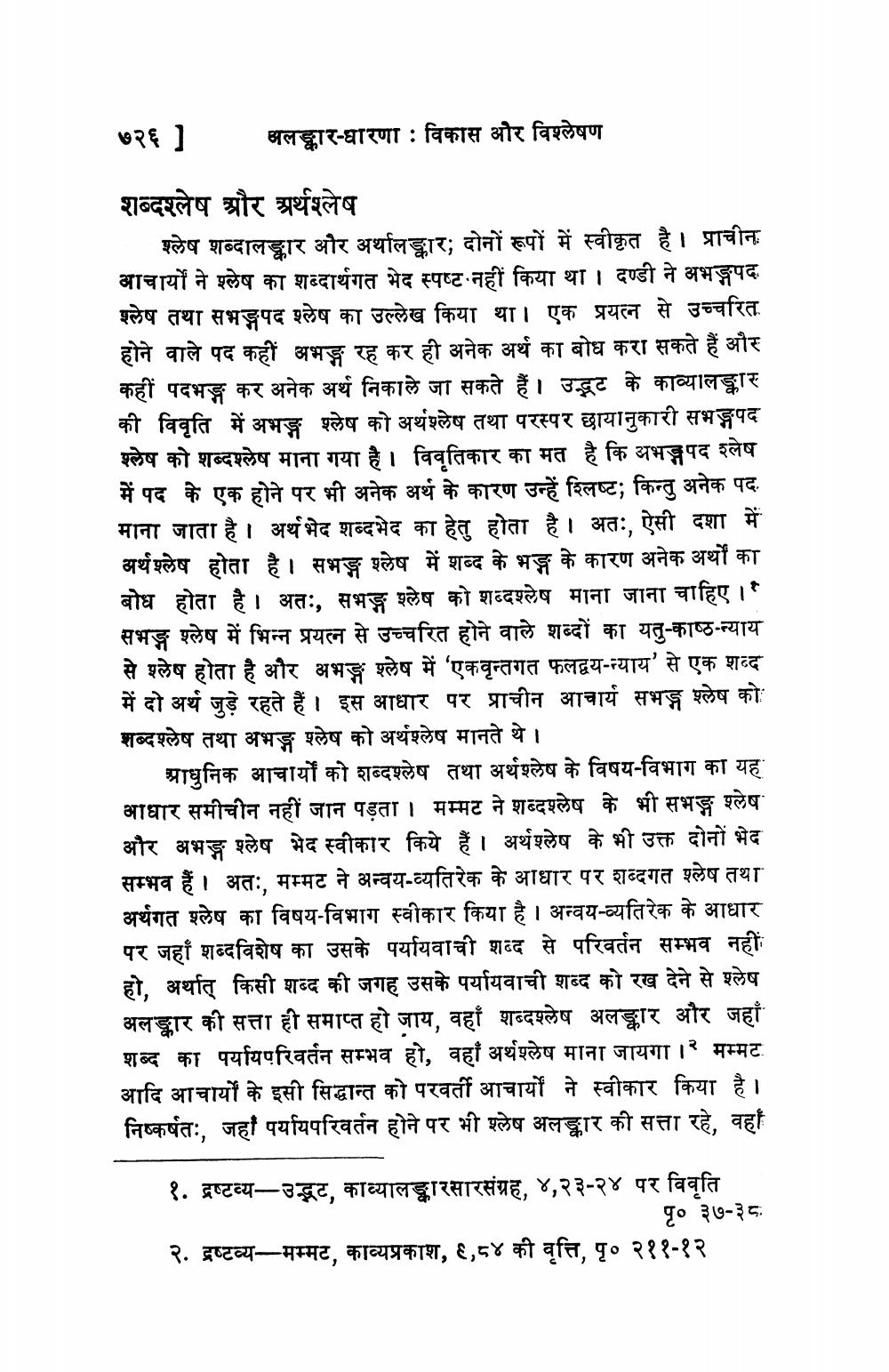________________
७२६ ]
शब्दश्लेष और अर्थश्लेष
श्लेष शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार; दोनों रूपों में स्वीकृत है । प्राचीन आचार्यों ने श्लेष का शब्दार्थगत भेद स्पष्ट नहीं किया था । दण्डी ने अभङ्गपद श्लेष तथा सभङ्गपद श्लेष का उल्लेख किया था। एक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले पद कहीं अभङ्ग रह कर ही अनेक अर्थ का बोध करा सकते हैं और कहीं पदभङ्ग कर अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं । उद्भट के काव्यालङ्कार की विवृति में अभङ्ग श्लेष को अर्थश्लेष तथा परस्पर छायानुकारी सभङ्गपद श्लेष को शब्दश्लेष माना गया है । विवृतिकार का मत है कि अभङ्गपद श्लेष में पद के एक होने पर भी अनेक अर्थ के कारण उन्हें श्लिष्ट; किन्तु अनेक पद माना जाता है । अर्थ भेद शब्दभेद का हेतु होता है । अतः ऐसी दशा में अर्थ श्लेष होता है । सभङ्ग श्लेष में शब्द के भङ्ग के कारण अनेक अर्थों का बोध होता है । अतः सभङ्ग श्लेष को शब्दश्लेष माना जाना चाहिए। सभङ्ग श्लेष में भिन्न प्रयत्न से उच्चरित होने वाले शब्दों का यतु- काष्ठ-न्याय से श्लेष होता है और अभङ्ग श्लेष में 'एकवृन्तगत फलद्वय-न्याय' से एक शब्द में दो अर्थ जुड़े रहते हैं । इस आधार पर प्राचीन आचार्य सभङ्ग श्लेष को शब्दश्लेष तथा अभङ्ग श्लेष को अर्थश्लेष मानते थे ।
1
"
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
आधुनिक आचार्यों को शब्दश्लेष तथा अर्थश्लेष के विषय विभाग का यह आधार समीचीन नहीं जान पड़ता । मम्मट ने शब्दश्लेष के भी सभङ्ग श्लेष और अभङ्ग श्लेष भेद स्वीकार किये हैं । अर्थश्लेष के भी उक्त दोनों भेद सम्भव हैं । अतः, मम्मट ने अन्वयव्यतिरेक के आधार पर शब्दगत श्लेष तथा अर्थगत श्लेष का विषय विभाग स्वीकार किया है । अन्वयव्यतिरेक के आधार पर जहाँ शब्दविशेष का उसके पर्यायवाची शब्द से परिवर्तन सम्भव नहीं हो, अर्थात् किसी शब्द की जगह उसके पर्यायवाची शब्द को रख देने से श्लेष अलङ्कार की सत्ता ही समाप्त हो जाय, वहाँ शब्दश्लेष अलङ्कार और जहाँ शब्द का पर्यायपरिवर्तन सम्भव हो, वहाँ अर्थश्लेष माना जायगा । मम्मट आदि आचार्यों के इसी सिद्धान्त को परवर्ती आचार्यों ने स्वीकार किया है । निष्कर्षतः, जहाँ पर्यायपरिवर्तन होने पर भी श्लेष अलङ्कार की सत्ता रहे, वहाँ
१. द्रष्टव्य — उद्भट, काव्यालङ्कारसारसंग्रह, ४, २३-२४ पर विवृति पृ० ३७-३८.
२. द्रष्टव्य - मम्मट, काव्यप्रकाश, ६, ८४ की वृत्ति, पृ० २११-१२