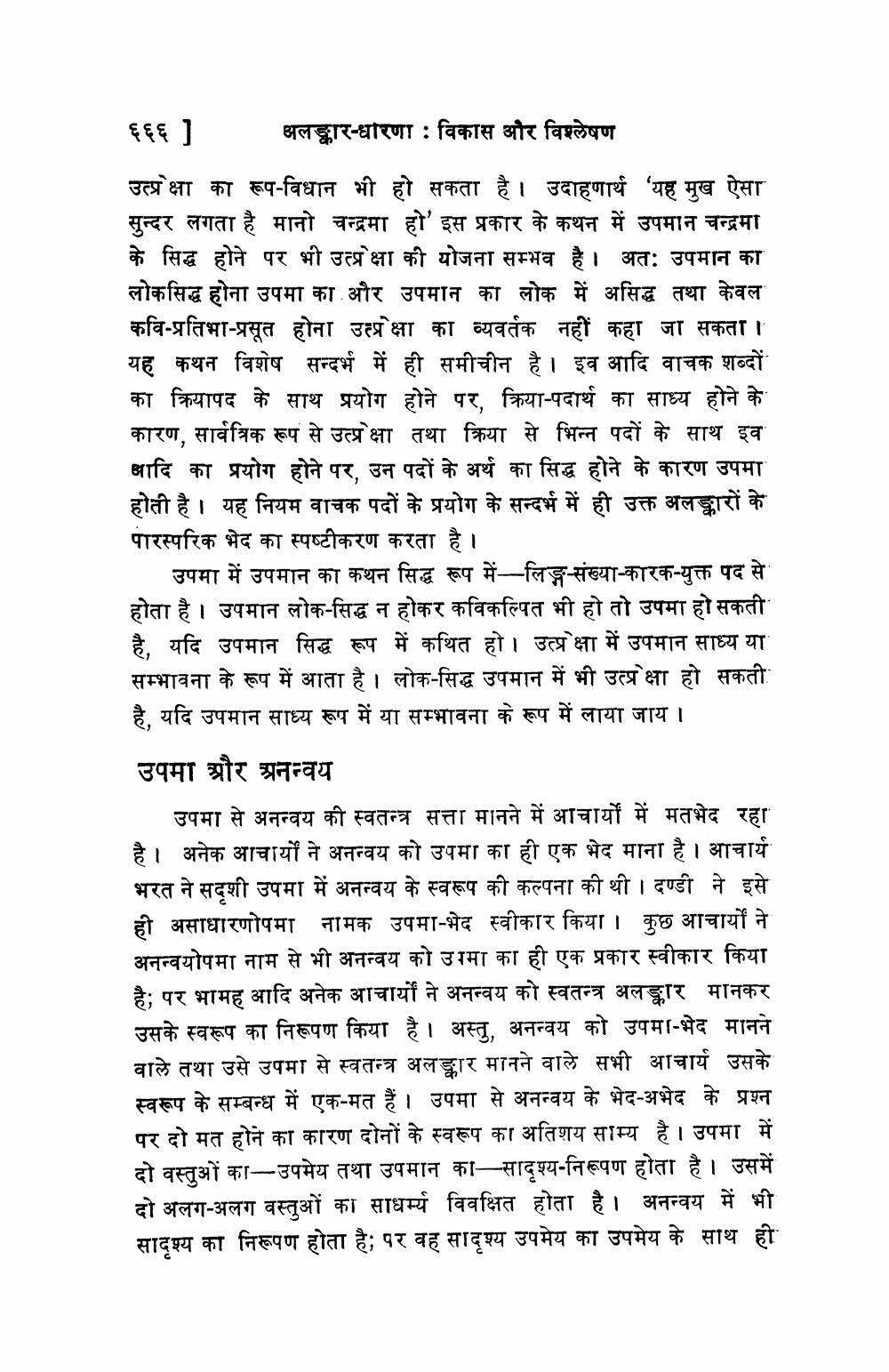________________
६६६ ] अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण उत्प्रेक्षा का रूप-विधान भी हो सकता है। उदाहणार्थ 'यह मुख ऐसा सुन्दर लगता है मानो चन्द्रमा हो' इस प्रकार के कथन में उपमान चन्द्रमा के सिद्ध होने पर भी उत्प्रेक्षा की योजना सम्भव है। अत: उपमान का लोकसिद्ध होना उपमा का और उपमान का लोक में असिद्ध तथा केवल कवि-प्रतिभा-प्रसूत होना उत्प्रेक्षा का व्यवर्तक नहीं कहा जा सकता। यह कथन विशेष सन्दर्भ में ही समीचीन है। इव आदि वाचक शब्दों का क्रियापद के साथ प्रयोग होने पर, क्रिया-पदार्थ का साध्य होने के कारण, सार्वत्रिक रूप से उत्प्रेक्षा तथा क्रिया से भिन्न पदों के साथ इव आदि का प्रयोग होने पर, उन पदों के अर्थ का सिद्ध होने के कारण उपमा होती है। यह नियम वाचक पदों के प्रयोग के सन्दर्भ में ही उक्त अलङ्कारों के पारस्परिक भेद का स्पष्टीकरण करता है।
उपमा उपमान का कथन सिद्ध रूप में-लिङ्ग-संख्या-कारक-युक्त पद से होता है। उपमान लोक-सिद्ध न होकर कविकल्पित भी हो तो उपमा हो सकती है, यदि उपमान सिद्ध रूप में कथित हो। उत्प्रेक्षा में उपमान साध्य या सम्भावना के रूप में आता है। लोक-सिद्ध उपमान में भी उत्प्रेक्षा हो सकती है, यदि उपमान साध्य रूप में या सम्भावना के रूप में लाया जाय । उपमा और अनन्वय
उपमा से अनन्वय की स्वतन्त्र सत्ता मानने में आचार्यों में मतभेद रहा है। अनेक आचार्यों ने अनन्वय को उपमा का ही एक भेद माना है। आचार्य भरत ने सदृशी उपमा में अनन्वय के स्वरूप की कल्पना की थी । दण्डी ने इसे ही असाधारणोपमा नामक उपमा-भेद स्वीकार किया। कुछ आचार्यों ने अनन्वयोपमा नाम से भी अनन्वय को उपमा का ही एक प्रकार स्वीकार किया है; पर भामह आदि अनेक आचार्यों ने अनन्वय को स्वतन्त्र अलङ्कार मानकर उसके स्वरूप का निरूपण किया है। अस्तु, अनन्वय को उपमा-भेद मानने वाले तथा उसे उपमा से स्वतन्त्र अलङ्कार मानने वाले सभी आचार्य उसके स्वरूप के सम्बन्ध में एक-मत हैं। उपमा से अनन्वय के भेद-अभेद के प्रश्न पर दो मत होने का कारण दोनों के स्वरूप का अतिशय साम्य है। उपमा में दो वस्तुओं का-उपमेय तथा उपमान का-सादृश्य-निरूपण होता है। उसमें दो अलग-अलग वस्तुओं का साधर्म्य विवक्षित होता है। अनन्वय में भी सादृश्य का निरूपण होता है; पर वह सादृश्य उपमेय का उपमेय के साथ ही