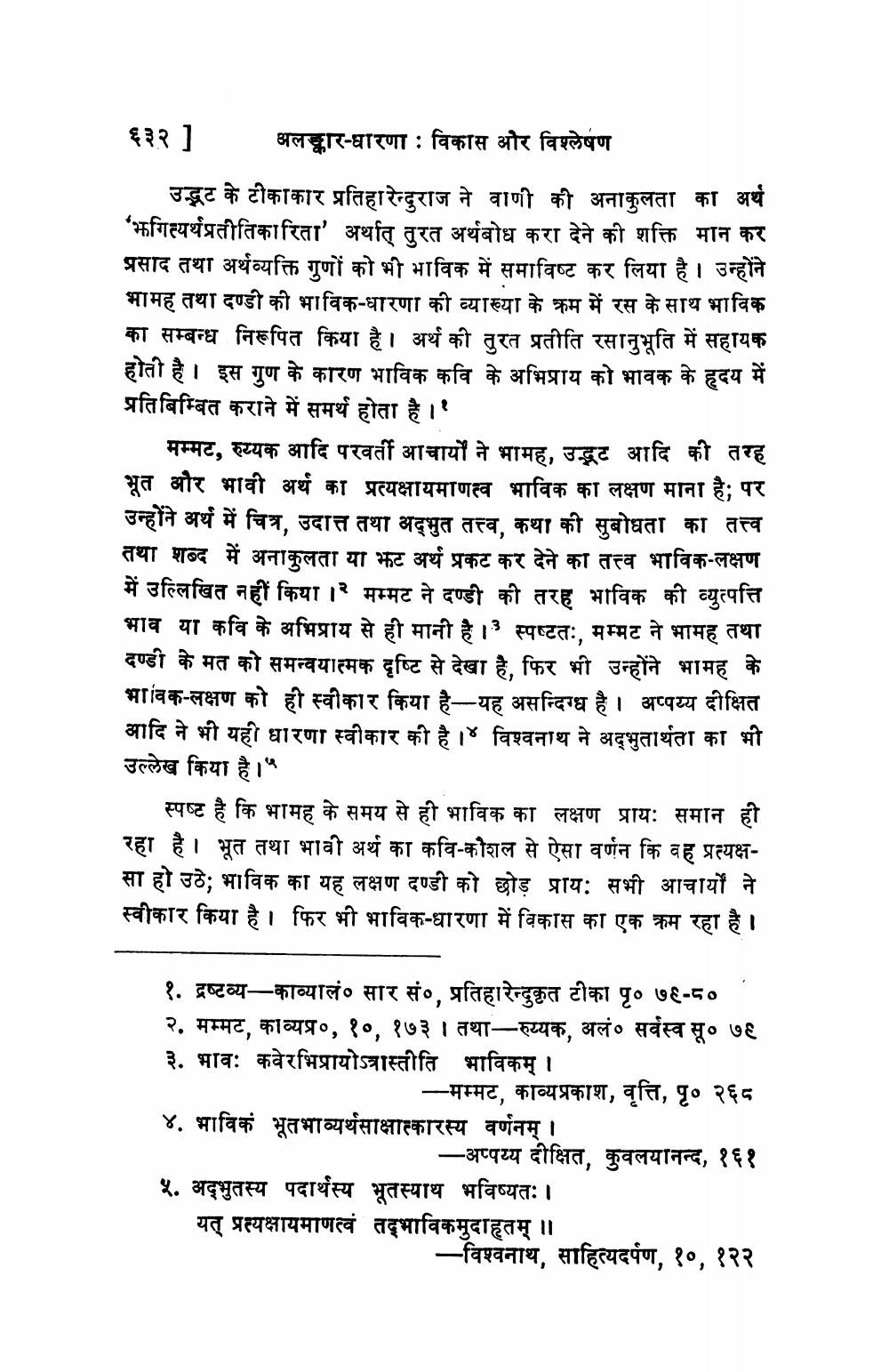________________
६३२ ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
उद्भट के टीकाकार प्रतिहारेन्दुराज ने वाणी की अनाकुलता का अर्थ 'झगित्यर्थप्रतीतिकारिता' अर्थात् तुरत अर्थबोध करा देने की शक्ति मान कर प्रसाद तथा अर्थव्यक्ति गुणों को भी भाविक में समाविष्ट कर लिया है। उन्होंने भामह तथा दण्डी की भाविक-धारणा की व्याख्या के क्रम में रस के साथ भाविक का सम्बन्ध निरूपित किया है। अर्थ की तुरत प्रतीति रसानुभूति में सहायक होती है। इस गुण के कारण भाविक कवि के अभिप्राय को भावक के हृदय में प्रतिबिम्बित कराने में समर्थ होता है।'
मम्मट, रुय्यक आदि परवर्ती आचार्यों ने भामह, उद्भट आदि की तरह भूत और भावी अर्थ का प्रत्यक्षायमाणत्व भाविक का लक्षण माना है; पर उन्होंने अर्थ में चित्र, उदात्त तथा अद्भुत तत्त्व, कथा की सुबोधता का तत्त्व तथा शब्द में अनाकुलता या झट अर्थ प्रकट कर देने का तत्त्व भाविक-लक्षण में उल्लिखित नहीं किया ।२ मम्मट ने दण्डी की तरह भाविक की व्युत्पत्ति भाव या कवि के अभिप्राय से ही मानी है। स्पष्टतः, मम्मट ने भामह तथा दण्डी के मत को समन्वयात्मक दृष्टि से देखा है, फिर भी उन्होंने भामह के भाविक-लक्षण को ही स्वीकार किया है-यह असन्दिग्ध है। अप्पय्य दीक्षित आदि ने भी यही धारणा स्वीकार की है। विश्वनाथ ने अद्भुतार्थता का भी उल्लेख किया है।
स्पष्ट है कि भामह के समय से ही भाविक का लक्षण प्रायः समान ही रहा है। भूत तथा भावी अर्थ का कवि-कौशल से ऐसा वर्णन कि वह प्रत्यक्षसा हो उठे; भाविक का यह लक्षण दण्डी को छोड़ प्रायः सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। फिर भी भाविक-धारणा में विकास का एक क्रम रहा है।
१. द्रष्टव्य-काव्यालं० सार सं०, प्रतिहारेन्दुकृत टीका पृ० ७९-८० । २. मम्मट, काव्यप्र०, १०, १७३ । तथा-रुय्यक, अलं० सर्वस्व सू० ७६ ३. भावः कवेरभिप्रायोऽत्रास्तीति भाविकम् ।
-मम्मट, काव्यप्रकाश, वृत्ति, पृ० २६८ ४. भाविक भूतभाव्यर्थसाक्षात्कारस्य वर्णनम् ।।
-अप्पय्य दीक्षित, कुवलयानन्द, १६१ ५. अद्भुतस्य पदार्थस्य भूतस्याथ भविष्यतः । यत् प्रत्यक्षायमाणत्वं तद्भाविकमुदाहृतम् ॥
-विश्वनाथ, साहित्यदर्पण, १०, १२२