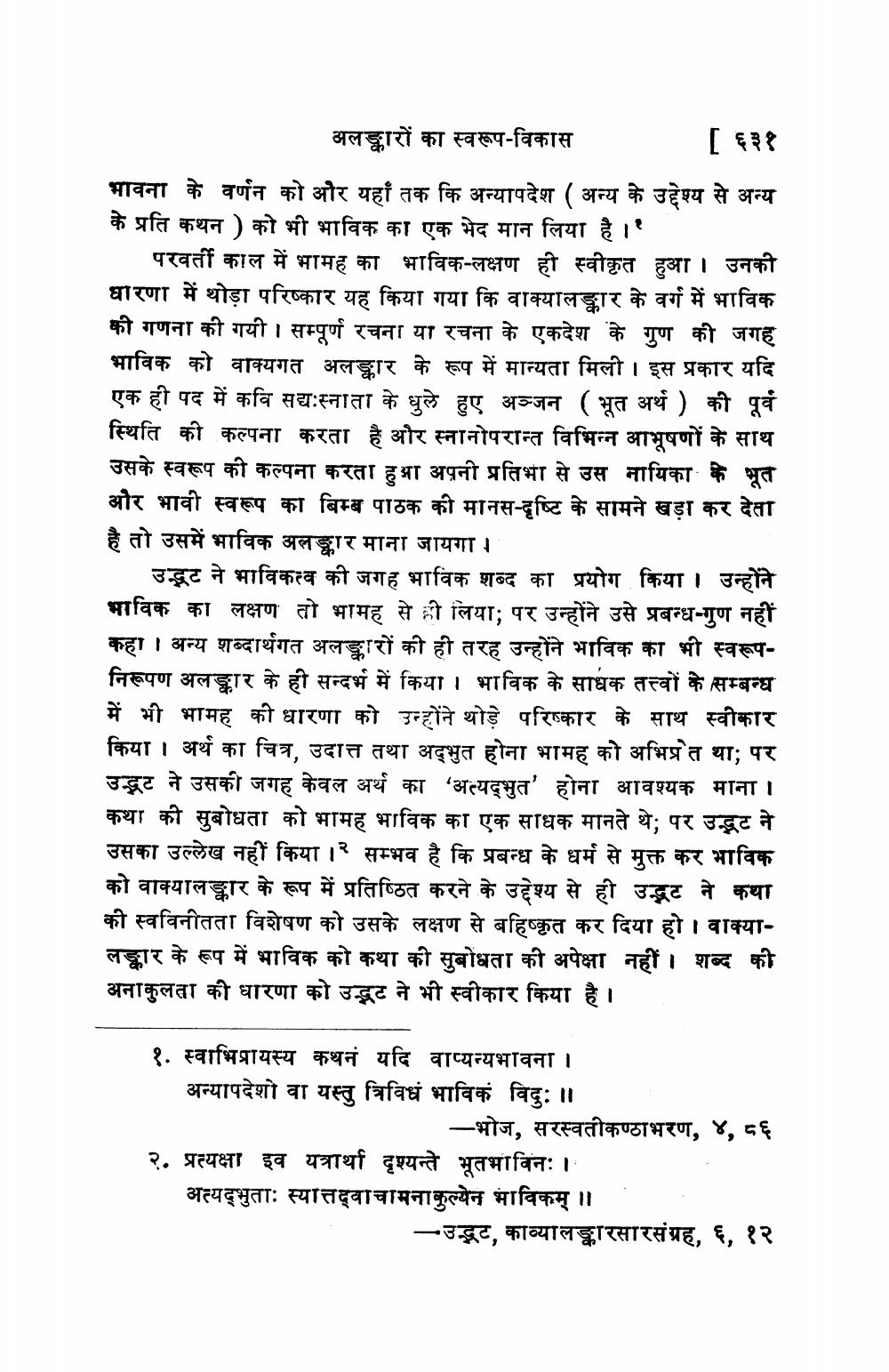________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास [ ६३१ भावना के वर्णन को और यहाँ तक कि अन्यापदेश ( अन्य के उद्देश्य से अन्य के प्रति कथन ) को भी भाविक का एक भेद मान लिया है।' __ परवर्ती काल में भामह का भाविक-लक्षण ही स्वीकृत हुआ। उनकी धारणा में थोड़ा परिष्कार यह किया गया कि वाक्यालङ्कार के वर्ग में भाविक की गणना की गयी। सम्पूर्ण रचना या रचना के एकदेश के गुण की जगह भाविक को वाक्यगत अलङ्कार के रूप में मान्यता मिली। इस प्रकार यदि एक ही पद में कवि सद्यःस्नाता के धुले हुए अञ्जन (भूत अर्थ ) की पूर्व स्थिति की कल्पना करता है और स्नानोपरान्त विभिन्न आभूषणों के साथ उसके स्वरूप की कल्पना करता हुआ अपनी प्रतिभा से उस नायिका के भूत और भावी स्वरूप का बिम्ब पाठक की मानस-दृष्टि के सामने खड़ा कर देता है तो उसमें भाविक अलङ्कार माना जायगा। __उद्भट ने भाविकत्व की जगह भाविक शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने भाविक का लक्षण तो भामह से ही लिया; पर उन्होंने उसे प्रबन्ध-गुण नहीं कहा । अन्य शब्दार्थगत अलङ्कारों की ही तरह उन्होंने भाविक का भी स्वरूपनिरूपण अलङ्कार के ही सन्दर्भ में किया। भाविक के साधक तत्त्वों के सम्बन्ध में भी भामह की धारणा को उन्होंने थोड़े परिष्कार के साथ स्वीकार किया। अर्थ का चित्र, उदात्त तथा अद्भुत होना भामह को अभिप्रेत था; पर उद्भट ने उसकी जगह केवल अर्थ का 'अत्यद्भुत' होना आवश्यक माना। कथा की सुबोधता को भामह भाविक का एक साधक मानते थे; पर उद्भट ने उसका उल्लेख नहीं किया ।२ सम्भव है कि प्रबन्ध के धर्म से मुक्त कर भाविक को वाक्यालङ्कार के रूप में प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से ही उद्भट ने कथा की स्वविनीतता विशेषण को उसके लक्षण से बहिष्कृत कर दिया हो। वाक्यालङ्कार के रूप में भाविक को कथा की सुबोधता की अपेक्षा नहीं। शब्द की अनाकुलता की धारणा को उद्भट ने भी स्वीकार किया है।
१. स्वाभिप्रायस्य कथनं यदि वाप्यन्यभावना। अन्यापदेशो वा यस्तु त्रिविधं भाविकं विदुः ॥
-भोज, सरस्वतीकण्ठाभरण, ४, ८६ २. प्रत्यक्षा इव यत्रार्था दृश्यन्ते भूतभाविनः । अत्यद्भुताः स्यात्तद्वाचामनाकुल्येन भाविकम् ॥
-उद्भट, काव्यालङ्कारसारसंग्रह, ६, १२