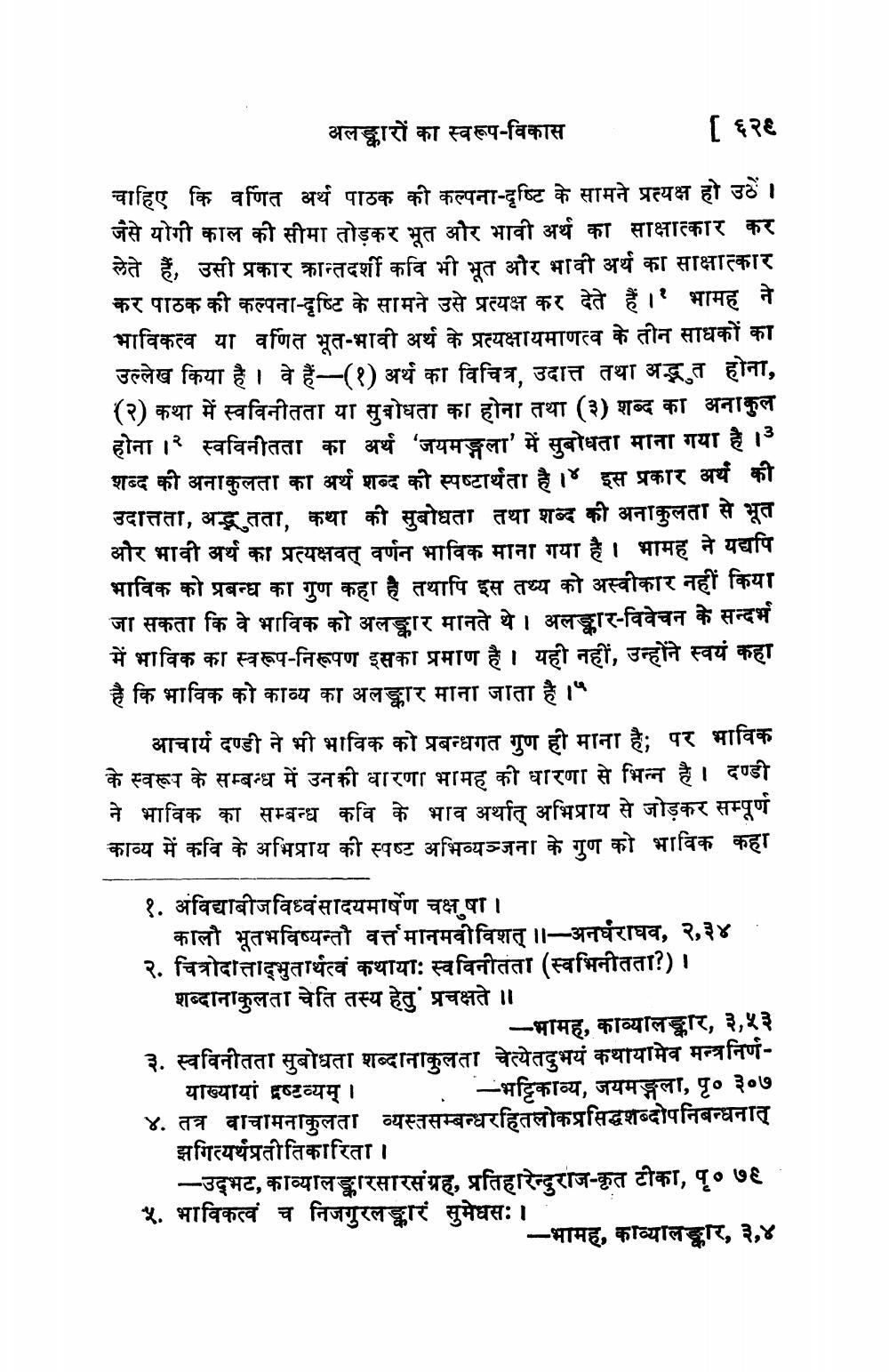________________
अलङ्कारों का स्वरूप - विकास
[ ६२९ चाहिए कि वर्णित अर्थ पाठक की कल्पना - दृष्टि के सामने प्रत्यक्ष हो उठें । जैसे योगी काल की सीमा तोड़कर भूत और भावी अर्थ का साक्षात्कार कर लेते हैं, उसी प्रकार क्रान्तदर्शी कवि भी भूत और भावी अर्थ का साक्षात्कार कर पाठक की कल्पना -दृष्टि के सामने उसे प्रत्यक्ष कर देते हैं । ' भामह ने भाविकत्व या वर्णित भूत-भावी अर्थ के प्रत्यक्षायमाणत्व के तीन साधकों का उल्लेख किया है । वे हैं -- (१) अर्थ का विचित्र, उदात्त तथा अद्भुत होना, (२) कथा में स्वविनीतता या सुबोधता का होना तथा (३) शब्द का अनाकुल होना । २ स्वविनीतता का अर्थ 'जयमङ्गला' में सुबोधता माना गया है । 3 शब्द की अनाकुलता का अर्थ शब्द को स्पष्टार्थता है । इस प्रकार अर्थ की उदात्तता, अद्भ ुतता, कथा की सुबोधता तथा शब्द की अनाकुलता से भूत और भावी अर्थ का प्रत्यक्षवत् वर्णन भाविक माना गया है। भामह ने यद्यपि भाविक को प्रबन्ध का गुण कहा है तथापि इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वे भाविक को अलङ्कार मानते थे । अलङ्कार-विवेचन के सन्दर्भ में भाविक का स्वरूप - निरूपण इसका प्रमाण है । यही नहीं, उन्होंने स्वयं कहा है कि भाविक को काव्य का अलङ्कार माना जाता है 14
आचार्य दण्डी ने भी भाविक को प्रबन्धगत गुण ही माना है; पर भाविक के स्वरूप के सम्बन्ध में उनकी धारणा भामह की धारणा से भिन्न है । दण्डी ने भाविक का सम्बन्ध कवि के भाव अर्थात् अभिप्राय से जोड़कर सम्पूर्ण काव्य में कवि के अभिप्राय की स्पष्ट अभिव्यञ्जना के गुण को भाविक कहा
१. अविद्याबीज विध्वंसादयमार्षेण चक्षुषा ।
कालो भूतभविष्यन्तौ वर्त्तमानमवीविशत् ॥ - अनर्घराघव, २,३४ २. चित्रोदात्ताद्भुतार्थत्वं कथायाः स्वविनीतता ( स्वभिनीतता ? ) । शब्दानाकुलता चेति तस्य हेतु ं प्रचक्षते ॥
- भामह, काव्यालङ्कार, ३, ५३ ३. स्वविनीतता सुबोधता शब्दानाकुलता चेत्येतदुभयं कथायामेव मन्त्र निर्णयाख्यायां द्रष्टव्यम् । — भट्टिकाव्य, जयमङ्गला, पृ० ३०७ ४. तत्र वाचामनाकुलता व्यस्तसम्बन्धरहितलोकप्रसिद्धशब्दोपनिबन्धनात् झगित्यर्थप्रतीतिकारिता ।
—उद्भट, काव्यालङ्कारसारसंग्रह, प्रतिहारेन्दुराज कृत टीका, पृ० ७६ ५. भाविकत्वं च निजगुरलङ्कारं सुमेधसः ।
- भामह, काव्यालङ्कार, ३,४