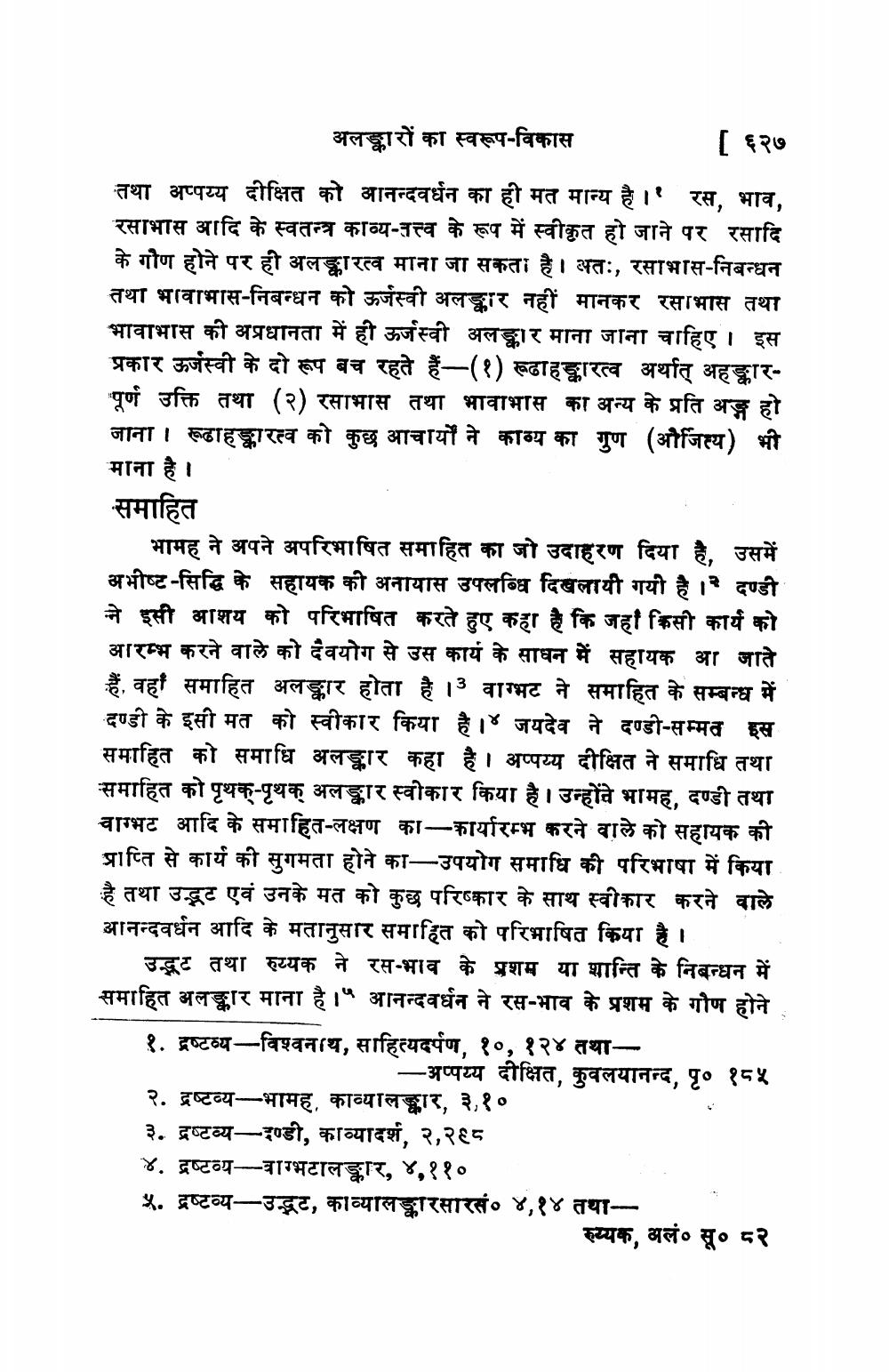________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास
[ ६२७
तथा अप्पय्य दीक्षित को आनन्दवर्धन का ही मत मान्य है। रस, भाव, रसाभास आदि के स्वतन्त्र काव्य-तत्त्व के रूप में स्वीकृत हो जाने पर रसादि के गौण होने पर ही अलङ्कारत्व माना जा सकता है। अतः, रसाभास-निबन्धन तथा भावाभास-निबन्धन को ऊर्जस्वी अलङ्कार नहीं मानकर रसाभास तथा भावाभास की अप्रधानता में ही ऊर्जस्वी अलङ्कार माना जाना चाहिए। इस प्रकार ऊर्जस्वी के दो रूप बच रहते हैं-(१) रूढाहङ्कारत्व अर्थात् अहङ्कारपूर्ण उक्ति तथा (२) रसाभास तथा भावाभास का अन्य के प्रति अङ्ग हो जाना। रूढाहङ्कारत्व को कुछ आचार्यों ने काव्य का गुण (औजित्य) भी माना है। समाहित
भामह ने अपने अपरिभाषित समाहित का जो उदाहरण दिया है, उसमें अभीष्ट-सिद्धि के सहायक की अनायास उपलब्धि दिखलायी गयी है। दण्डी ने इसी आशय को परिभाषित करते हुए कहा है कि जहां किसी कार्य को आरम्भ करने वाले को दैवयोग से उस कार्य के साधन में सहायक आ जाते हैं, वहीं समाहित अलङ्कार होता है । वाग्भट ने समाहित के सम्बन्ध में दण्डी के इसी मत को स्वीकार किया है। जयदेव ने दण्डी-सम्मत इस समाहित को समाधि अलङ्कार कहा है। अप्पय्य दीक्षित ने समाधि तथा समाहित को पृथक्-पृथक् अलङ्कार स्वीकार किया है। उन्होंने भामह, दण्डी तथा वाग्भट आदि के समाहित-लक्षण का कार्यारम्भ करने वाले को सहायक की प्राप्ति से कार्य की सुगमता होने का उपयोग समाधि की परिभाषा में किया है तथा उद्भट एवं उनके मत को कुछ परिष्कार के साथ स्वीकार करने वाले आनन्दवर्धन आदि के मतानुसार समाहित को परिभाषित किया है।
उद्भट तथा रुय्यक ने रस-भाव के प्रशम या शान्ति के निबन्धन में समाहित अलङ्कार माना है।५ आनन्दवर्धन ने रस-भाव के प्रशम के गौण होने . १. द्रष्टव्य-विश्वनाथ, साहित्यदर्पण, १०, १२४ तथा
-अप्पय्य दीक्षित, कुवलयानन्द, पृ० १८५ २. द्रष्टव्य-भामह, काव्यालङ्कार, ३,१० ३. द्रष्टव्य-दण्डी, काव्यादर्श, २,२६८ ४. द्रष्टव्य-वाग्भटालङ्कार, ४,११० ५. द्रष्टव्य-उद्भट, काव्यालङ्कारसारसं० ४,१४ तथा
रुय्यक, अलं० सू० ८२