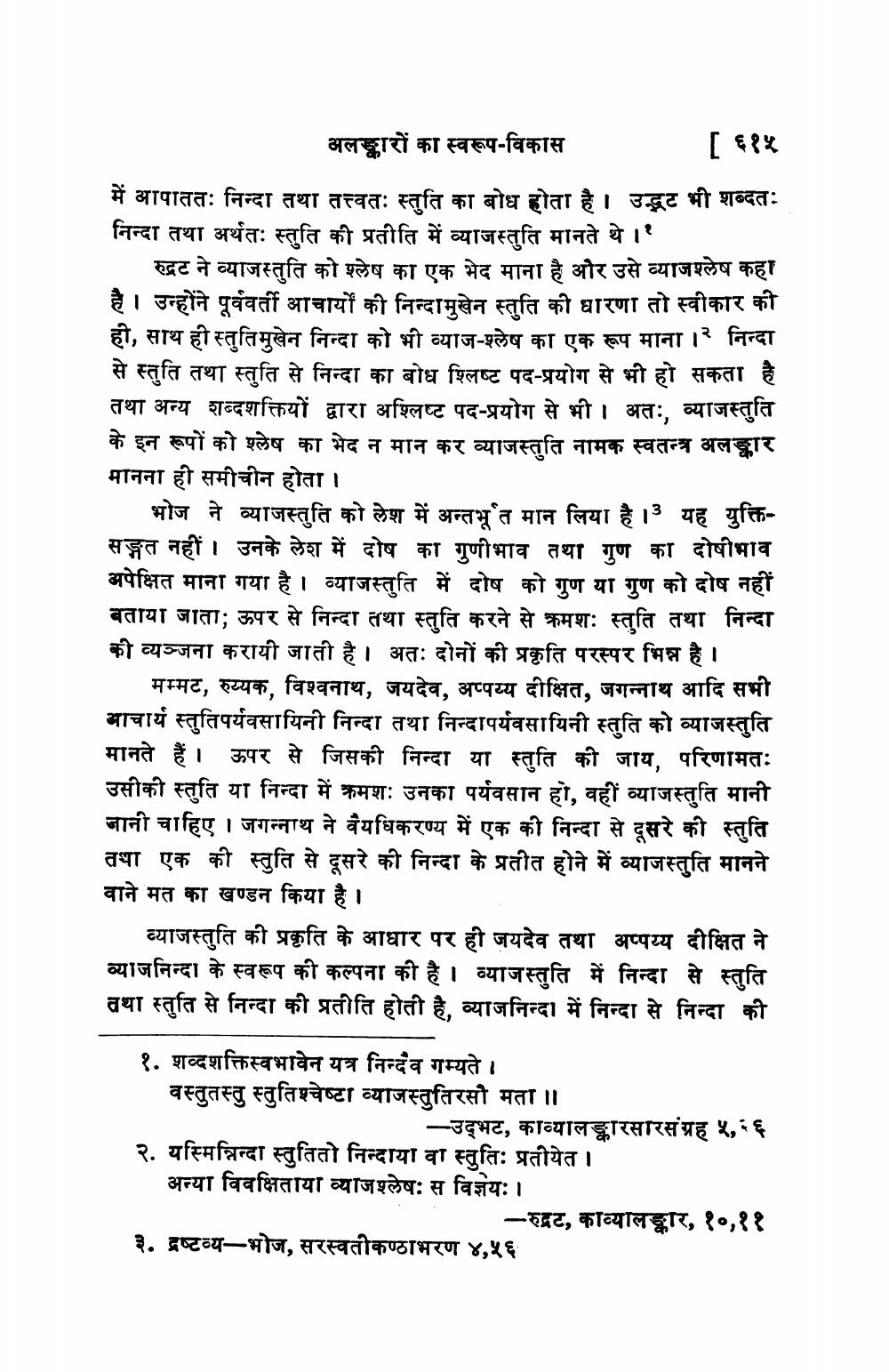________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास
में आपाततः निन्दा तथा तत्त्वतः स्तुति का बोध होता है। उद्भट भी शब्दतः निन्दा तथा अर्थतः स्तुति की प्रतीति में व्याजस्तुति मानते थे ।'
रुद्रट ने व्याजस्तुति को श्लेष का एक भेद माना है और उसे व्याजश्लेष कहा है। उन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों की निन्दामुखेन स्तुति की धारणा तो स्वीकार की ही, साथ ही स्तुतिमुखेन निन्दा को भी व्याज-श्लेष का एक रूप माना।२ निन्दा से स्तुति तथा स्तुति से निन्दा का बोध श्लिष्ट पद-प्रयोग से भी हो सकता है तथा अन्य शब्दशक्तियों द्वारा अश्लिष्ट पद-प्रयोग से भी। अतः, व्याजस्तुति के इन रूपों को श्लेष का भेद न मान कर व्याजस्तुति नामक स्वतन्त्र अलङ्कार मानना ही समीचीन होता।
भोज ने व्याजस्तुति को लेश में अन्तर्भूत मान लिया है। यह युक्तिसङ्गत नहीं। उनके लेश में दोष का गुणीभाव तथा गुण का दोषीभाव अपेक्षित माना गया है। व्याजस्तुति में दोष को गुण या गुण को दोष नहीं बताया जाता; ऊपर से निन्दा तथा स्तुति करने से क्रमशः स्तुति तथा निन्दा की व्यञ्जना करायी जाती है। अतः दोनों की प्रकृति परस्पर भिन्न है।। ___ मम्मट, रुय्यक, विश्वनाथ, जयदेव, अप्पय्य दीक्षित, जगन्नाथ आदि सभी भाचार्य स्तुतिपर्यवसायिनी निन्दा तथा निन्दापर्यवसायिनी स्तुति को व्याजस्तुति मानते हैं। ऊपर से जिसकी निन्दा या स्तुति की जाय, परिणामतः उसीकी स्तुति या निन्दा में क्रमशः उनका पर्यवसान हो, वहीं व्याजस्तुति मानी जानी चाहिए । जगन्नाथ ने वैयधिकरण्य में एक की निन्दा से दूसरे की स्तुति तथा एक की स्तुति से दूसरे की निन्दा के प्रतीत होने में व्याजस्तुति मानने वाने मत का खण्डन किया है।
व्याजस्तुति की प्रकृति के आधार पर ही जयदेव तथा अप्पय्य दीक्षित ने व्याजनिन्दा के स्वरूप की कल्पना की है। व्याजस्तुति में निन्दा से स्तुति तथा स्तुति से निन्दा की प्रतीति होती है, व्याजनिन्दा में निन्दा से निन्दा की
१. शब्दशक्तिस्वभावेन यत्र निन्दैव गम्यते । वस्तुतस्तु स्तुतिश्चेष्टा व्याजस्तुतिरसौ मता ॥
-उद्भट, काव्यालङ्कारसारसंग्रह ५,२६ २. यस्मिन्निन्दा स्तुतितो निन्दाया वा स्तुतिः प्रतीयेत । अन्या विवक्षिताया व्याजश्लेषः स विज्ञेयः।
-रुद्रट, काव्यालङ्कार, १०,११ ३. द्रष्टव्य-भोज, सरस्वतीकण्ठाभरण ४,५६